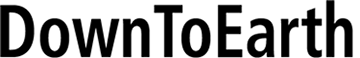
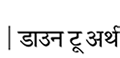
बर्मा के जंगलों पर अपने आधिपत्य के लिए अंग्रेजों ने न केवल वहां की स्थानीय आदिम जनजाति ‘करेन’ का शोषण किया, बल्कि उनकी परम्परागत कृषि प्रणाली को भी बर्बाद कर दिया था



टोंग्या एक ऐसी चाल है जिसका अंग्रेजों ने बर्मा (आधुनिक म्यांमार) में खूब इस्तेमाल किया। इस पद्धति का पहली बार प्रयोग वहां 19वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। म्यांमार की भाषा में ‘टोंग’ का अर्थ टीला और ‘या’ का अर्थ खेती होता है। साम्राज्यवादियों ने इस पद्धति का विकास इसलिए किया, ताकि वनों को व्यावसायिक मूल्य वाले वृक्षों से पाटा जा सके। मानव श्रम के लिए उन्होंने ऐसे गैर-ईसाई लोगों को अपने अधीन किया, जो परंपरागत झूम खेती में कुशल थे और जो अंग्रेजों के कारोबारी हितों के लिए अपनी पहाड़ियों पर ही भूमिहीन मजदूर के तौर पर काम करने के लिए बहलाए गए अथवा मजबूर किए गए थे।
टोंग्या, बर्मा में अंग्रेजों के राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से जुड़ी व्यवस्था थी। बर्मा के सागौन, उस समय दुनिया की बेहद मूल्यवान लकड़ी थी और इसे हासिल करना बहुत कठिन होता था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेज सागौन की जरूरत के लिए भारत में मालाबार की पहाड़ियों से होने वाली आपूर्ति पर निर्भर थे। बर्मा की तरफ रुख करने के पीछे ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य वहां स्थित सागौन के विशाल जंगलों पर अपना आधिपत्य कायम करना था। अंग्रेजों ने बर्मा को अपना उपनिवेश बनाने के लिए तीन युद्ध किए। पहला, 1824-26 के बीच। उसके बाद 1852 में और अंत में 1885 में अंग्रेजों ने बर्मा पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य कायम कर लिया। टोंग्या पद्धति की अवधारणा 19वीं सदी के मध्य और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान ब्रिटिश हितों को संतुष्ट करने के लिए विकसित की गई थी। उन्होंने स्थानीय घुमंतू पहाड़ी लोगों द्वारा व्यवहार में लाई जाने वाली संस्कृति ‘झूम कृषि’ के एक रूप को अपनाया।
बर्मा के तेनास्सेरिम क्षेत्र में अंग्रेजों का सामना झूम किसानों से हुआ। इनमें अधिकतर ‘करेन’ जाति के लोग थे, जो सागौन के जंगलों में खेती करते थे। ये किसान वार्षिक तौर पर जंगलों की सफाई और कटाई किया करते थे और वहां खाद्यान्न और कपास की फसलें उगाते थे। मिट्टी की उर्वरता को क्षीण होने से बचाने के लिए करेन लोगों ने एक आवर्तन प्रणाली को अपनाया, जिसमें वन क्षेत्रों में भूमि को 10-15 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था।लेकिन अंग्रेजों ने अपने इस नए उपनिवेश में व्यावसायिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत वन भूमि प्रबंधन की इस पद्धति को तहस-नहस कर दिया।
सन 1830 से ही अंग्रेज अधिकारियों ने झूम किसानों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था। इन प्रयासों में 1852 के बाद और तेजी आ गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्मा के पेगु प्रांत के सागौन के जंगलों पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले झूम खेती करने वाले किसानों को पहाड़ी जंगल छोड़ने और निचले मैदानी इलाकों में स्थायी तौर पर धान की खेती करने को प्रेरित किया। ब्रिटिश वनपाल विलियम सीटन ने सन 1863 में उल्लेख किया है कि शुरू में करेन लोगों ने खेती के अपने परंपरागत तरीकों को छोड़ने से इनकार कर दिया था।
यह एक नाजुक स्थिति थी। पेगु पर अंग्रेजों ने अभी-अभी अपना आधिपत्य स्थापित किया ही था और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोध अभी भी काफी मुखर था। वन अधिकारियों ने भी इन लोगों को मैदानी इलाकों में चले जाने के लिए मजबूर करने से इनकार कर दिया। अब दूसरा विकल्प था - लालच देना। वन अधिकारियों ने करेन आदिवासियों का दिल जीतने के लिए वानिकी कार्यों में भाग लेने का प्रयास शुरू कर दिया। डायेट्रिच ब्रैंड्रिस (जो बाद में भारत के पहले वन महानिरीक्षक बने) ने सफलतापूर्वक कुछ प्रयोग किए, जिसके आधार पर उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे करेन लोगों को उनके द्वारा साफ किए गए पहाड़ों पर सागौन रोपने के लिए तैयार करें।
विचार यह था कि झूम किसान अपने खेतों की फसलों के स्थान पर वन विभाग की ओर से दी गई सागौन की पौधों का रोपण करेंगे। करेन द्वारा परंपरागत झूम खेती काे छोड़ना उस क्षेत्र में सागौन के जंगलों को बढ़ने में मदद कर सकता था। इसी तरह से टोंग्या पद्धति की परिकल्पना की गई। लेकिन करेन आदिवासी इससे प्रभावित नहीं थे। औपनिवेशिक वनपालों के मुताबिक, करेन आदिवासी यह भली-भांति जानते थे कि यह पद्धति धीरे-धीरे उनको उनके पारंपरिक जीवन पद्धति के अंत की ओर ले जाएगी। वजह साफ थी कि एक सागौन के जंगल को तैयार होने में 100-150 वर्ष लग जाते हैं, जो करेन लोगों के 10-15 वर्षीय झूम कृषि चक्र से कहीं ज्यादा है।
स्वाभाविक तौर पर, करेन लोगों ने सबसे पहले टोंग्या पद्धति के क्रियान्वयन के सभी प्रयासों का पुरजोर विरोध किया। कुछ करेन अंग्रेजों के आधिपत्य वाले बर्मा से पलायन कर गए (1860 के मध्य में करेन समूह पूर्व से सियाम या उत्तर से राजतंत्रीय बर्मा भाग गए)। बाकी लोग अपनी पारंपरिक खेती करते हुए सागौन के जंगल में फंस गए। हालांकि, उन्होंने सभी सबूत नष्ट कर दिए थे, ताकि बाद में यह पता न चल पाए कि उस क्षेत्र में कभी सागौन उगाई भी गई थी। सागौन को नष्ट करते पाए जाने पर वन अधिकारियों ने उन लोगों पर भारी जुर्माना लगाया था।
सन 1870 की शुरुआत से अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक लगान और जुर्माना लगाने के साथ ही प्रलोभन भी दिया जिसमें वृक्षारोपण के लिए दिया जाने वाला धन अथवा निजी उपयोग के लिए अलग भूमि का आवंटन शामिल था। ताकि कृषकों को टोंग्या पद्धति में हिस्सेदारी के लिए राजी किया जा सके।
अंग्रेजों द्वारा करेन लोगों को निजी इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से भूमि दिए जाने के वादे के बाद सन 1869 में थारावाड्डी जिले के एक गांव में सर्वप्रथम करेन समुदाय ने सागौन रोपण के लिए तैयार हुए। इसके बाद दूसरे गाव के लोगों ने भी इसे अपनाया। इस तरह 1880 के अंत तक ब्रिटिश बर्मा के एक बड़े हिस्से में टोंग्या पद्धति अपना ली गई थी। सन 1876 में जहां सागौन का कुल रोपण क्षेत्र सिर्फ 425.25 हेक्टेयर था, वहीं अगले दस साल में टोंग्या के तहत वृक्षारोपण बढ़कर 4,050 हेक्टेयर तक पहुंच गया। सन 1906 तक यह आंकड़ा बढ़कर 28,350 हेक्टेयर को पार कर गया था। सन 1900 में इन बागानों से 30 हजार टन लकड़ी की वार्षिक आपूर्ति होने का अनुमान लगाया जाता है।
जाहिर है, 19वीं सदी बर्मा में कई शाही वानपालों ने टोंग्या प्रणाली को एक बड़ी सफलता के के तौर पर रेखांकित किया। जैसा कि बार्थोल्ड रिब्बेन्ट्रोप (जिसे बर्मा में प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद भारत का वन महानिरीक्षक बनाया गया) ने टिप्पणी की, “टोंग्या प्रणाली ने अंग्रेजों के विरोधी करेन समुदाय को विभाग के सबसे वफादार सेवकों में तब्दील करने में सक्षम बनाया।” लेकिन अस्थिरता के बादल जल्द ही उमड़ने लगे। औपनिवेशिक बर्मा में 20वीं सदी की शुरुआत में बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने 1930 के दशक से टोंग्या को प्रचलन से बाहर करने पर मजबूर कर दिया।
यह प्रणाली मूल रूप से ऐसे समय में विकसित की गई थी, जब अंग्रेजों के लिए सागौन तक पहुंच आवश्यक थी। अंग्रेजों ने पेगु स्थित सागौन के जंगलों पर अपना आधिपत्य 1852 के युद्ध के बाद स्थापित किया। लेकिन म्यांमार के सबसे कीमती सागौन के जंगल राजतन्त्र नियंत्रित क्षेत्र में थे। वहां से निर्यात अंग्रेजों के लिए काफी अस्थिर और असुरक्षित था। राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से अक्सर आपूर्ति बंद हो जाती थी। इन परिस्थितियों में, टोंग्या के माध्यम से सागौन का पैदावार एक सफल अनुभव साबित हुई।
हालांकि, 1885 में हुए तीसरे बर्मा युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की पहुंच केंद्रीय और उत्तरी बर्मा तक सुनिश्चित कर दी थी। अब यह ज्यादा जरूरी हो गया था कि वनों को बढ़ावा देने की इस विधि को व्यापक क्षेत्र में अपनाया जाए। इसके बाद पूरा ध्यान प्राकृतिक उत्पादन की ओर मुड़ता चला गया।
आखिर में एक कीड़े ने पूरी पटकथा को बदल दिया। और आखिरकार शाही जंगलों को भी उजाड़ दिया। कुछ अंग्रेजों ने सगौन के मोनोकल्चर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मोनोकल्चर कई कीड़ों को स्थायी रूप से बसने में मदद करता है। मसलन, इस शताब्दी की शुरुआत में सागौन के पेड़ों को बीहोल बोरर नामक नामक एक कीट के चलते व्यापक क्षति होने की पुष्टि हुई है। ा ये कीट सागौन के पेड़ों द्वारा पोषित हुए थे या नहीं यह एक बहस का मुद्दा था। कुछ लोगों का तर्क था कि ऐसा सागौन की वजह से नहीं, बल्कि बारिश की वजह हुआ। आखिर में, 1936 में एक गंभीर वित्तीय संकट ने औपनिवेशिक अधिकारियों को इस पद्धति को खत्म करने पर मजबूर कर दिया।
लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के किंग्स कॉलेज के भूगोल विभाग में पढ़ाते हैं।
We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together.

Comments are moderated and will be published only after the site moderator’s approval. Please use a genuine email ID and provide your name. Selected comments may also be used in the ‘Letters’ section of the Down To Earth print edition.