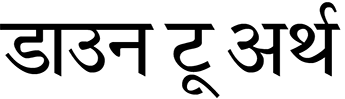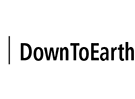बाबरी विध्वंस: भागीदारी के प्रयास से बुझ सकती हैं आग की लपटें
6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस की घटना की प्रतिक्रियास्वरूप डाउन टू अर्थ के संस्थापक संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा लिखा गया लेख
On: Monday 06 December 2021
बाबरी मस्जिद विध्वंस को 29 साल हो चुके हैं। इन सालों में सांप्रदायिक सदभाव सुधरने की बजाय बिगड़ ही रहा है। डाउन टू अर्थ के संस्थापक संपादक अनिल अग्रवाल फरवरी 1993 में इस घटना पर अपना संपादकीय लिखा था। जो आज भी प्रासंगिक है। इसलिए इस संपादकीय को हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया जा रहा है।
डाउन टू अर्थ हमेशा से यह मानता रहा है कि देश आज उत्पादकता घटने और जंगलों, घास के मैदानों, तालाबों, पोखरों और नम-भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लगातार क्षय होने जैसी जिन बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है, उनसे निपटने का सबसे सही तरीका आत्म-प्रबंधन और आत्म-नियंत्रण है। इन समस्याओं के चलते ही देश भयंकर गरीबी का सामना कर रहा है और इसी के चलते देश के कराड़ो लोगों के सामने जीने का संकट पैदा हो रहा है।
यह उन गंावों में रहने वाले समुदायों का अपना अनुभव है, जो वह पारिस्थितिकी के नष्ट होने के चलते अपने जीवन में पैदा होने वाले संकटों को महसूस कर रहे हैं। शहर-केंद्रित प्रशासक और बुद्धिजीवी भले ही कुछ और सोचें, पारिस्थितिक संकट को लेकर निश्चित रूप से एक सामाजिक प्रतिक्रिया जन्म ले रही है, भले ही फिलहाल यह काफी सीमित है। कई तरह की असमानाताओं को दरकिनार कर कई समुदायों ने अपने वातावरण का कायाकल्प किया है। उनका अनुभव देश के उन नीति-निर्माताओं के लिए एक संकेतक है, जो पारिस्थितिक क्षय को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं।
1986 में जब पीवी नरसिंह राव मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्हें भारत के पर्यावरण की स्थिति पर एक प्रस्तुति दिखाई गई और बताया गया कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस पर उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी कि ‘यह तो लगभग हर चीज के लिए सच है।’
पिछले कुछ महीनों से देश, अलग-अलग समुदायों के बीच तनावों और शहरों में बड़े स्तर पर हिंसा की घटनाओं का सामना कर रहा है। कानून-व्यवस्था को संभालने वाला तंत्र इस समस्या की जड़ तक पहुंचने में नाकाम रहा है, जिससे समाज को जन-धन का नुकसान उठाना पड़ा है। इन हिंसक घटनाओं की दुनिया भर में निंदा की गई है और इसने भारत की अंहिसक देश की छवि को चोट पहुंचाई है।
हमने डाउन टू अर्थ के इस अंक में जो सवाल उठाया है वह यह है - क्या शहरी सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने में भागीदारी वाली राजनीति वैसे ही सकारात्मक परिणाम दे सकती है जैसे वह ग्रामीण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से निपटने में देती है? इस सवाल के जवाब में हमने उसी दृष्टिकोण का पालन किया है जो हम सामान्य रूप से संसाधन-प्रबंधन से जुड़े मामलों का विश्लेषण करते समय करते हैं।
यह दृष्टिकोण सफल उदाहरणों की पहचान करना है और फिर उनकी पड़ताल कर यह समझना है कि किस चीज ने उन्हें सफल बनाया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंबई और सूरत सहित देश के कम से कम नौ प्रमुख शहर आग की लपटों में घिर गए। हालांकि देश के एक बड़े हिस्से ने ऐसा नहीं किया और जिस सवाल का हमने जवाब मांगा वह है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ?
इस अंक में पेश तीन विशिष्ट मामलों में यानी महाराष्ट्र के भिवंडी, बिहार के भागलपुर और नई दिल्ली के ओखला में हमने पाया कि शांति और सांप्रदायिक सौहार्द्र की व्यवस्था के चलते यहां जीवंत समुदायों ने एकता की पहल की। यह पहल इतनी प्रासंगिक है कि हमने यहां विस्तार से उसे यहां पेश करने का फैसला लिया है।
पहली महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, वह यह कि हमारी मुख्यधारा की राजनीति सांप्रदायिक सौहार्द्र के खराब होने जैसी स्थिति से निपटने में तेजी से नकारा होती जा रही है। अपने वोट बैंक को पालने-पोसने के लिए भाजपा से लेकर कांग्रेस और सीपीएम तक ने लोगों को समुदाय और जाति में बांटने का काम किया है।
बैलेट बॉक्स के आधार पर बना लोकतंत्र अपने को साबित करने में नाकाम रहा है और यह कई मायनों में खतरनाक है। दंगा-प्रभातिव क्षेत्रों में अपने सर्वे में हमने पाया कि बहुत कम लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को मदद के लिए अपने बीच पाया। यहां तक कि धर्मनिरपेक्षता के लिए मुखर सीपीएम भी कलकत्ता के लोगों को बचाने में नाकाम रही, जहां यह सत्ताधारी पार्टी है।
केवल देश की राजनीतिक पार्टियां ही जान-बूझकर लोगों को बांटने का काम नहीं कर रहीं, कई मामलों में आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण भी सामाजिक सद्भाव को नष्ट करने का काम कर रहा है। भारी तादाद में अप्रवासियों वाला कोई शहर जिसमें संस्थाएं न हों, और जो दो समुदायों के बीच सौहार्द्र विकसित कर सकता है, वह आसानी से ऐसे बक्से में तब्दील हो जाता है, जिसे बस चिंगारी दिखाने की जरूरत है।
यहां तक कि एक ऐसा शहर भी, जिसमें कभी मजबूत सामुदायिक संस्थाएं थीं, आसानी से तेज आधुनिकीकरण की आड़ में दंगाई बन सकता है, अगर उसे शांत दिमाग से समझाया नहीं जाता। इन स्थितियों में, बिना किसी चरित्र वाले समाज के ऐसे भयावह आयाम हो सकते हैं, जिसमें किसी भी इमारत के निवासी एक लूटपाट करने वाली भीड़ में शामिल हो सकते हैं और अपने पड़ोसियों को लूट सकते हैं। इसमें जमीन एक डराने वाली बहुमूल्य संपत्ति में तब्दील हो सकती है, जैसा कि कई महानगरों में हुआ है। इनमें अर्थ-निहित स्वार्थ, बढ़े हुए सांप्रदायिक जुनून का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और अपने संसाधन आधार यानी जमीन पर कब्जा करने के लिए खास बस्तियों को लक्षित करेंगे।
प्रतिकूल प्रशासनिक-व्यवस्था भी दंगे में पड़ोसी को शिकार बनाने की मानसिकता को बल देती है। गैर-कानूनी काम करने की मानसिकता किसी खास स्थिति में निहित नहीं होती। अगर आप किसी जंगल में रहने वाले लोगों के सारे अधिकार खत्म कर देंगे तो जंगल की लकड़ी बीनने वाला हर आदमी अनैतिक हो जाएगा।
शहरी भारत की अधिकांश आबादी अवैध बस्तियों में रहती है और इसलिए उन्हें ऐसे सत्ता-दलालों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कानून के दायरे से बाहर काम करना जानते हैं। ये दलाल इन निवासियों को वे सारी नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें जीवित रहने में मदद कर सकती हैं। ये दलाल जो लोगों ओर प्रशासन के बीच गैर-कानूनी काम करते हैं, किसी तरह से राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वे इस प्रक्रिया में उन राजनेताओं को बाहर कर देना चाहते है, जिनकी समृद्धि वैध गतिविधियों में निहित है। ऐसे में राज्य, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए खुद जिम्मेदार है, जो खाली राजनीतिक स्थान को लफंगीकरण से भरने की कोशिश करती है।
अगर अलग-अलग धर्मों के पड़ोसियों के बीच सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है और चरित्र-विहीन समाज बनने से रोकना है तो निश्चित रूप से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए तंत्र की आवश्यकता है। दंगों के दौरान जब नफरत बढ़ाने वाली अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिनमें टीवी भी एक भूमिका निभाता है, तो लोगों को समझना चाहिए कि सामाजिक सद्भाव के लिए क्या सही है और कौन सी खबर पर उत्तेजित होने से पहले उसकी पड़ताल कर लेनी चाहिए। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वालों पर लगाम लगाने के लिए संवेदनशील संचार माध्यमों की खास जरूरत है। भागलपुर, भिवंडी और ओखला दिखाते हैं कि यह किया जा सकता है।
सांप्रदायिक सौहार्द्र को कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से कानून-व्यवस्था संभालने वाले तंत्र पर भरोसा करने के कारण भारतीय राज्य ने सामुदायिक पहल को बढ़ावा देने की उपेक्षा की है। इसने केवल अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसका आर्थिक खामियाजा अंतिम आदमी को भुगतना पड़ता है।
कोई आश्चर्य नहीं कि किसी संकट के समय कानून-व्यवस्था संभालने वाले तंत्र की आम शिकायत यही होती है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इस तरह से क्या वन विभाग हर एक पेड़ की रक्षा के लिए एक चौकीदार की मांग करेगा या वन्य जीवों को संरक्षित रखने वाली एजेंसी हर बाघ के लिए एक गार्ड की मांग करेगी। क्या पुलिस चाहेगी कि किसी मुस्लिम-बहुल इलाके में हर हिंदू के घर के बाहर एक पुलिस चौकी हो या फिर किसी हिंदू-बहुल इलाके में हर मुस्लिम के घर के बाहर एक पुलिस चौकी हो। हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा किया जाता है, इसके बावजूद राजनीतिक प्रक्रिया का संप्रदायीकरण हो जाने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कानून-व्यवस्था संभालने वाला प्रशासन आपात स्थिति में निरपेक्ष रहे।
चूंकि जगंल का चौकीदार अकेले जंगल को बचाने की गारंटी नहीं है, इसीलिए पर्यावरणविदों ने सामाजिक घेराबंदी को एक उपाय के तौर पर पेश किया। उनका अनुभव बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, उनका इस्तेमाल और अनुशासित तरीकों से उनका बंटवारा किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि ग्रामीण-स्तर की वार्ताओं, बहसों और सौदेबाजी से किया जा सकता है।
पर्यावरण की रक्षा करने से पूरे समुदाय को बेहतर आर्थिक परिणाम मिलने की वजह से ऐसे मुद्दे आम सहमति से हल कर लिए जाते हैं, जिन पर लोगों में मतभेद होते हैं। यह निश्चित तौर पर ‘बॉलीवुड के सुपरहीरो अमिताभ बच्चन वाला दृष्टिकोण’ नहीं है, जिसमें एक स्तर पर लफंगा बना रहने वाला कोई आदमी जो हमेशा किसी से उलझने और लड़ने को तैयार रहता है, लेकिन किसी देवदूत की तरह उन गरीब लोगों को बचाने आ जाता है, जो उसकी राह देख रहे होते हैं।
राजनीतिक पार्टियों को अपनी बांटने की नीति को लेकर कोई डर इसलिए नहीं है क्योंकि वास्तविक जीवन में कोई सुपरहीरो नहीं होता। जहां तक जनता का सवाल है तो वह जरूर मुंबईया फिल्मों की तरह चुपचाप सुनने और देखने वाली बनी रहती है। राजनेताओं के लिए सहमति वाला और आस-पड़ोस के साथ बातचीत से समस्याएं सुलझाने वाला समाज एक गंभीर खतरे की तरह है क्योंकि वह उनके राजनीतिक स्पेस को कम करेगा और संसाधनों के दलाल के तौर उनकी भूमिका को खत्म कर देगा।
उचित रूप से पोषित, सामुदायिक पहल बढ़ती हुई जगह की मांग करती है और वह महज सांप्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए काम करने से संतुष्ट नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, चिपको आंदोलन द्वारा वनरोपण करने के लिए आयोजित महिला-समूहों ने विस्तार किया और दूसरे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को उठाया। जाहिर है कि राज्य ने इसे अपने कामों में दखल और प्रशासनिक स्पेस कम होने के तौर पर लिया है और वह इससे नाखुश है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारतीय राज्य ने कभी भी अपने और व्यक्ति के बीच एक मध्यस्थ-स्तर बनाने का प्रयास नहीं किया है। सामाजिक निकटता वह स्तर है जिस पर सहभागी राजनीति जन्म ले सकती है और विकसित हो सकती है। यही वह स्तर भी है जो व्यक्ति को केवल एक निष्क्रिय मतदाता के बजाय सीधे सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेने और बातचीत करने की अनुमति देता है। देश में आजादी के बाद से ही ऐसी सामाजिक विकास संस्थानों की उपेक्षा की गई। अगर समुदाय के स्तर की पहल सब कुछ हो जाती है तो राज्य की भूमिका क्षेत्रीय और अस्थायी हो जाती है।
यही वजह है कि सामाजिक सद्भाव के लिए समुदाय के स्तर पर कोई पहल की जाती है तो नौकरशाही का प्रयास रहता है कि समुदाय को केवल उसी एक मुद्दे ओर सीमित समय के लिए अधिकार दिए जाएं। हालांकि इन पैमानों से आगे जाकर देखें तो सामुदायिक पहल एक शक्तिशाली अवधारणा है, जिसे नौकरशाही अपने काम में रुकावट के तौर पर देखती है और जिसके साथ उपकार की भावना दिखाते हुए पेश आती है।
आज देश के सामने जो चुनौती है, वह कई मायनों में पूरी दुनिया के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है। पारिस्थितिक विविधता ने दुनिया भर में एक असाधारण सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया है। हालांकि तकनीकी प्रगति ने वैश्विक सांस्कृतिक समरूपता की एक असाधारण प्रक्रिया विकसित की है। लेकिन सांस्कृतिक विविधता, जैव-विविधता के जैसे ही प्रकृति का एक नियम है और इसका भी उसी की तरह सम्मान करने की जरूरत है।
केवल सांस्कृतिक प्रक्रियाएं ही तकनीकी प्रगति से निपट सकती हैं और सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए इसे सांस्कृतिक विविधता के तौर पर अवशोषित कर सकती हैं। गर्व करने वाले हिंदुओं को, गर्व करने वाले मुस्लिमों के साथ उसी तरह रहना सीखना चाहिए, जैसे गर्व करने वाले गुजरातियों को गर्व करने वाले नगाओं के साथ।
यह उतना आसान नहीं है, जितना शिक्षा और एक-दूसरे के बारे में तार्किकता के साथ जानना और एक दूसरे के बर्ताव का सम्मान करना। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है। दरअसल यह एक जीवंत समाज बनाने का मामला है, जिसमें अलग - अलग संस्कृतियों से आए लोग आस-पड़ोस में रहने वालों से बातचीत और संवाद करें। इसी से ऐसा समाज बन सकेगा, जिसमें सबको लाभ हो।
केवल राजनीतिक पार्टियों के बीच संवाद की तुलना में यह कहीं बेहतर होगा कि लाखों-करोड़ों लोगों के बीच अनगिनत संवाद हों, जिससे समाज में सहयोग और स्थिरता की भावना पनपे। ऐसे में अगर राजनीतिक पार्टियों के बीच बातचीत नाकाम भी हो जाती है तो ये करोड़ो लोग आपस में ही बातचीत करके स्थितियों को संभाल सकेंगे।