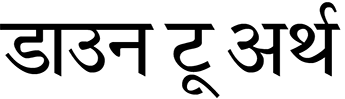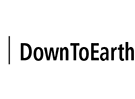सोम बाजार, लॉकडाउन और ट्विटर पर बनती पॉलिसी
हम लोग अपने ट्विटर और अपनी इंस्टाग्राम में इस कदर खोये हुए थे कि हम में से कुछ को यह समझ ही नहीं आया कि वे घरों की और क्यों लौट रहे हैं?
On: Friday 22 May 2020

 लॉकडाउन की वजह से खाली पड़ी सड़कें। फोटो: विकास चौधरी
लॉकडाउन की वजह से खाली पड़ी सड़कें। फोटो: विकास चौधरी लॉकडाउन को दो माह होने वाले हैं। पिछले लगभग 60 दिनों से जेहन में बार- बार एक ही ख्याल आता है- उन तमाम लोगों, जिनसे मैं ' 'सोम बाजार' से छोटा- मोटा सामान खरीदा करती थी, उनका क्या हो रहा होगा? हमारे इलाके में सोम बाजार हर सोमवार चार बजे बाद लगा करता था। पहले यह हाट 'वीर बाजार' के नाम से मशहूर था। लेकिन फिर किन्ही कारणों से हर सोमवार को लगने लगा। सोम बाजार में हर तरह का सामान मिलता है- और अच्छी बात यह है कि यहां अमीर- गरीब सभी शॉपिंग करने आते हैं। यहां 'अर्बन इंडिया' की 'मॉल्स' की दीवारें नहीं हैं, जो आपसे आपके पर्स का मूल्यांकन करवा के ही आपको एंट्री दिलवाएंगी।
सोम बाजार तो एक 'पब्लिक गुड' की तरह है जो सड़कों पर लगता है और हमारे शहरों की देसी रौनक बढ़ाता है। मानो एक मेले की तरह।
आखिरी बार मैं वहां शायद मार्च के पहले हफ्ते में गई थी। उसके पहले कई दिन बीमार रही- ठंड लग गई थी तो जाना न हो पाया था। अकसर जिम से लौटते वक्त वापसी में तरह-तरह का सामान खरीदते हुए लौटा करती थी। जैसे अगरबत्ती, गेंदे के फूल- बिल्कुल ताजे, सब्जी, मौसम के फल। एक बार उत्साहित होकर एक अनानास बेचने वाले भैय्या से पूछा था कि इस बार आम कब तक आएंगे? उन्होंने एक ठेले की तरफ इशारा करते हुए बताया था कि कोंकणी आम शायद वहां अभी ही मिल जाए। मन में पता नहीं क्या सूझी थी कि धमक के दूसरे भैय्या के पास जा पहुंची और पापा के लिए दो किलो आम लेती आई थी। शायद मुझे पहले से ही आम के इस मौसम का संकेत हो गया था।
उसी तरह बांस की छोटी टोकरियां खरीदने की शौकीन रही हूं। घर में छोटी- मोटी चीजों को रखने में काम आ जाया करती हैं, ये टोकरियां- जो ईकोफ्रेंडली हस्तशिल्प के नाम पर बखूबी बिकती हैं। उस दिन भी एक बहुत खूबसूरत बांस की टोकरी लाई थी, जिसमें अभी कुछ लहसुन और कच्ची हल्दी रख दी है।
सोम बाजार अकसर ही मुझे छोटे शहरों और गांवों के ग्रामीण हाट बाजारों की याद दिलाया करता है। मध्यप्रदेश में जब रहा करती थी, तो हर रोज कहीं न कहीं हाट-बाजार के दृश्य देखने को मिलते थे। मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियां बेचते कुम्हार भाई- बहन, जड़ी बूटी को बोरे पर सजाते आदिवासी, उबले हुए मूंगफली दाने और सिंघाड़े, जंगली फल बेर, करौंदा, सजावट का सामान, बंदनवार, पशुओं के लिए चारा, खेतों से लायी गयी हरी लाल भाजी।
फर्क बस इतना ही था कि वहां भीड़ नहीं होती थी। लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदकर अपने काम पर लग जाया करते थे। कई बार सड़क पर खड़े होके भुट्टे, चाय, आदि का सेवन किया है, मध्यप्रदेश के घने जंगलों से लगे गांवों की किसी सड़क के किनारे।
बिलकुल वैसे ही दृश्य यहां दिल्ली में सोम बाजार में देखने को मिलते रहे। यहां भीड़ ज़्यादा होती थी। सिर्फ ग्रामीण लोग ही नहीं तथाकथित 'स्मार्ट सिटीज़' के लोग भी अनगनित चीज़ें खरीदते नज़र आते थे । दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह वही महानगर एवं स्मार्ट सिटीज़ हैं, जिन्होंने सैकड़ों मज़दूर - जो कि कभी ग्रामीण हाट छोड़कर शहर में हाट लगाने, काम ढूंढते आये थे - उनको रातों रात अनाथ बना दिया – जब कि उनके बनाये कमरों में हम सुरक्षित बैठे रहे।
पिछले साल सर्दी के दिनों की बात है। अगरबत्ती वाले भैय्या जो एक जूस वाले के बगल में अपनी साइकिल पर ही दुकान लगाते थे - उन्हें कुछ हफ़्तों से मैंने देखा नहीं था। फिर एक दिन अचानक ही जब मैंने उन्हें कहीं और खड़ा पाया तो पूछा कि वे कहां गए थे ? मुझे देख वे भी उत्साहित होकर बोले- बेटे की शादी है, भागलपुर गए थे। पैसे का कुछ इंतजाम करने। बेटे का ब्याह होने वाला था, सो गांव में व्यवस्था करके आये थे, और साथ ही छठ पूजा भी मना आये थे। मैंने बात करते- करते अगरबत्ती खरीदी और उनसे विदा ले, आगे निकल आयी।
आज इस लॉकडाउन में कई बार उनका ख़याल आता है। मुझे नहीं पता कि उनके बेटे की शादी हो गयी या नहीं । बुज़ुर्ग तो वे थे ही, लेकिन अपने ऊपर शर्म आती है कि जिनको भैय्या बोल कर इतने साल अगरबत्तियां खरीदीं आज उनका नाम भी मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने कभी पूछा ही नहीं था उनका नाम, क्योंकि मेरे जैसे सभी शहर के दुनियादारी समझने वाले, गांव की सादगी से दूर अपने मोबाइल फ़ोन और अपनी संवेदनहीनता में इतने खोये हुए थे, कि हम भूल गए कि यह देश दिल्ली और मुंबई की इमारतों से नहीं बल्कि उनके लाखों- करोड़ों मज़दूरों से बनता है।
उन सज्जनों से बनता है जो "इनक्रेडिबल इंडिया" जैसे स्लोगन्स की नींव हैं। जिन्होंने हमारे शहर एवं हमारे घर बनाये, हमें वे सहूलियतें प्रदान कीं, जो हमें चाहिए थीं। जिन्होंने हमारी पार्टियों और शादियों को अपने फूलों द्वारा सुन्दर बनाया। जिन्होंने एक थकी दोपहर में हमें बेल का शरबत पिलाया, या कुल्हड़ की चाय सर्दियों की शाम में हमें परोसी। आगरा एक्सप्रेस वे पर ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट का वह दृश्य जब ऑनलाइन न्यूज पर देखा तो आँखें नम हो आईं - न जाने कितने ऑटो रिक्शा में आज तक बैठी हूं। चाहे दिल्ली हो, मुंबई, हो, या फिर मध्य प्रदेश का सिवनी जिला। कितनी बार न जाने कितने अनगिनत ऑटो वाले भैय्या ने हमें अपने स्थान, अपने घर सुरक्षित पहुंचाया था, और आज जब वे स्वयं ही अपने घरों को निकाल दिए गए, तो पहुँच नहीं पाए।
हम यहां कैसे पहुंच गए? कैसे हम इतने संवेदनहीन हो गए कि पहली बार जीवन में हम गरीबी की इस त्रासदी को रोज़ अपनी आँखों के सामने एक सैलाब कि तरह उमड़ते हुए देख रहे हैं?
शायद वे हमारे जीवन की रग- रग में जाने अनजाने ही बस गए थे, और हम उनके होते हुऐ भी अंधे हो गए थे। शहरों की भागम भाग में व्यस्त रहे। हम भूल गए कि वे भी हमारे बीचों बीच हैं। लेकिन हम लोग अपने ट्विटर और अपनी इंस्टाग्राम में इस कदर खोये हुए थे कि हम में से कुछ को यह समझ ही नहीं आया कि वे घरों की और क्यों लौट रहे हैं? और आये भी कैसे ? जिस देश में सेलिब्रिटी और जाने माने लोग जब पहले कुछ दिन पूरे देश को इंस्टाग्राम पर हाथ ही धोना सिखा रहे थे - वे मज़दूरों की इन गंभीर परेशानियों को कैसे समझ सकते थे?
'इनफॉर्मल सेक्टर' तो शायद बस 'इंग्लिश कॉन्फरेंसेस’ और सेमिनार्स में ही सुनने में अच्छा लगता आया है, सालों से। शायद इसीलिए आज भी हम ठीक- ठीक नहीं जानते कि भारत में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं? जानेंगे भी कैसे? कांफ्रेंस ख़तम, हमारी 'हाई -टी' ख़तम, और उसी के साथ ज़िम्मेदारी भी। सोशल सेक्टर कि इस त्रासदी को अपनी आँखों के सामने कितनी ही बार देखती आयी हूँ - जहाँ गरीबी पर अंग्रेजी में संवाद होता है, लेकिन जिस गरीब के ऊपर वह संवाद हो रहा है - उस गरीब के कानों तक 'पॉलिसी मेकर्स' कि यह आवाज़ नहीं पहुँचती।
शायद यही कारण है कि किसी ने सोचा ही नहीं कि भारत में अधिकतर मज़दूर अपने इन्ही हाट बाज़ारों से पैसा कमा के मनी आर्डर के द्वारा अपने गांव वापस भेजा करते थे। हमने नहीं सोचा कि वह अगरबत्ती वाले भइया अपने घर से दूर रहते हैं, परिवार को भागलपुर के किसी गांव में छोड़ कर। वही गांव जहाँ मेरे जैसे कई अन्य पॉलिसी समझने के इच्छुक लोग महज़ 'टूरिज्म' के लिए जाते रहे हैं - जिन्हें लगा कि चार दिन गांव घूम के, फोटो इत्यादि लेकर वे 'रूरल-अर्बन डिवाइड' समझ गए हैं।
आज सोचा करती हूं कि जैसे-जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं, वैसे - वैसे क्या कभी वह भीड़ भरा उत्सवीय नज़ारा अपने पड़ोस के सोम बाजार में दोबारा देखने को मिलेगा? सोशल डिस्टेन्सिंग, हैंड सेनिटाइजर, फेस मास्क के बीच में क्या सब को पहचान भी पाउंगी? और उन्हें पहचान भी लिया तो शायद खुद की इस शर्मिंदगी से बच पाऊँगी? क्योंकि इस आपदा में हम और आप साथ जरूर हैं, लेकिन हम और आप सदियों से बनती हुई उस संवेदनहीनता के उतने ही गुनहगार हैं, जितने कि वे लोग जिनकी पॉलिसी शीशों के महलों में बनती आयी और जिनकी आवाज़ ट्विटर तक ही थम कर रह गयी। गांव और शहर के उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक नहीं पहुंची। पहुँचती भी कैसे ? सोम बाजार न तो कोई ऐप है, और न ही वो डिजिटल इंडिया का कोई स्मरणीय स्मारक।