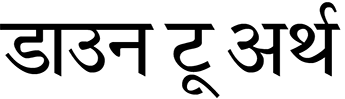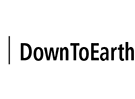मांस की बजाय गेहूं: मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने बदला अपना खानपान
गरीबी और सरकारी राशन पर भरोसे के चलते बदल रही आदतें, हालांकि खानपान में विभिन्नता पर पड़ रहा नकारात्मक असर
On: Wednesday 18 May 2022

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में रहने वाले भील व भिलाला समुदाय के आदिवासियों के खानपान में पिछले कुछ सालों में बदलाव आ रहा है। इन लोगों में से अधिकांश ने अपनी खुराक में परंपरागत अनाजों के साथ ही मांस खाना या तो छोड़ दिया है या फिर कम कर दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश में आदिवासियों की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में उनके खानपान में ये बदलाव उनके स्वास्थ्य और पारंपरिक-ज्ञान पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।
2011 की जनगणना के लिहाज से इन दोनों जिलों में आदिवासी बहुसंख्यक हैं।
1980 के दशक से मध्य प्रदेश में बच्चों और टीबी के रोगियों में कुपोषण पर काम करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था चाइल्डफंड इंडिया, के मुताबिक उनकी खुराक में ये बदलाव करीब 15 साल पहले आना शुरू हुआ। संस्था के प्रतिनिधि ने डाउन टू अर्थ से कहा, ‘ उसी दौर में इन लोगों ने बाजरा और ज्वार की जगह गेहूं खाना शुरू कर दिया और ज्यादातर परिवारों ने मांस खाना छोड़ दिया।’
इस बदलाव में कई कारकों ने अपनी भूमिका निभाई: खराब आर्थिक स्थिति, ऐसी फसलों की पैदावार जो ज्यादा फायदेमंद हों और सामुदायिक वितरण व्यवस्था पर उस तरह की निर्भरता और भरोसा, जो पारंपरिक भोजन और आदतें ला पाने में नाकाम रहीं।
मधु हतिला जब अपनी किशोरावस्था में थी तो अलीराजपुर के सेजवाड़ा गांव में रहने वाला उनका परिवार अपने घर में कई जानवरों के साथ मुर्गे भी पालता था। ऐसा केवल उनके गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में होता था। इससे पहले यह परंपरा पड़ोस के झाबुआ जिले में भी थी।
आज इन गांवों में मुर्गे बड़ी मुश्किल से दिखते हैं। गाय और बकरियां भी केवल बड़े परिवारों वाले लोग पाल रहे हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके।
इस संवाददाता ने झाबुआ जिले के जिन गांवों झपरी, नवापारा व गोलाबड़ी और अलीराजपुर के सेजवाड़ा व रिंगोल गांवों का दौरा किया, वहां भील व भिलाला समुदाय के आदिवासियों में आज की तारीख में कोई मांस खाने वाला नहीं मिला।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ (एनआईआरटीएच) के 2009 के अध्ययन के मुताबिक, ऐतिहासिक रूप से ये आदिवासी मांस खाते रहे हैं और मांसाहारी खाने को ही प्राथमिकता देंगे। हालांकि अध्ययन में यह भी पाया गया कि गरीब होने के चलते आदिवासी महीने में दो या तीन बार से ज्यादा मांस नहीं खा पाते या फिर किसी पारिवारिक कार्यक्रम या त्योहारों में मांस खाते हैं।
नेशनल न्यूट्रिशन मॉनीटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) के मुताबिक, देश के आदिवासियों की आबादी में 1988-90 के दूसरे और 2008-09 के तीसरे सर्वेक्षणों में प्रतिदिन, प्रति खुराक तीन यूनिट प्रोटीन की कमी दर्ज की गई थी।
इस रिपोर्ट में पाया गया कि इस अवधि के दौरान, सभी आयु-समूहों में प्रोटीन-कैलोरी पर्याप्तता वाले व्यक्तियों का अनुपात कम हो गया। प्रोटीन, ऊर्जा और कैलोरी के मामले में पर्याप्त आहार लेने वाली आबादी का अनुपात कम पाया गया। अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों में यह 29 से 32 फीसदी रहा तो वयस्कों में 63 से 74 फीसदी और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में 25 फीसदी रहा।
यही नहीं, उनकी खुराक में एक महत्वपूर्ण बदलाव और भी आया है और वह है मुख्य अनाजों का कम होना।
अलीराजपुर जिले के रिंगोल गांव की लड्डो हलिता कभी सूरज उगने के साथ अपने दिन की शुरुआत बाजरा पीसने से करती थीं। बाजरे की फसल उनके घर के पीछे पड़ी जमीन में की जाती थी। पूरा परिवार बाजरे के आटे की बनी रोटियां खाता था। हालांकि यह चालीस साल पहले की बात है।
वह कहती हैं- ‘ बाजरा पीसने में मेहनत तो बहुत लगती थी, लेकिन उससे मेरे हाथ मजबूत हो गए। आज तो हम पास के बाजार में गरीबी रेखा का कार्ड दिखाते हैं और गेहूं खरीद लेते हैं।
पहले कुदरती तौर पर होने वाली फसलों जैसे ज्वार, बाजरा और मक्के पर आदिवासियों का अटूट भरोसा था। इसके अलावा जंगल से पत्तेदार सब्जियां और फल जैसे पुवड़िया, राजन, किकोडे और चवली आदि भोजन का दूसरे प्रमुख स्रोत थे।
आज उनके खाने में मुख्य तौर पर गेहूं, दाल और चावल शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा वे मौसमी सब्जियां भी लेते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मॉनीटरिंग ब्यूरो (एनएनएमबी) के अध्ययन के मुताबिक, उनकी खुराक से प्रति कैलोरी 50 ग्राम अनाज प्रति दिन कम हो गया है, हर दिन लिए जाने वाले विटामिन ए में 117 माइक्रोग्राम की कमी आई है जबकि कुल एनर्जी एक दिन के लिहाज से 150 किलो कैलोरी कम हो चुकी है।
मजबूरी के चलते आया बदलाव
इस बदलाव के पीछे का मुख्य कारण पैसा है। पारंपरिक अनाज उगाने और बेचने वालों को यह महसूस होने लगा था कि इन अनाजों की मांग कम हो रही है। इसलिए उन्हानें गेहूं, सोयाबीन और दूसरी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया।
इन फसलों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और यहां की भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मार्च 2022 में, झाबुआ को एमपी पेयजल परिक्षण अधिनियम के तहत ‘पानी की कमी वाला’ जिला घोषित किया गया था।
इसके अलावा आजीविका के लिए खेती पर रहने वाले लोग अब सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन पर भरोसा करने लगे हैं। साथ ही वे टमाटर, बैंगन, आलू और भिंडी जैसी मौसमी सब्जियां भी उगाते हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, समय के साथ देश के आदिवासियों की खुराक एकांगी और कम पोषण वाली होती चली गई है।
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में सामुदायिक पोषण की प्रमुख डॉ सुपर्णा घोष जेरथ ने इस बात को रेखांकित किया कि पूरे देश में, यहां तक कि ग्रामीण इलाकों में भी पोषण को लेकर तेज संक्रमण का दौर जारी है।
इसके परिणामस्वरूप लोगों के लिए पोषणयुक्त आहार की कमी पड़ती है। इस स्थिति के लिए विविध, पोषक तत्वों से भरपूर स्वदेशी खाद्य पदार्थों और उनके स्थायी उपयोग के बारे में पारंपरिक-पारिस्थितिक ज्ञान के क्षरण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
उन्होंने कहा, - ‘कुदरती फसलों की लागत बढ़ने, जलवायु-परिवर्तन, परिवार के सदस्यों के पलायन करने, गरीबी और अन्य वजहों के चलते देश का आदिवासी समुदाय अब बाजार के खाद्यान्नों पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। हालांकि सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला अनाज जो स्थानीय बाजारों से मिल रहा है, वह एकांगी, खराब गुणवत्ता का और कम पोषण वाला है। यही वजह है कि जैव विविधता वाले क्षेत्रों में रहने के बावजूद आदिवासी समुदाय कुपोषित हैं और उसका स्वास्थ्य खराब है।”
आईसीएमआर के तहत राष्ट्रीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉ हेमलता आर का कहना है कि देश के आदिवासी समुदाय के खानपान की आदतों में बदलाव लाने वाले कारकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी एक कारक है। आदिवासी समुदायों और क्षेत्र में काम करने वाले शोधकर्ताओं के अनुसार, सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सांस्कृतिक रूप से स्वदेशी लोगों के आहार के अनुकूल नहीं है।
हालांकि इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, बेगलुरू में आदिवासियों के स्वास्थ्य पर काम करने वाले प्रशांत एन श्रीनिवास की राय इससे अलग है। वह डाउन टू अर्थ से कहते हैं, ‘ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दोष देना एक तरह से खराब स्वास्थ्य संकेतकों पर आरोप लगाना भी है। लोगों को यह सोचना चाहिए कि इससे कम से कम आदिवासियों को भूख से तो नहीं लड़ना पड़ रहा।
इस योजना में सांस्कृतिक अनुकूलन की कमी ने खुराक में बदलाव लाने में बदलाव किया है। इसके मिलने वाले अनाज में शायद की कोई प्रोटीन हो, इसने शाकाहार को बढ़ावा दिया और लोगों को काफी हद तक चावल पर निर्भर कर दिया।
संस्कृतिकरण की भूमिका
इन दोनों जिलों में कुछ आदिवासी समुदायों के लिए मांस से दूर जाने का कारण उनकी आस्था भी थी।
विकास संवाद मानव-विकास संसाधन संगठन से जुड़े एक खाद्य अधिकार कार्यकर्ता सचिन जैन ने डाउन टू अर्थ से कहा, ‘आदिवासी समुदाय का संस्कृतिकरण उनके आहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसलिए उनका स्वास्थ्य बदल रहा है। इस समुदाय में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाने का चलन बढ़ रहा है।, जिसका एक उदाहरण लोगों का शाकाहारी होना है।’
छत्तीसगढ़ में, भूमि के क्षरण, वन जैसे खाद्य-स्रोतों तक पहुंच में कमी, खेती में प्रयोगों की कमी और चारागाह के नष्ट होने के कारण आदिवासियों का आहार समय के साथ सिकुड़ गया है।
बाल रोग विशेषज्ञ और ग्रामीण छत्तीसगढ़ में स्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल- ‘जन स्वास्थ्य सहयोग और संगवारी’ के संस्थापक सदस्य योगेश जैन ने हरित क्रांति से उत्पन्न एक प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डाला।
उनके मुताबिक, ‘ पिछले तीस सालों में केवल पारंपरिक अनाज के अनुकूल जमीन पर गेहूं और चवाल की खेती इसलिए शुरू हो गई क्यांकि सरकार ने इसे समर्थन दिया। पारंपरिक अनाजों की खेती को इस हद तक हतोत्साहित किया गया कि अब कई युवा लोग इसकी कई किस्मों की पहचान तक नहीं कर सकते।’
वन भी देश के आदिवासी समुदायों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2018 ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में आधे से अधिक आदिवासी आबादी अपने पारंपरिक आवासों से बाहर चली गई है।
यही नहीं, 2001 से 2011 के बीच खेती करने वाली आदिवासी आबादी की तादाद में भी दस फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। इसी दौरान खेती में काम करने वाले मजदूरों की तादाद नौ फीसदी बढ़ गई।
यूनिसेफ के एक बयान में पाया गया है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा समेत कुछ अन्य राज्यों के आदिवासियों ने भूमि अलगाव, विस्थापन और कम मुआवजे के जख्मों को सबसे ज्यादा झेला हैं।
श्रीनिवास के मुताबिक, वन अधिकारों को लागू करने के फौरी तरीके और वन विभाग की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भी आदिवासियों की अपनी भूमि और जंगल पर निर्भरता को कम किया है।
वह कहते है, ‘ आदिवासियों के आसपास की पूरी आर्थिकी इस तरह से बदल चुकी है कि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहने के अलावा उनके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। अब उन्हें आय वाले आर्थिक-तंत्र में शामिल होना और खानापान की आदतों में बदलाव लाना ही पड़ेगा।’