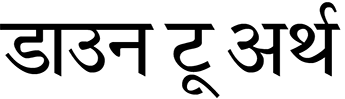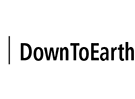“भारत को दवा शोध में अगुवाई करनी होगी”
लैंसेट कोविड-19 कमिशन के सदस्य व अमेरिका स्थित हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में लेक्चरर प्रशांत यादव ने दवाओं के मुद्दे पर डाउन टू अर्थ से बात की
On: Wednesday 12 January 2022

 कोविड-19 के उपचार के लिए दुनियाभर में दवा बनाने का उत्साह क्यों ठंडा है?
कोविड-19 के उपचार के लिए दुनियाभर में दवा बनाने का उत्साह क्यों ठंडा है?
इसके कई कारण हैं। पहला, कई ऐसी दवाओं को कोरोना में इस्तेमाल किया गया जिन्हें दूसरी बीमारियों में दिया जाता है (रिपरपस्ड ड्रग)। लेकिन ऐसे प्रयास विफल रहे। इसने उत्साह कम कर दिया। दूसरा, दवाइयां हर तरह के राजनीतिक विवादों में घिर गईं, चाहे वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो या आइवरमेक्टिन। इससे मरीजों में दवाओं के प्रति संशय बना हुआ है।
दवा कंपनियों के सामने भी कड़ी चुनौती है। इस स्थिति को देखने का एक और तरीका है। टीका विकसित करने में बहुत प्रतिस्पर्धा है। लेकिन चिकित्सीय उपचार के लिए दवाएं बनाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जो भी पहली प्रभावी दवा के साथ आएगा, उसे बहुत कुछ हासिल होगा। सरकारों को उन्हें अग्रिम रूप से थोक आदेशों के साथ प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जैसा वैक्सीन के लिए किया था।
क्या निम्न और मध्यम आय वाले देशों को उच्च आय वाले देशों की तुलना में चिकित्सा विज्ञान पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है?
हां, लेकिन पहले एक ठीक-ठाक दवा की आवश्यकता है। फिर, सरकारों को खुद से यह पूछने की जरूरत है कि क्या उनके पास दवा उत्पादन और वितरण के लिए कोई तंत्र है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अपने कम टीकाकरण कवरेज के कारण यह प्रयास और अधिक करने की आवश्यकता है। जोखिम बस यह है कि यदि यह तंत्र बना लिया गया और शोध में कोई बहुत कारगर दवा नहीं मिली तो उस तंत्र का क्या होगा। लेकिन यह तंत्र आगे आने वाली महामारियों में जरूर मददगार साबित होगा यानी विकसित किया गया तंत्र बेकार नहीं जाएगा।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (एमएबी) ने कोविड-19 के उपचार में बेहतर नतीजे दिए हैं लेकिन क्या वे अपनी उच्च उत्पादन लागत के साथ भारत के लिए व्यवहारिक है?
एमएबी दवाओं के शुरुआती संकेत अच्छे हैं। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि टीकों की तरह इनका वितरण असमान रूप से होगा। उनकी लागत न केवल इसलिए अधिक है क्योंकि लोग दावा करते हैं कि अनुसंधान का यह क्षेत्र महंगा है, बल्कि इसलिए भी कि प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारत जैसे देशों के लिए रेमडेसिविर (यदि यह प्रभावी सिद्ध हो जाती है) जैसी दवाएं बेहतर विकल्प हैं क्योंकि इसका उत्पादन कई देशों में किया जा सकता है और कंपनियां दवा का अपना मालेक्यूल भी बना सकती हैं। ये दोनों बातें एमएबी दवाओं पर लागू होना मुश्किल है।
एमएबी दवाओं का उत्पादन मुश्किल है। ये दवाएं जनता के लिए सस्ती नहीं हैं। हम इससे कैसे उबर सकते हैं?
दवाओं के महंगे होने के अलावा एक तथ्य यह भी है कि इनमें से अधिकांश दवाएं जो फिलहाल उपलब्ध हैं, चाहे वह एमएबी, रेमडेसिविर या आईएल-6 ब्लॉकर्स- अस्पताल में ही दी जानी है। जब इसे ध्यान में रखा जाता है तो भारत जैसे देश में उपचार की कुल कीमत काफी अधिक हो जाती है क्योंकि अस्पताल में रहने का खर्च भी जुड़ जाता है। अब चुनौती ऐसी दवाओं को विकसित करने की है जिसे लोग खुद ले सकें। हमें उन विकल्पों के बारे में भी सोचने की जरूरत है जो बीमारी के पहले चरण के लिए उपलब्ध हों, न कि केवल तब जब लोग भर्ती हों और ऑक्सीजन पर हों।
महामारी की हालिया दूसरी लहर के दौरान भारत अलग तरीके से क्या कर सकता था?
भारत के मामले में केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य एजेंसियों को पहले से ही दवाओं के लिए परीक्षण शुरू करना चाहिए था जिनका उपयोग हल्के संक्रमण के लिए किया जाए और जिन्हें खाया जा सके। हमें तीन परिस्थितियों के बारे में सोचना होगा। पहला, हम प्रभावी एंटीवायरल दवाओं के शोध में सफल हो गए। दूसरा, हमारे पास कोई प्रभावी एंटीवायरल नहीं हुआ और हमें एमएबी पर ही निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा, रिपरपस्ड दवाएं रोग की गंभीरता के शुरुआती दिनों के लिए ही प्रभावी सिद्ध होगी। हर एक परिस्थिति में विनिर्माण, मूल्य निर्धारण, वितरण और विनियमन का अलग अलग तरीका होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने अभी तक इन तीनों परिस्थितियों पर काम शुरू किया है।