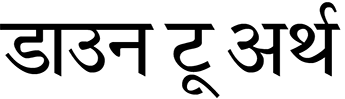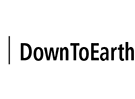महज किताब ही नहीं, आईना भी
“जल थल मल” हमारे समाज, विज्ञान और पर्यावरण के अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालती है
On: Tuesday 12 February 2019

“जल थल मल” किताब साढ़े तीन अरब साल पहले के एक घटनाक्रम के जिक्र से शुरू होती है। यह वह दौर था जब धरती पर केवल एक कोशकीय जीव पनपते थे। तब साएनोबैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से आई क्रांति ने धरती की रूपरेखा बदल दी। किताब इस रहस्य से भी पर्दा उठाती है कि कैसे ऑक्सीजन नामक विषैली गैस जीवन का आधार बन गई। धरती बचाने के तमाम प्रयासों को लेखक सोपान जोशी सिरे से खारिज करते हुए दलील देते हैं कि यह मानना भारी भूल होगी कि आज पृथ्वी को बचाना जरूरी है। इस ग्रह पर जीवन हमारे किए धरे से नहीं आया है और न ही हमारे मिटाए मिट सकेगा।
किताब हमारे बीते कल और आज का वैज्ञानिक व प्रमाणिक दस्तावेज है जो हमें पर्यावरण, विज्ञान और समाज के उन विषयों से रूबरू कराता है जिनके बारे में हम आमतौर पर बात करने से कतराते हैं। “जल थल मल” एक आईना है जो हमें हमारा बदनुमा चेहरा भी दिखाता है। लेखक मल अथवा टट्टी अथवा गू के बारे में खुलकर बात करता है और उसके विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं की आलोचनात्मक समीक्षा भी। किताब साफ-सफाई के काम में लगे उस तबके की जिंदगी में गहराई से झांकती है जो अब भी पीढ़ी दर पीढ़ी मल रूपी बोझ ढो रहे हैं। लेखक ने स्वच्छ भारत अभियान और इसके नाम पर बन रहे शौचालयों पर भी सवाल उठाया है और वर्तमान सफाई व्यवस्था पर भी। वह भी वाजिब और ठोस वजहों के साथ।
“जल थल मल” हमें ऐसे लोगों से परिचित कराती है जो चकाचौंध से दूर हैं लेकिन पर्यावरण के शिल्पकार की भूमिका निभा रहे हैं, उसे गढ़ रहे हैं। चाहे वह कोलकाता के मछुआरे हों या ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के संरक्षक और अभिभावक ध्रुबोज्योति घोष अथवा रेलवे को बायोडाइजेस्टर शौचालय देने वाले लोकेंद्र सिंह।
लेखक जल स्रोतों के प्रदूषण को सीवर और शौचालयों से सीधा जोड़ते हुए सवाल पूछते हैं कि क्या शौचालय बनाना और इस्तेमाल करना ही संपूर्ण समाधान है? अगर हर किसी के पास सीवर का शौचालय होगा तो हमारे जलस्रोतों का क्या होगा? वह साफ कहते हैं कि हमारी सरकार ही नहीं, पढ़े लिखे समाज को उन लोगों से शर्म आती है जो खुले में शौच करते हैं। लेकिन उन्हें अपनी नदियों और तालाबों को सीवर बना डालने में कोई शर्म नहीं आती। किताब पूरी मजबूती के साथ दलील देती है कि शौचालय बनाने भर से शुचिता नहीं आ जाती। खासकर तब जब शौचालय के मैले पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न हो। साथ ही मानती है कि अगर खुले में शौच जाने के लिए इतनी जमीन हो कि मल दूसरे लोगों के संपर्क में न आए और प्राकृतिक आड़ भी बने रहे तो इसे गंदगी फैलाने वाली व्यवस्था नहीं कहा जा सकता।
“शरीर से नदी की दूरी” अध्याय दुनिया भर में नदी प्रदूषण के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालता है। चाहे वह इंग्लैंड की टेम्स नदी का प्रदूषण हो या यूरोप के अन्य किसी देश का। जिस फ्लश संस्कृति पर शहर फल फूल रहे हैं, उसका नकारात्मक पक्ष पुस्तक शिद्दत से उठाती है और बताती है कि हमारे शहरों का जलस्रोतों से संबंध खत्म होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत दूर से पानी छीनकर ला सकते हैं। अपने जलस्रोत बचाने में उनकी कोई रुचि और कोई स्वार्थ नहीं बचा है। लेकिन जलस्रोतों को मैले पानी का पात्र बनाने में शहरों का स्वार्थ है। लेखक दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी दाखिल होती है। यहां नदी एक झील में तब्दील हो जाती है क्योंकि बांध से पानी नीचे नहीं छोड़ा जाता। यहां से सारा पानी दिल्ली के इस्तेमाल के लिए निकाल लिया जाता है। यही वजह है कि लेखक ने दिल्ली जैसे शहरों के आसपास रहने वाले लोगों को अपने जलस्रोतों को शहरों की बुरी नजर से बचाकर रखने की सलाह दी है।
लेखक के अनुसार, दिल्ली का यमुना से संबंध सदा ऐसा नहीं था। अरावली से आने वाली कई नदियां यमुना में मिलती थीं। ये नदियां कई कुओं, बावड़ियों और तालाबों से जुड़ी हुई थीं। दिल्ली के पानीदार इतिहास की झलक इलाकों के नामों में अब भी दिखती है। इनके नाम पर ही हौजखास, मोती बाग, धौला कुआं, झील खुरेजी, हौज रानी, पुल बंगश, खारी बावली, अठपुला, लाल कुआं, हौजे शम्सी, पुल मिठाई, दरियागंज, बारहपुला, नजफगढ़ झील, पहाड़गंज आदि का नामकरण हुआ। लेकिन तथाकथित विकास के लिए इनकी बलि चढ़ गई। दिल्ली का चमचमाता हवाई अड्डा कम से कम तीन तालाबों की बलि पर बना है। पुस्तक बदहाल व्यवस्था के बीच कुछ चमकदार उदाहरण भी पेश करती है। पंजाब में काली वेईं नदी को पुनर्जीवित करने वाले बलबीर सिंह सींचेवाल का किस्सा इसी कढ़ी में शामिल है। उन्होंने लोगों को जोड़कर 160 किलोमीटर लंबी नदी को साफ करके दिखा दिया। पुस्तक में सीवेज तंत्र के प्रदूषण के समाधान के रूप में डीसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम की जरूरत पर जोर देकर बताया है कि छोटी-सी जगह में ये तंत्र स्थापित करके सीवर के मैले पानी का उपचार किया जा सकता है। इसके कई सफल उदाहरण पेश किए गए हैं।
लेखक ने “खाद्य सुरक्षा की थल सेना” अध्याय में यूरिया की समस्या पर रोशनी डालते हुए बताया कि आज दुनियाभर में 10 करोड़ टन कृत्रिम नाइट्रोजन का खेती में इस्तेमाल होता है। इसमें से केवल 1.7 करोड़ टन ही भोजन में आ पाता है। बाकी का 8.7 करोड़ टन नाइट्रोजन पर्यावरण में छूट जाता है। इसके कुछ रासायनिक रूप बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं और उपजाऊ मिट्टी को तेजाबी बना देते हैं। वह मानते हैं भारत और दुनिया को खाद्य उत्पादन में निर्भर बनाने वाला यूरिया अब पर्यावरण के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आज दुनिया की 40 फीसदी आबादी इसी पद्धति से उगा खाना खाती है।
लेखक ने बेहद आम बोलचाल की भाषा में यह किताब गढ़ी है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसे पढ़कर अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। मोटे अक्षर और सोमेश कुमार के चित्रांकन किताब को बोझिल नहीं बनते देते और पठनीयता को बरकरार रखते हैं। लेखक ने गहन शोध के बाद इस पुस्तक को जीवंत रूप दिया है। संदर्भ सूची लेखक की मेहनत की पुष्टि करती है। हिंदी में ऐसी किताब दुर्लभ है। यह हमें आईना भी दिखाती है और कुछ बेहतरीन समाधान भी पेश करती है।