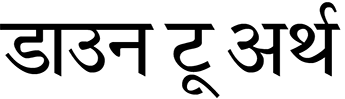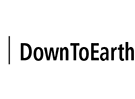साहित्य में पर्यावरण: सहअस्तित्व का पुनर्जन्म
सिनेमाई परदे पर प्रकृति का चित्रण हमें सिर्फ ताली बजाने वाला मूक दर्शक बनाकर छोड़ देता है
On: Monday 01 November 2021

 इलस्ट्रेशन: रितिका बोहरा
इलस्ट्रेशन: रितिका बोहरा - नीरा जलक्षत्रि -
साल 2020 में एक डॉक्यूमेंट्री फीचर ‘माई ऑक्टोपस टीचर’ ने जब ऑस्कर जीता, तो इस ओर पूरी दुनिया का ध्यान गया, पर्यावरण की चिंता को लेकर यह उन चंद दृश्य माध्यमों में से एक थी, जो बिना शोर मचाए हुए आपसे प्रकृति की नाड़ी स्पंदन को महसूस करने का आग्रह करती है इस सिनेमा का आग्रह है कि आप बिना किसी विचार को उस पर थोपे हुए बस उसे शांति के साथ ठहरकर देखें और सुनें। यह सिनेमा आपको जीने का वह फलसफा सिखाने की क्षमता रखती है, जिसने आदिम युग से मनुष्य को गढ़ा है। अपनी दृश्य भाषा के जरिये यह डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर अलग तरह से दर्शकों से संवाद कायम करती है हालाँकि प्रकृति को गौर से देखने का आग्रह करने वाले कई दृश्य पहले भी सिनेमा में आये हैं, लेकिन ऐसे दृश्यों की संख्या काफी कम है, इस सन्दर्भ में ‘माई ऑक्टोपस टीचर’ एक बेहतरीन मिसाल है, जहाँ मनुष्य की कहानी पीछे है और प्रकृति को महसूस करने का का धैर्य पहले आता है ।
अगर बात करें सिनेमा में पर्यावरण की, वो वह सिनेमा में हमेशा से किसी न किसी रूप में उपस्थित रहा हैं, प्रकृति के सौन्दर्य को सिनेमा ने हमेशा ही एक रंगमंच की भूमि की तरह इस्तेमाल किया, बस उसी तरह जैसे पृष्ठभूमि में अतिरिक्त कलाकार उपस्थित रहते हैं, मानो वो होते हुए भी नहीं होते। दर्शकों का ध्यान उनपर बहुत कम जाता है। प्रकृति की ऐसी ही उपस्थित है सिनेमा में, बस किसी दृश्य को और सुंदर बनाने के लिए, लेकिन दर्शक बस उसी को ठहरकर देखता और सुनता ही नहीं रहता, वह मुख्य पात्र की कहानी के साथ आगे बढ़ जाता है। अब तक सिनेमा ने ऐसा ही अलांकारिक रेखांकन गढ़ा है, जिसमें कहानी किसी इंसान के आसपास ही घूमती रहती है । प्रकृति को ठहरकर सुनने का अभ्यास सिनेमाई दृश्यों में अगर कभी किया भी तो बस किसी किरदार के जरिये ही। प्रकृति को ख़ुद किसी किरदार में ढालकर सिनेमाई दर्शकों के सामने बहुत कम फिल्मों में परोसा गया। हालाँकि शुरू से चले आ रही इस प्रवृत्ति में पिछले तीन दशकों में कुछ बदलाव भी आया है, बीते कुछ दशकों में पर्यावरण के कई मुद्दों को लेकर बहुत बेहतरीन फिल्में बनी हैं जिनमें- ड्रीम्स (अकीरा कुरुसावा 1990), फ़ायर डाउन बिलो, (फ्लिक्स एनिकेस 1997) अ सिविल एक्शन (स्टीवन जैलियन 1998) एरिन ब्रोकोविच ( स्टीवन सोडेनबर्ग 2000) अवतार( जेम्स कैमरून 2009) इत्यादि शामिल हैं। हालाँकि ये सूची लम्बी हो सकती है, अगर इसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट्स फिल्म्स, टेलीविज़न सीरीज़ को भी जोड़ दिया जाए ।
पर्यावरण की चिंता को लेकर ये फिल्में अपने नैरेटिव की वजह से ध्यान भी खींचती हैं और पर्यावरण दोहन के लिए जिम्मेदार कॉरपोरेट को सीधे कठघरे में खड़ा करने की कोशिश भी करती हैं, दुनियाभर में औद्योगीकरण के बाद जिस तरह जंगलों से आदिवासियों और वन्यजीवों को बेदखल कर या उनकी हत्या करके जल-जंगल और ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया और उसे तहस -नहस किया गया है, उसी कॉरपोरेट लालच को प्रतिनिधिक तौर पर एक यूटोपियन ग्रह पर कब्जे की कोशिश करने के रूप में 2009 में आयी फिल्म ‘अवतार’ काफी बेहतरीन तरीके से सामने लाती है ।
पिछले दो दशकों से पर्यावरण की चिंता को लेकर कई डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट्स फिल्म्स, टेलीविज़न सीरीज़ और बड़ी फ़िल्में बनी हैं और लगातार इन सबने मिलकर पर्यावरण विमर्श को सिनेमा की मुख्यधारा की बहस में शामिल करने की कोशिश की है, इस क्रम में टेलीविज़न सीरीज़ ‘चेनोंबिल’ (2019) का नाम खासतौर पर लिया जा सकता है । लेकिन इसी के बरक्स एक दूसरा सच यह भी है, कि जितनी फ़िल्में जलवायु परिवर्तन, परमाणु शक्ति के दुष्परिणाम, प्रकृति के अत्यधिक दोहन और उसे प्रदूषित किये जाने को लेकर बनी हैं, उनसे है । बड़ी संख्या में ऐसी फ़िल्में बनी है जो कहीं न कहीं प्रकृति के ख़िलाफ़ छेड़े गए युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से जायज़ ठहराती हैं। बतौर दर्शक ऐसे सिनेमा को देखते समय विशेषरूप से सावधान रहने की ज़रूरत है ।
अगर गौर से देखें, तो पिछले कुछ-एक दशकों में सिनेमा के जरिये कॉरपोरेट ने दुनिया की एक अलग तरह से ढालने की कोशिश की है, उसने एक्शन फिल्मों, सुपर हीरोज की फिल्मों और किसी अनजान एलियन या भयावह विपत्ति से मानवता को होने वाले संभावित ख़तरों वाली फिल्मों से दुनिया को पाट दिया है । इस क्रम में आप याद करें डायनासोर, एनाकोंडा, शार्क, व्हेल, चिपेंज़ी और हलक सीरीज़ की फ़िल्में। दरअसल सिनेमा ने पिछले कई सालों से अपने दृश्य भाषा के जरिये पर्यावरण को ही मुख्य खलनायक की तरह से रचा है । अक्सर इन फिल्मों का नायक प्रकृति के रूप में गढ़े गए खलनायक पर विजय अभियान पर निकलता है और इस अभियान में वह सबकुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। सिनेमा इस तरह की फिल्मों के जरिये वन्य जीवों के ख़िलाफ़ एक भय का माहौल बनाता है ताकि उनके दमन का रास्ता साफ़ हो सके ।
जबकि असली खलनायक वह व्यावसायिक लालच है, जिसने पूरी पृथ्वी के जीवन को ही संकट में डाल दिया है, मूलतः व्यावसायिक सिनेमा उसे छोड़कर बाकी सबको खलनायक दिखाता है । इन फिल्मों में अब अगर इन फिल्मों के दृश्यों को याद करें तो एक्शन फिल्मों और सुपर हीरोज की फिल्मों में जिस तरह एक-एक दृश्य में प्रकृति को तहस-नहस किया जा रहा होता है और दर्शक दीर्घा में बैठा दर्शक ताली बजाता है, ठीक उसी वक्त उस दर्शक को दृश्य भाषा के जरिये उन दृश्यों का अभ्यस्त भी बनाया जा रहा होता है। ताकि जंगल, पहाड़ और नदियों के दोहन पर मनुष्यों की ख़ामोशी बनी रहे , या वह उस तरह विरोध न करे जैसा हर जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए । क्यूंकि सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन ही संप्रेषित नहीं करता, वह विचार भी संप्रेषित करता है और मानव -मस्तिष्क की कंडिशरनिंग भी करता है । लेकिन कुछ वक़्त से कुछ एक फिल्मों ने और आन्दोलन से इस कंडिशनिंग को तोड़ने की कोशिश भी की है ।
ये संयोग नहीं है कि पर्यावरण विमर्श को लेकर पिछला एक दशक काफी उथल-पुथल भरा भी रहा है, और कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन कोई अवधारणा नहीं रह गया है, बल्कि आज का सच बन गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है,भारतीय सिनेमा भी इससे अलग नहीं है । भारतीय सिनेमा में भी इसी साल यानी 2021 दो उल्लेखनीय फिल्में कुछ अंतराल पर आई हैं एक हिंदी में फिल्म ‘शेरनी’ और दूसरी मलयालम में आई है ‘भूमिका’ । हालाँकि दोनों ही अलग शैली की फ़िल्में हैं और इन दोनों फिल्मों से पहले भी पर्यावरण की चिंता को लेकर ‘पानी’ (2008)’जल’ (2013) ‘इरादा’ (2017), ‘कड़वी हवा’ (2017) जैसी फ़िल्में बनी हैं। दोनों फिल्मों में स्त्री और प्रकृति के संदर्भ को बुना गया है । इनमे इकोफेमिनिज्म का स्वर भी सुनाई पड़ता है। हालाँकि भूमिका को हॉरर फिल्म की शैली में गढ़ा गया है लेकिन स्त्री और प्रकृति को एकमेव करके देखने की गुज़ारिश करती यह फिल्म स्त्री के ज़रिये प्रकृति के दोहन की कहानी को जिस तरह गढ़ती है, वह इस फिल्म की तमाम कमजोरियों के बावजूद इसे इकोफेमिनिस्ट श्रेणी की फिल्म में लाकर खड़ा कर देता है। हालाँकि हॉरर शैली में बने होने के बादजूद यह फिल्म कहीं-कहीं ज्यादा अतार्किक भी बन पड़ी है । बहरहाल इस विषय पर भारतीय सिनेमा में फ़िल्में बनना एक बेहतरीन शुरुआत का संकेत है ।
अब बात करते हैं अमित वी. मसुरकर की फिल्म ‘शेरनी’ की, या फिल्म जिस ख़ामोशी बिना ज्यादा लाउड हुए सिनेमा की दृश्य भाषा के ज़रिये पर्यावरण क्षरण और पितृसत्ता की सांठ-गांठ को बेनकाब करती है, वह इस फिल्म को एक बेहतरीन विजुअल अनुभव में बदल देता है । अमित अपनी इस फिल्म में स्त्री और शेरनी दोनों को एक-दूसरे का रूपक बनाकर पेश करते हैं, जो पितृसत्ता के जंगल में अपने लिए रास्ता बना रही हैं । यह फिल्म इकोफेमिनिज्म विचारधारा को बहुत खूबसूरती से उकेरती है । फॉरेस्ट ऑफिसर विद्या विन्सेंट, आखिर में शेरनी के बच्चों के रूप में वन्य जीव की अगली पीढ़ी को पितृसत्ता के हाथों से बचा लेती है । हालाँकि इस फिल्म का फ़लक और ज्यादा बड़ा है, यह पर्यावरण के मुद्दे से लेकर स्थानीय दलगत राजनीति, कार्यक्षेत्र पर लैंगिक भेदभाव, अवैध खनन, ग्रामीण समाज में रोज़गार की समस्या, वन्य जीवों के शिकार, लाभ के लिए इकोसिस्टम को ख़तरे में डालने और पर्यावरण के मुद्दे पर कोर्पोरेटपरस्त राजनेता और उनकी असंवेदनशीलता और अशिक्षा जैसे कई मुद्दों को एक साथ बहुत बारीकी से उठाती है ।
यह फिल्म स्त्री और प्रकृति के संवेदनशील रिश्ते को नयी तरह से परिभाषित करने की कोशिश भी करती है, साथ ही यह सिर्फ़ समस्या ही सामने नहीं रखती बल्कि एक उम्मीद भी जगाती है, वनमित्रों के रूप में नयी पीढ़ी के ज़रिये, यह फिल्म उम्मीद जगाती है कि भले ही वर्तमान पीढ़ी न समझे, लेकिन आने वाली पीढ़ी ज़रूर प्रकृति और मनुष्य के सह-अस्तित्व के रिश्ते को नए सिरे से समझेगी और बनाएगी । बहरहाल पर्यावरण के मुद्दे पर इस तरह की गंभीरता को हिंदी सिनेमा में देखना सुखद है ।
(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम कॉलेज में सहायक प्राध्यापिका हैं।)