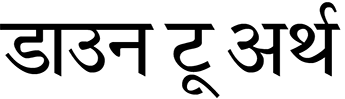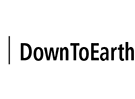साहित्य में पर्यावरण: संघर्ष की आदि कविताएं
आदिवासी साहित्य में जल-जंगल और जमीन को बचाने की आत्मीय आवाजें उठाई जा रही हैं
On: Monday 18 October 2021

 इलस्ट्रेशन: रितिका बोहरा
इलस्ट्रेशन: रितिका बोहरा - संजय कुंदन -
भारत में पर्यावरण संरक्षण दो स्तरों पर दिखता है- एक तो सरकार और एनजीओ की कवायदों में और दूसरा प्राकृतिक परिवेश के बीच रहने वाले आदिवासियों के संघर्ष में। पहले तरह के प्रयासों के तहत सरकार पौधारोपण का अभियान चला रही है। अनेक तरह के निर्माण कार्यों में अब पर्यावरण मानकों को लागू कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे औद्योगिक इकाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की तत्परता दिखाई नहीं देती। प्रदूषण रोकने के लिए बनी संस्थाओं के निर्देशों की अवहेलना भी आम बात है। अरबों रुपये से चलने वाली प्रदूषण विरोधी कई परियोजनाएं मुकाम पर पहुँच नहीं ही पाईं।
इसी तरह कई एक बड़ी संख्या ऐसे एनजीओ की है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को एक अनुष्ठान में बदल दिया है। दौड़, चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताओं और सेमिनारों द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है, उसका कितना लाभ पर्यावरण को पहुँच रहा है या पहुँचेगा, उसका आकलन करना मुश्किल है। पर्यावरण संरक्षण की असली लड़ाई तो जंगल-पहाड़ पर रहने वाले आदिवासी और अन्य लोग लड़ रहे हैं क्योंकि पर्यावरण को होने वाला नुकसान सीधे उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण के लिए उनकी लड़ाई उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन और न्याय के संघर्ष में तब्दील हो गई है और जिसमें प्रकारांतर से जनतंत्र की रक्षा की माँग भी समाहित है। इसलिए यह एक व्यापक संघर्ष हो गया है, जिसमें देश भर के अनेक बुद्धिजीवी भी शामिल हो चुके हैं और साहित्यकारों के लिए भी यह एक बड़ा मुद्दा है। यह मनुष्यता के पक्ष में उठने वाली समस्त आवाज़ों में जगह पा चुका है।
दरअसल साम्राज्यवाद-बाजारवाद-पूंजीवाद की पोषक सत्ता प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए न सिर्फ प्राकृतिक परिवेश को छिन्न-भिन्न कर रही है बल्कि इसका विरोध कर रहे लोगों को भी तरह-तरह से निशाना बना रही है। इसके लिए उसने सीधे-सीधे प्रभावित लोगों को प्रताड़ित करने के साथ-साथ विकास का एक विमर्श भी छेड़ रखा है, जो वर्चस्ववाद का ही विस्तार है। चूँकि समकालीन हिंदी कविता का मूल स्वभाव राजनीतिक है और यह राजनीति कमज़ोर व्यक्ति की राजनीति है, लिहाजा आज पर्यावरण रक्षा का यह संघर्ष हिंदी कविता में प्रमुखता से जगह पा रहा है।
संयोग से हाल के दशकों में हिंदी कविता का दायरा विस्तृत हुआ है और इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी कवि उभरकर आए हैं और ‘हिंदी आदिवासी कविता’ के रूप में एक विशिष्ट धारा हिंदी कविता की व्यापक धारा का हिस्सा बनी है। इन कवियों ने जल, जंगल ज़मीन के संघर्ष को करीब से देखा है इसलिए उनकी कविताओं में इस लड़ाई के बेहद प्रामाणिक चित्र आये हैं। उनकी कविताओं में विकास को लेकर जहाँ तीखी बहस मिलती है वहीं नष्ट होती प्रकृति का हाहाकार भी मिलता है। कवि के भीतर व्याकुलता रहती है कि प्रकृति का सौंदर्य पता नहीं कितने दिन बचा रहेगा।
सभी आदिवासी कवियों ने प्रकृति के साथ अभिन्न रूप से जुड़े अपने जीवन के प्रति गहरा लगाव, आत्मीयता और अपने जीवन मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शायी है। वंदना टेटे लिखती हैंः
हम सब/ इस धरती की माड़/ इस सृष्टि के हाड़/ हमारी हड्डियाँ/ विंध्य, अरावली और नीलगिरि/ हमारा रक्त/ लोहित, दामुदह, नरमदा और कावेरी/ हमारी देह/ गंगा-जमना-कृष्णा के मैदान/ हमारी छातियाँ/जैसे झारखण्ड के पठार/ और जैसे कंचनजंघा/ हम फैले हुए हैं/ हम पसरे हुए हैं/ हम यहीं इसी पुरखा ज़मीन में/ धँसे हैं सदियों से/ हमें कौन विस्थापित कर सकता है/ सनसनाती हवाओं और तूफ़ानों-सी/ हमारी ध्वनियों-भाषाओं को/ कौन विलोपित कर सकता है/ कोई इनसान ?/ कोई धर्म ?/ कोई सत्ता ?/ सिंगबोङा (सूरज) और चांदबोङा को/ इस जवान धरती को/ कौन हिला सकता है/ कह गई है पुरखा बुढ़िया/ कह गया है पुरखा बूढ़ा/ कोई नहीं, कोई नहीं …
महादेव टोप्पो बताते हैं कि प्रकृति से ही आदिवासियों ने जीवन का ज़रूरी पाठ सीखा है। किताबी ज्ञान से वे भले ही अपरिचित हों , पर जीवन के लिए जरूरी दृष्टि की उनके पास कोई कमी नहीं हैः
कुंएं के पास/ पानी पीकर/ गर्मियों में/ मधुमक्खियों के/ उड़ने की ऊंचाई देखकर/ मेरे गांव में बच्चे/ पता लगा लेते हैं/ कहां और कितनी दूरी पर/ मिलेगा मधु का छत्ता/ और वहां कितना है मधु/ जब भी वे इन छत्तों से/ निकालते हैं मधु/ चखा जाते हैं मुझे मधु का स्वाद/ जाहिर है -/ सबको मालूम है/ वे बच्चे स्कूल नहीं जाते/ लेकिन पढ़ लेते हैं/ मधुमक्खियों के अलावा/ वनस्पतियों से,/ जीव जंतुओं, चींटी या मधुमक्खी से/ जीने के जरूरी कई कई पाठ।
बहुत सारी कविताओं में प्रकृति बस स्मृति के रूप में आती है क्योंकि वह लगातार नष्ट हो रही है। युवा कवयित्री जसिंता केरकेट्टा की यह कविता इसका एक उदाहरण है: मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा,/ देखो, यही थी कभी गाँव की नदी।/ आगे देख ज़मीन पर बड़ी-सी दरार/ मैंने कहा, इसी में समा गए सारे पहाड़।/ अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे/ सामने दूर तक फैला था भयावह क़ब्रिस्तान।/ मैंने कहा, देख रही हो इसे?/ यहीं थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान।
ये पंक्तियाँ एक भयावह भविष्य की ओर इशारा करती हैं। इनमें यह आशंका व्याप्त है कि कहीं आज जो कुछ बचा है, वह भी नष्ट न हो जाए। आदिवासी कवियों ने प्रकृति के साथ अपने जीवन की विडम्बनाओं के भी मार्मिक चित्र खींचे हैं। अपनी एक कविता में निर्मला पुतुल लिखती हैंः
तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हज़ारों/ पर हज़ारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारा पेट/ कैसी विडम्बना है कि/ ज़मीन पर बैठ बुनती हो चटाईयाँ/ और पंखा बनाते टपकता है/ तुम्हारे करियाये देह से टप....टप...पसीना...!/ क्या तुम्हें पता है कि जब कर रही होती हो तुम दातुन/ तब तक कर चुके होते हैं सैकड़ों भोजन-पानी/ तुम्हारे ही दातुन से मुँह-हाथ धोकर ?
यह पूरी अर्थव्यवस्था और विकास पर एक सवाल है। आख़िर आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के एक बडे़ तबके को जीवन की बुनियादी सुविधाएँ भी मयस्सर नहीं हैं, जबकि यह तबका अपने श्रम से दूसरों के लिए तमाम सुविधाएँ जुटा रहा है। निर्मला पुतुल की कुछ और पंक्तियाँ देखें:
बाबा!/ मुझे उतनी दूर मत ब्याहना/ जहाँ मुझसे मिलने जाने ख़ातिर/ घर की बकरियाँ बेचनी पड़े तुम्हें/ मत ब्याहना उस देश में/ जहाँ आदमी से ज़्यादा/ ईश्वर बसते हों/ जंगल नदी पहाड़ नहीं हों जहाँ/ वहाँ मत कर आना मेरा लगन
यह आदिवासी जीवन के मर्म को व्यक्त करने वाली कविता है। प्रकृति की गोद में रहने वाले लोग अपने सहज परिवेश में सरल जीवन जीना चाहते हैं। एक लड़की इस बात से डरती है कि वह जंगल- पहाड़ से दूर न हो जाए। वह तथाकथित विकसित समुदायों के सभ्य होने के दावों पर तंज कसती है और कहती है कि उसे आदमी पसंद हैं ईश्वर नहीं। हमारा सभ्य समाज उन्हें पिछड़ा मानता है और खुद को मुख्यधारा कहता है। इस कथित मुख्यधारा पर करारा प्रहार करते हुए महादेव टोप्पो लिखते हैं :
जैसे ही मुख्यधारा में तुम्हारे/ चाहता हूं करना प्रवेश/ मुझे दिखते हैं/ मुख्य-धारा के द्वार पर/ कई असभ्य, अमानवीय, और ढेरों चेहरे क्रूर/ फिर भी कर साहस, समेट हिम्मत/ बह चुका हूं दूर तक बहुत/ मुख्य-धारा में तुम्हारे/ और देख रहा हूं अब/ अक्षर–दूरबीन के सहारे/ न तो वहाँ पवित्रता है/ न सह्रदयता/ न शिष्टाचार/ न सहयोग/ न स्वच्छता/ न सच्चाई/ न ईमान/ न करुणा/ न दया/ न एकजुटता/ नहीं, वहां वह कुछ नहीं, जिसे समझूं मैं/ पवित्रता तुम्हारी मुख्यधारा की/ इसलिए चाहता हूं लौटना/ तुम्हारी मुख्यधारा से छिटककर/ पहाड़ों में बहती क्षीण-धारा के करीब/ अपनी कुटिया, अपने गांव में/ जहां आदमी कम से कम/ आदमी के रूप में नहीं, कोई पशु क्रूर/ आदमी ही है अपने चेहरे के अंदर और बाहर .
आदिवासी कवि साफ कहते हैं कि उन्हें कैसे रहना है, यह वह तय करेंगे। दरअसल वह गैर आदिवासी समुदाय या शासक वर्ग की श्रेष्ठता ग्रंथि को चुनौती देते हैं और यह ऐलान करते हैं कि प्रकृति से तदाकार उनके जीवन में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने हक़ के लिए लड़ेंगे।
अनुज लुगुन कहते हैं: माँ के वक्ष-सा/ भू पर बिखरे पर्वत/ आसमान को थाह लेने की आकांक्षा में/ ज़मीन पर खड़े वृक्ष/ धूप में सूखती नदी के गीले केश/ पान कराते हैं जो दैनिक/ चिड़ियों और जानवरों के आहट से संगीत/ मूक खड़े कह रहे हैं/ कातर दृष्टि से-/ मत ललकारों हमें/ मूक हैं किन्तु/ अपना अधिकार मालूम है/ जो भी प्रतिक्रिया होगी/ वह प्रतिशोध नहीं/ हक़ की लड़ाई होगी/ क्यों तोड़ रहे हो/ हमारे घरौन्दों को/ हमें क्यों सिमटा कर रख देना चाहते हो/ क्या ये जग केवल तुम्हारा है?/ न तेरा न मेरा/ हम दोनों का यह संसार/ कुछ कहता हमसे मूक संसार।
ग्रेस कुजूर की कविताओं में एक गहरा आवेग है। उनका मानना है कि बिना आक्रामक हुए आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा। प्रकृति पर हुए हमले और संसाधनों की लूट के विरुद्ध वे कठोर शब्दों में कहती हैं- हे संगी/क्यों घूमते हो/झुलाते हुए खाली गुलेल/…क्या तुम्हें अपनी धरती की/सेंधमारी सुनाई नहीं दे रही?/क्या अब भी निहारते हो/अपने को/दामोदर और स्वर्ण रेखा के/काले जल में/किसने की है चोरी/भिनसरिया में ठेकी के संगीत की/ और उखाड़ी है किसने/आजी के जाने की कील?/ ‘पुटुस’ तक को/ उखाड़ कर ले जाएँगे लोग/और धन/तुम खोजोगे उसकी बची हुई जड़ों में/अपना झारखंड/हंडिया और दारू से सींचकर/क्या किसी ने उगाया है-/कोई जंगल?”
जाहिर है आदिवासी कविताओं में पर्यावरण को लेकर एक आक्रामक रवैया दिखता है, जो निश्चय ही उनके अनुभव की देन है। शोषण के अंतहीन सिलिसले और लगातार हो रहे वैचारिक हमले ने उन्हें यह रवैया अख्तियार करने पर विवश किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि पर्यावरण रक्षा की असली लड़ाई आम जनता ही लड़ेगी, जिसकी अगुआई आदिवासी समुदाय ही करेगा।
(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हैं।)