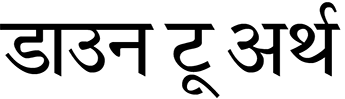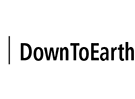वन गुर्जरों के साथ एक दिन
सरकार हमारे और जंगल के बीच के रिश्ते को नहीं समझती। जंगल बिना हम नहीं और हमारे बिना जंगल नहीं
On: Tuesday 05 January 2021

 उत्तराखंड के पश्चिमी तराई की वन गुर्जर बस्ती की महिलाएं। फोटो: स्नेहलता शुक्ला
उत्तराखंड के पश्चिमी तराई की वन गुर्जर बस्ती की महिलाएं। फोटो: स्नेहलता शुक्ला मुजीबुर्रहमान, जिनकी उम्र सौ साल से ऊपर है बताते हैं कि अंग्रेजों को हमारे जंगलों में रहने की अहमियत पता थी। अपने मवेशियों के साथ पहाड़ों में ले जाने को अंग्रेज़ सरकार प्रोत्साहित करती थी। उस सरकार ने ही हमें कभी यहां जंगलों में बसाया था या कम से कम यहां से कभी खदेड़ा नहीं था। उन्होंने कभी हमारे चौड़ या चौर (चराई के प्राकृतिक मैदान) बर्वाद नहीं किए। उस समय तक घास की कभी कमी नहीं हुई। पेड़ भी ऐसे रहे जो हमारे मवेशियों के काम आए। ये सारी वनस्पति मवेशी बड़े चाव से खाते थे।
मुजीबुर्रहमान उत्तराखंड पश्चिमी तराई की वन गुर्जर बस्ती और दिल्ली से तकरीबन 280 किमी. दूर टांडा क्रासिंग के पास बसे बूढ़ा खत्ता तराई क्षेत्र में बसे वन गुर्जरों में से एक हैं। यहां वन गुर्जरों की बस्ती है। जहां दर्जनों परिवार रहते हैं।
मुजीबुर्रहमान बताते हैं कि पहले वन्य जीवों का एक दायरा था और बहुत कम ऐसा होता था कि वो हमारे बाड़ों या बस्तियों की तरफ आए हों। इसकी वजह ये थी कि छोटे-छोटे जानवर घने जंगलों में ही रहते थे। इसलिए जहां छोटे जानवरों जैसे हिरण, चीतल को अपने लिए घास ऊपर ही मिल जाती थी। वहीं शिकारी और बड़े जानवरों को अपने शिकार भी वहीं मिल जाते थे। न हम कभी उनकी दुनिया में जाते थे और न वो कभी हमारी बस्तियों में आते थे।
वह कहां से और कब पहाड़ों में आए होंगे? इस सवाल के जवाब में मुजीबुर्रहमान बताते हैं कि जितना सुनी सुनाई बात याद हैं, उसमें दो बातें हैं – पहली कि हम गुर्जर हैं और सबसे पहले हम गुजरात में रहते थे वहां से कभी कश्मीर गए होंगे और फिर नीचे की तरफ आना शुरू किया होगा। हिमाचल और उत्तराखंड में आज भी रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन गुजरात से संबंध नहीं रहे। वे कभी किसी लालच में यहां वहां नहीं गए, बल्कि अपनी मस्ती और धुन में चलते रहे। कभी कोई मौका आया होगा, बुजुर्गों के सामने तो दो ठिकाने बना लिए। एक जाड़ों के लिए और एक गर्मियों के लिए। गर्मियों में पहाड़ की ऊंचाई पर जाड़ों में नीचे तराई में।
अभी क्या दिक्कतें हैं और क्यों लगता है कि इससे तो अंग्रेजों का राज बेहतर था? मुजीबुर्रहमान बताते हैं कि ये सरकार एक तरह से हमें जंगलों में रहने की सज़ा देती है। वो हमारे और जंगल के बीच के रिश्ते को नहीं समझती। जंगल बिना हम नहीं और हमारे बिना जंगल नहीं। ऐसा हम भी मानते हैं और अंग्रेज़ भी मानते थे, तभी तो उन्होंने हमें बसाया होगा। बड़े-बुजुर्ग बताते थे कि वो हमसे पूछ- पूछ कर बल्कि हमसे ही कहते थे कि अपनी पसंद के पेड़ लगाओ। हम उनके लिए पेड़ ज़रूर लगाते थे, लेकिन अपनी पसंद और ज़रूरत के। अब तो इनकी मर्जी। कितना भी कहो कि इन पेड़ों से घास नहीं पनपेगी, लेकिन मानते नहीं बल्कि धमकी देते हैं। जुर्माना करते हैं और बस्तियाँ तोड़ते हैं।
क्या होना चाहिए कि सब ठीक हो जाए? इसका जवाब मुजीबुर्रहमान नहीं देते, बल्कि पास में बैठे युवाओं की तरफ इशारा करते हैं कि ये जानें। इन्हें तय करना है कि इनके लिए क्या ठीक है।
वन गुर्जर परिवारों में बिना बताए जाने का एक नुकसान यह है कि आमतौर पर दोपहर में महिलाएं घरों में नहीं मिलतीं बल्कि वो चारा लाने के लिए जंगल में जाती हैं। बाड़े में जो बकरियाँ हैं उनके लिए हरा चारा लाना इसलिए अब ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उन्हें चरने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा सकता अन्यथा जंगली जानवर उन्हें अपना शिकार बना सकते हैं। तयशुदा दिन जब दूसरी बस्ती में पहुंचे तो महिलाओं से मुलाकात हुई। हालांकि इन्हें ये पता नहीं था कि कोई बहार से मिलने आने वाला आने वाला है।
जिन महिलाओं से मुलाक़ात हो सकी वो उस समय चूल्हे पर गर्मागर्म रोटियां और आलू मटर की सब्जी बनाती हुई मिलीं। परिचय की गांठ बंधने में थोड़ा वक़्त तो लगा, लेकिन जब एहतराम हो गया तो खुलकर बातें हुईं। कौतूहल से शुरू हुई यह लंबी मुलाक़ात बहनापे में जल्दी ही बदल गयी।
इनके तजुर्बों में अंग्रेज़ सरकार का ज़िक्र तो नहीं था, लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर और मुजीबुर्रहमान की बातों से संदर्भ लेते हुए तुलना लगातार दिमाग में चलती रही। यह इक्कीसवीं सदी की वो महिलाएं थीं जिन्हें बदलते हुए समय का अंदाजा तो है और उनकी ख्वाहिशें भी बदलते समय के साथ चलने की हैं, लेकिन अपनी स्थिति में जीना जानती हैं।
यहां इन बस्तियों में रहते हुए सबसे ज़्यादा डर कब लगता है? यह सवाल काफी देर के बाद पूछने के बाद उन्होंने बताया- जब वन विभाग के लोग अपनी गाड़ियों से अचानक से हमारी बस्तियों में आ धमकते हैं। हमारे मर्दों के साथ गाली-गलौच करते हैं और कई बार हाथ भी उठाते हैं। ये देखकर हम महिलाएं बाहर निकलती हैं। और फिर हमारे साथ भी वही करते हैं। कई बार मर्द बाहर निकलने से मना कर देते हैं तो टॉर्च जलाकर हमें सोते हुए देखने अंदर चले आते हैं।
दूसरा डर तब लगता है जब रात को शौच के लिए अंधेरे में बाहर निकलते हैं क्योंकि आजकल हाथियों का बहुत डर बढ़ गया है। वो बस्तियों की तरफ आने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। घर में शौच क्यों नहीं बनवा लेते? इस सवाल ने जैसे उनकी पीड़ा की नब्ज़ पर हाथ रख दिया हो, एक महिला ने लगभग हाथ पकड़कर उठाते हुए वो जगह दिखलाई जो उसके डेरे के एक किनारे पर थी और जहां टूटी ईंटें, सूख चुके सीमेंट की परतें और एक टूटी टायलेट सीट पड़ी थी। बताया कि – ये बनाया था। चोरी से। एक दिन रेंजर आया और तोड़ गया। गालियां भी दे गया कि बाप की जमीन समझते हो जो यहां कुछ भी करोगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो चाहते हैं कि हर घर में शौचालय हो? चाहते होंगे लेकिन हमारे घर तो अपने नहीं हैं न, ये तो वन विभाग के अधीन हैं।
अच्छा अगर कोई बीमार हो या किसी को बच्चा होना हो तब? ज़्यादातर बच्चे तो यहीं पैदा हो जाते हैं। रात-बिरात कभी कोई दिक्कत आ जाती है तब मुश्किल होती है। वन विभाग छह बजे शाम के बाद कहीं आने जाने नहीं देता। कितने बच्चे बिना हुए ही मर गए। महिलाएं भी। तब बहुत बुरा लगता है। लेकिन एम्बुलेंस बुला सकते हो? हां जैसे एम्बुलेंस तो यहीं होती है? घंटों इंतज़ार के बाद भी नहीं आती।
खाने पीने को तो खूब मिलता है? यह बात उन्हें जैसे नागवार गुज़री और सबसे मुखर महिला साथी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ बताया कि - मेहनत क्या कम है? सुबह तीन बजे से रात आठ बजे तक एक पांव पर रहते हैं।
बच्चों को लेकर क्या सोचती हैं? इस सवाल ने जैसे कहीं भीतर जमा इच्छाओं को उकसावा दे दिया हो? बताते हुए आवाज़ में चहक थी कि हम चाहते हैं कि वो पढ़ें-लिखें और इस असुरक्षा और अपमान से बाहर निकलें। तो बच्चे स्कूल जाते हैं? हां, जब आठवीं में पढ़ने लायक होते हैं तब पहली में नाम लिखवाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो भी स्कूल नहीं जाते। क्यों? स्कूल दूर है और जंगल के रास्ते जाना बच्चों के बस का नहीं है, हम भी उन्हें नहीं जाना देना चाहते। जानवरों का खतरा है। आंगनबाड़ी? थी, पहले पास में ही था जहां से हर महीने राशन मिलता था। कभी कभी वो हमारे डेरों पर आकर बच्चों को पढ़ती भी थी। अभी कब खुलेगी पता नहीं है।
बच्चियों और महिलाओं में स्वच्छता को लेकर ललक है खासकर माहवारी के दौरान लेकिन चाहकर भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और किसी तरह वो अपने अपने लिए उपाय ढूंढती हैं।
मर्दों की दुनिया थोड़ा अलग है। वो हर समय कोई न कोई जुगत करते रहते हैं ताकि ज़िंदगी आसान बनी रहे। संगठन भी बनाते हैं, बैठकों में भी जाते हैं, थाना-कचहरी भी करते हैं। गालियां भी सुन लेते हैं और मार भी खा लेते हैं। फिर मवेशियों में लग जाते हैं। दूध का हिसाब किताब रखना सीखते हैं। नेताओं से भी मिलते जुलते रहते हैं। सभा सम्मेलनों में जाते हैं और नेताओं का चुनाव प्रचार भी करते हैं। जब इस सबका हासिल पूछो तो थोड़ा मायूसी से बताते ज़रूर हैं -कुछ खास होता नहीं है। सालों से जिंदगी इसी जद्दोजहद में बीत रही है कि ऐसा करने से ठीक रहेगा या वैसा करने से।
दही, छाछ, घी और मक्खन से भरपूर भोजन का स्वाद तो वाकई अच्छा था लेकिन इन सबकी कहानियों के साथ जायका अजीब तरह से कसैला था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक भारत के इन नागरिकों के साथ हो रहा अमानवीय और सौतेला व्यवहार ही याद रहा। जो याद रह गया यहां लिखा गया।
लेखिका पिछले 15 सालों से महिला अधिकारों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं और उन्होंने उत्तराखंड में रह रहे वन गुर्जरों के बीच जाकर उनके बारे में जानने की कोशिश की। यह उनका अपना संस्मरण है।