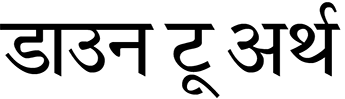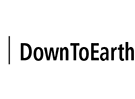डाउन टू अर्थ खास: खानपान में बदलाव से कम हो रही है आदिवासियों की उम्र!
खानपान में परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने के कारण आदिवासी आबादी की जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है
On: Thursday 14 July 2022

 मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अलीराजपुर और झाबुआ में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण व्यापक है (फोटो: तरण देओल)
मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले अलीराजपुर और झाबुआ में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण व्यापक है (फोटो: तरण देओल) 70 वर्षीय जेतली ने अपने परिवार की तीन पीढ़ियों को देखा है, लेकिन यह संख्या उनके पूर्वजों की तुलना में कम है। वह बताती हैं, “जब मैं छह साल की थी, तब मेरे परिवार की कम से कम पांच पीढ़ियां एक साथ रहती थीं।”
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के छापरी गांव में रहने वाली जेतली का मानना है कि उनके भील आदिवासी समुदाय के लोग उतना नहीं जी रहे, जितना कुछ दशक पहले तक जीते थे। डॉक्टरों का कहना है कि देर से शादी और कम बच्चे होने के कारण ऐसा है। जेटली की धारणा पूरी तरह से गलत नहीं है।
स्वास्थ्य पर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपेसनेट इकॉनोमिक्स के शोधकर्ताओं का प्रोसिडिंग्स ऑफ नेशनल अकैडमी ऑफ साइंसेस (पीएनएएस) में हालिया प्रकाशित अध्ययन कहता है कि यदि आप भारत के अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवार में पैदा हुए हैं, तो आप उच्च जाति के हिंदू की तुलना में चार साल कम जिंदा रहने की संभावना रखते हैं।
मार्च 2022 में प्रकाशित यह अध्ययन कहता है कि ऊंची जाति के हिंदुओं की अपेक्षा आदिवासियों की जीवन प्रत्याशा करीब चार साल कम रहती है। इसी तरह दलितों की औसत उम्र लगभग तीन साल और मुस्लिमों की करीब एक साल कम रहती है
(देखें,उम्र में अंतर)।

अध्ययन के अनुमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2010-11 पर आधारित हैं, जिसमें नौ राज्यों- असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विश्लेषण किया गया है।
इनमें से मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति समूहों की जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। पुरुषों की यह 57.4 वर्ष और महिलाओं की 60.1 वर्ष है।
अनुसूचित जनजाति समूहों की जीवन प्रत्याशा हमेशा अन्य सामाजिक समूहों के बीच सबसे कम रही है। जुलाई 2019 में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने एक प्रेस बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि एसटी समूहों की जीवन प्रत्याशा 63.9 वर्ष है, जबकि सामान्य आबादी की 67 वर्ष है। इसमें 2016 के लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन का हवाला दिया गया है जिसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया था।
कम जीवन प्रत्याशा के विभिन्न कारणों में एसटी और गैर एसटी जातियों के बीच स्वास्थ्य व पोषण संकेतकों, शिक्षा के स्तर व गरीबी के स्तर में अंतर को गिनाया गया था। साथ ही एसटी की पारंपरिक जीवनशैली, बस्तियों की दूरी और बिखरी हुई आबादी को भी कम जीवन प्रत्याशा का कारण माना गया।
पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू में अप्रैल 2022 में प्रकाशित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन में भी कहा गया है कि अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में एसटी समूहों की जीवन प्रत्याशा जन्म के समय और पूरे जीवन में सबसे कम है।
हालांकि, इसमें कहा गया कि इस समूह के जीवन प्रत्याशा के आंकड़ों में सुधार हुआ है। 1997-2000 में जन्म के समय अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 57 वर्ष थी, जो 2013-16 में बढ़कर 68 वर्ष हो गई। इस तरह एसटी पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 54.5 वर्ष से बढ़कर 62.4 वर्ष हो गई। ये अनुमान 1997-2000 और 2013-16 के बीच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और नमूना पंजीकरण सर्वेक्षणों के आंकड़ों पर आधारित हैं।
क्या है वजह
अनुसूचित जनजाति समूहों की कम जीवन प्रत्याशा के विभिन्न कारणों में खानपान में परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना, प्रमुखता से शामिल हैं। 87 प्रतिशत एसटी आबादी वाले मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले में यह स्थिति साफ देखी जा सकती है।
झाबुआ के गोलाबाड़ी गांव की निवासी और भील आदिवासी कालिया दुतिया कहते हैं, “20 साल पहले हम प्राकृतिक फसलें उगाते थे। अब रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है। फसलों और डेरी उत्पादों में पहले जैसी गंध नहीं आती।” दुतिया की हां में हां मिलाते हुए अलीराजपुर के सेजावाड़ा गांव के निवासी और भिलाला आदिवासी लड्डो हटीला कहते हैं, “चार दशक पहले जब मैं 20 साल का था, तब मेरे दिन की शुरुआत मोती बाजरा या ज्वार को पीसकर होती था। इनसे रोटी बनती थी। इसने मेरी बाहों को मजबूत बना दिया। अब हम बाजार से गेहूं खरीदते हैं।”
स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले मोती बाजरा, ज्वार, मक्का, जड़ी-बूटियों, फलों और सब्जियों की जगह स्टेपल फूड जैसे गेहूं, दाल, चावल और मौसमी सब्जियों ने ले ली है। दुतिया कहते हैं, “हमने भोजन के लिए जंगल जाना बंद कर दिया क्योंकि इसमें पहले जितने फल और सब्जियां नहीं हैं। बचपन में मैंने कोकोड़ा (स्पिनी लौकी) को खाया था। मुझे याद नहीं है कि पिछली बार में मैंने यह कब देखा था।”
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में प्रोफेसर और कम्यूनिटी न्यूट्रिशन की प्रमुख सुपर्णा घोष जेरथ कहती हैं, “खाद्य उपलब्धता पर जलवायु के प्रभाव, बाजारों को प्राथमिकता और चावल व दालों की संकर किस्मों की खेती के कारण पौष्टिक देसी खाद्य पदार्थों की खपत धीरे-धीरे कम हो रही है।” डाउन टू अर्थ ने दोनों जिलों के पांच गांवों में अपने दौरे के दौरान पाया कि यहां प्रोटीन के प्रमुख स्रोत मांस की खपत लगभग न के बराबर है। यहां कुपोषण का स्तर भी ऊंचा है।
एनएफएचएस (2019-21) के पांचवे चरण में कहा गया है कि झाबुआ में पांच साल से कम उम्र के 49.3 प्रतिशत बच्चे स्टंटेड हैं (उम्र के सापेक्ष कम लंबाई), 17.9 प्रतिशत बच्चे वेस्टेड (ऊंचाई के सापेक्ष कम वजन) और 41.7 प्रतिशत अंडरवेट (उम्र के सापेक्ष कम वजन) हैं। अलीराजपुर में पांच साल से कम उम्र के 34.6 प्रतिशत बच्चे स्टंटेड, 15.4 प्रतिशत वेस्टेड और 31.6 प्रतिशत अंडरवेट हैं। राज्य में काम करने वाले चाइल्डफंड इंडिया की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रतिभा पांडे कहती हैं, “इन आंकड़ों को कमतर आंका जा सकता है, क्योंकि माता-पिता बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में लाने से हिचकते हैं। पारंपरिक दवाओं पर अधिक निर्भरता के चलते चिकित्सा हस्तक्षेप में देरी हो जाती है।”
भोजन में बदलाव
ऐसी स्थिति पूरे देश में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के तहत राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (एनएनएमबी) की 2009 की एक रिपोर्ट, जिसमें नौ राज्यों को शामिल किया गया है, 1985-89 और 2007-08 के बीच जनजातीय क्षेत्रों में कुछ खाद्य पदार्थों की खपत में मामूली गिरावट की ओर इशारा करती है।
इस अवधि के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुशंसित प्रतिदिन का न्यूट्रिशन इनटेक (पोषण का सेवन) भी कम रहा। दूसरे (1988-90) और तीसरे (2008-09) एनएनएमबी सर्वेक्षणों के दौरान बाजरे और अनाज की खपत में प्रतिदिन 50 ग्राम प्रति उपभोग इकाई (सीयू) की कमी आई, जबकि प्रोटीन का सेवन प्रतिदिन 3 ग्राम प्रति सीयू, विटामिन ए का सेवन प्रतिदिन 117 माइक्रोग्राम प्रति सीयू और ऊर्जा का सेवन प्रति सीयू प्रतिदिन 150 किलो कैलोरी कम हुआ।
सीयू को आईसीएमआर द्वारा उम्र, लिंग और शारीरिक गतिविधि के आधार पर कैलोरी खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। एनएनएमबी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न आयु वर्ग के केवल 29-32 प्रतिशत बच्चे, 63-74 प्रतिशत वयस्क और 25 प्रतिशत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं ने प्रोटीन, ऊर्जा और कैलोरी के मामले में पर्याप्त आहार का सेवन किया।
शोध से संकेत मिलता है कि यह बदलाव इस तथ्य के कारण हो सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से प्राप्त गेहूं जैसे अनाज अब आदिवासियों के आहार पर हावी हो गए हैं। सोशल वर्क फुटप्रिंट्स जर्नल में 2017 में प्रकाशित एक अध्ययन कहता है कि जनजातीय समुदाय खेती और खपत की आधुनिक प्रणालियों से वंचित हैं। इसने उन्हें रागी, चामा, बाजरा और मक्का जैसी अपनी स्वदेशी खाद्य वस्तुओं के बजाय पीडीएस से राशन लेने को मजबूर कर किया।”
बाल रोग विशेषज्ञ व जन स्वास्थ्य सहयोग और संगवारी के संस्थापक सदस्य योगेश जैन कहते हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हरित क्रांति के वक्त बाजरा की जमीन को गेहूं और धान के लिए उपयुक्त पाया गया। वह कहते हैं कि इससे बाजरे की पहुंच इतनी सीमित हो गई है कि युवा इसकी किस्मों को भी नहीं पहचान पाते।
स्वास्थ्य देखभाल की कमी
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच के मामले में जनजातीय आबादी अब भी संघर्ष कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20 के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिक जनजातीय आबादी वाले पांच राज्य- महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेलंगाना को छोड़कर सभी को उप-केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में 2,408 उप-केंद्र, 491 पीएचसी और 116 सीएचसी की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 2018 की एक रिपोर्ट “ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया” बताती है कि आदिवासी समूहों को संचारी, गैर-संचारी और मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों के तिहरे बोझ का सामना करना पड़ता है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बैक्टीरियल और वायरल रोग, यौन संचारित रोग और त्वचा संक्रमण की व्यापकता बहुत है।
बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में आदिवासियों के स्वास्थ्य पर काम करने वाले प्रशांत एन श्रीनिवास का कहना है कि वर्तमान स्वास्थ्य डेटा आंशिक तस्वीर पेश करता है। मध्य और दक्षिण भारत में कई वन-संबद्ध समूह जनजातियों के रूप में पहचानते हैं, लेकिन एसटी समूहों के रूप में उन्हें मान्यता नहीं मिली है। ये समूह शहरी और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति समूहों की तुलना में हाशिए पर हैं। वह कहते हैं, “राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में स्वास्थ्य संकेतक दोनों समूहों का औसत है। यदि अलग-अलग सर्वेक्षण किया जाए तो गैर-मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की गरीबी का पता चलेगा।”
सुधार के संकेत
तमाम कमियों के बावजूद अनुसूचित जनजाति की आबादी के स्वास्थ्य संकेतक लंबी अवधि में सुधार दिखाते हैं। 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति की आबादी में शिशु मृत्यु दर 1988 में प्रति 1,000 जन्म पर 90.5 से घटकर 2014 में 44.4 हो गई है। लेकिन जब अन्य सामाजिक समूहों के साथ तुलना की जाती है, तो शिशु मृत्यु दर में अंतर 10 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाता है।
एनएनएमबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1998-99 और 2007-08 के बीच 1-5 आयु वर्ग के अनुसूचित जनजाति के बच्चों में स्टंटिंग 58 प्रतिशत से घटकर 56 प्रतिशत हो गई है। वेस्टिंग भी 23 से 22 प्रतिशत पर आ गई है। इसी तरह अंडरवेट की स्थितियां भी इस अवधि में 57 से 52 प्रतिशत पर आ गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए बच्चों पर रेपिड सर्वेक्षण के अनुसार, 2013-14 तक इन आंकड़ों में सुधार हुआ है। स्टंटिंग के आंकड़ों में 42.3 प्रतिशत, वेस्टिंग में 18.7 प्रतिशत और अंडरवेट की स्थिति 36.7 प्रतिशत बेहतर हुई है। ये आंकड़े रुझानों के थोड़ा बेहतर होने की ओर इशारा करते हैं।