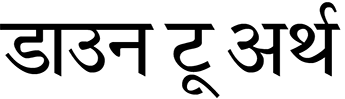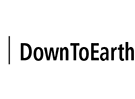जय भीम: सत्य और फंतासी के बीच झूलती एक कहानी
गणतंत्र को बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है, ऐसी समझ वाले लोगों को जवाब दे रही है जय भीम
On: Monday 15 November 2021

 जय भीम फिल्म का एक दृश्य। फोटो: twitter@LijoMolJosee
जय भीम फिल्म का एक दृश्य। फोटो: twitter@LijoMolJosee
सीआईडी के एक आला अफसर का एक झक बड़ा सा कमरा है। अधिकारी वकील से कहता है “ एक पुलिसवाला है जो वकीलों को गिरगिट समझता है और एक वकील है जो पुलिसवाले को दीमक समझता है, और यह दोनों मिलकर एक केस पर काम करेंगे। कमाल की बात है न”.....
“गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है चंद्रू। दैट्स दी ट्रुथ यु नो (आप भी मानेंगे कि यही हकीकत है )”। बातचीत के आखिर में कुर्सी से उठते हुए वकील कहता है , “ मेरी एक रिक्वेस्ट है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आपको किसी से मिलवाना है।”
अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह पर गांव के लोग इकठ्ठा हैं। जहां वकील और सीआईडी का अफसर भी मौजूद है। इकठ्ठा हुए गांव के लोगों को किसी एक वामपंथी पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है, “ पुलिस किस तरह आपको झूठे केस में फंसती है, इसे जानने के लिए वकील साहब अधिकारी को लेकर आये हैं...”
सिलसिला शुरू होता है लोगों की शिकायतों का, फिर बारी आती है एक छोटे से बच्चे की जो कहता है कि, “ मेरे बाबूजी नहीं मिले तो पुलिस मुझे मारने लगी। तब से सकूल में कोई भी चीज गायब होती है तो पहले मेरे बैग की ही तलाशी लेते थे। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया।”
इस तरह का तजुर्बा शायद पुलिस अधिकारी को पहली बार हुआ था, जो उसके चहरे पर साफ झलकता है। बच्चे की बात उससे सुनी नहीं जाती और वह उस कमरे से बाहर निकल आता है। ठीक यही वह सीन है जो ‘जय भीम’ फिल्म को अबतक इस विषय पर बनी तमाम फिल्मों से न केवल अलग करती है, बल्कि इस फिल्म को मील का पत्थर बनाती है।
इस सीन में केवल उस पुलिस अधिकारी का मोहभंग नहीं होता बल्कि इस फिल्म को देख रहे उन तमाम दर्शकों का होता है, जिन्होंने अपनी ‘समझ’ या मजबूरी के तहत यह मान लिया है कि, “गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है”
उस अधिकारी की तरह शायद पहली बार हम उस सच से रूबरू होते हैं कि हमें जबरन मनवाया गया है कि, “गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है”
हमारे देश में पुलिस/अर्धसैनिक बलों का गरीम मासूम लोगों पर अत्याचार कोई नयी बात नहीं। पुलिस द्वारा झूठे मुकदमों में आम लोगों को फंसना भी अब एक ‘आम-बात’ हो गयी है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर पत्रकारों/ पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हम यह भी जानते हैं कि अक्सर दोषी पुलिसवाले पर कार्रवाई नहीं होती या ‘सबूतों’ के अभाव में वे छूट भी जाते हैं और यह सब किसी ‘गणतंत्र को इस देश में बचाने’ के नाम पर होता है।
जनता पर पुलिस के अत्याचार पर यह न तो पहली फिल्म है और न ही आखिरी। न जाने कितनी फिल्में कोर्ट सीन/वकालत की पृष्ठभूमि पर बने। हाल में बनी जॉली एलएलबी भी उसी का एक उदाहरण है, पर ‘जय भीम’ में पहली बार हम शहर के दर्शक आदिवासियों पर हो रहे पुलिसिया जुल्म को इतने खुले ढंग से रखा हुआ देखते हैं।
फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां किसी मवेशियों की तरह लोगों को उनके नस्ल (या जाति!) के हिसाब से कुछ को छोड़ दिया जा रहा है और कुछ को रोक लिया जा रहा है। एक पुलिसवाला अगले से पूछता है , “ इनकी गलती क्या है?”
इसपर पुलिसवाला जवाब देता है,“ यही कि यह पैदा हुए...”
कुछ आदिवासियों को झूठे इल्जाम में पुलिस फंसा लेती है, जिनमें पुलिस की मार से एक आदिवासी की हिरासत में मौत हो जाती है। ‘जय भीम’ की कहानी उन आदिवासियों के केस को लड़ते वकील की कहानी है। देखा जाय तो कहानी में उस हिसाब से नयापन कुछ भी नहीं है।
निर्देशक ने फिल्म के विषय को जिस सहजता और निडरता से चुना वह सहजता फिल्म की किस्सागोई में नहीं है। पूरी फिल्म देखते हुए यही लगता है कि निर्देशक शुरू से आखीर तक इसी असमंजस में पड़ा रहा कि वह एक फीचर फिल्म पर काम कर रहा है या एक डाक्यूमेंट्री पर।
शुरूआती कुछ गांव, आदिवासी समाज के दृश्यों को छोड़ दिया जाय तो पूरी फिल्म में किस्सागोई के नाम पर निर्देशक की बस वह बेसब्री दिखी कि वह तथ्यों को कितनी सच्चाई के साथ दिखा रहा है। तथ्यों के प्रति निर्देशक की इस ईमानदारी ने फिल्म की किस्सागोई को ही ख़त्म कर दिया।
निर्देशक का यह कंफ्यूजन फिल्म के बाकी हिस्सों पर भी है। मसलन फिल्म में निर्देशक ने एक ओर जहां तथ्यों के प्रति बहुत ईमानदारी दिखाई पर जब भी उसे तथ्यों से थोड़ी सी निजात मिली। वहीं यही निर्देशक जाने क्यों ‘स्टीरियोटाइप’ की गिरफ्त में आ गया।
आदिवासी का मतलब गरीब होना एक हद तक सच है पर आदिवासी स्त्री होने का मतलब चहरे पर अजीब क्रीम को पोते हुए रहना कहां का तुक है?
हम भारतीय दर्शक आदिवासियों के नाम पर एक लम्बे समय तक ‘ हुब्बा! हुब्बा! डांस’ और अजीबोगरीब वेशभूषा पहने लोगों को देखने के आदी रहे हैं। बेशक यह पुराने फिल्मों के उस ‘आदिवासी’ के इमेज को तोड़ कर काफी हद तक एक ‘आदिवासी’ को एक इंसानी शक्ल देने में सफल रही, पर निर्देशक खुद को पूरी तरह आदिवासी के ‘स्टीरियोटाइप’ से छुड़ा पाने में विफल रहा।
यह उलझन आदिवासी महिला ही नहीं, बाकी किरदार पर भी भारी था जैसे, चूंकि वकील फिल्म का नायक है तो उसे सुदर्शन होना ही है। पुलिस वाला विलेन है तो उसका चहेरा भी एक ‘विलेन’ जैसा ही होना चाहिए। फिल्म के अदालत का सीन हॉलीवुड की ‘बेन-हुर’ के भव्य रोमन महलों की याद दिलाता है।
जाने, क्यों निर्देशक के तथ्यों के प्रति इमानदारी यहाँ पर अचानक गायब हो जाती है। जॉली एलएलबी (पार्ट 1 ) का अदालत इस हिसाब से तथ्यों से बहुत ज्यादा करीब है। फिल्म में एक और नायक (वकील) के किरदार को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी गयी।
वकील के वामपंथी रुझान को दिखने के लिए दीवार पर मार्क्स का बेढब कट-आउट लगा दिखता है, वहीं दूसरी ओर पुलिसवालों के हमेशा नयी झक सफेद बनियान पहने दिखाया गया, मानो वह थाने में नहीं, बल्कि किसी त्यौहार पर गए हैं।
जेल में कैदियों की सुफेद हाफ पेंट, आधी बांह का कुर्ता और टोपी हमें फिल्मी कैदी के ‘स्टीरियोटाइप’ की याद दिलाता है। केवल यही नहीं, एक लम्बे समय जेल में रहने के बाद भी कैदियों की वर्दियां मैली नहीं होतीं।
क्या पता, जिस तरह गणतंत्र को इस देश में बचाने के लिए कभी-कभी तानाशाही की जरूरत पड़ती है शायद उसी तरह तथ्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए कभी कभार ‘स्टीरिओटाइप’ की जरूरत पड़ती है। परेशानी तब होती है, जब इस ‘स्टीरियोटाइप’ के चलते अनजाने ही सही तथ्यों के साथ एक बड़ी गलती हो जाती है।
‘जय भीम’ फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि ‘सत्य घटनाओं’ पर आधारित है. तथ्यों के अनुसार यह फिल्म सन 1993 में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में घटित एक घटना पर आधारित है जिसमें बीस मार्च 1993 के दिन जेवरात चुराने के आरोप में पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है जिसमें राजाकुन्नु भी एक था। पुलिस कस्टडी में राजाकुन्नु की मौत हो जाती है। केस की सुनवाई सन 1993 में शुरू होती है और तेरह वर्ष के लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार इसका फैसला आता है।
‘सत्य घटना’ पर आधारित इस फिल्म में राजाकुन्नु की बीवी सेन्जिनी को इस केस के शुरू होने के पहले से गर्भवती दिखाया जाता है। न केवल पूरे केस के चलने के दौरान बल्कि फैसले के वक्त भी सेन्जिनी गर्भवती है। दूसरे शब्दों में इस फिल्म के अनुसार सेन्जिनी तेरह साल गर्भधारण किये हुए रही।
शायद कुछ अतिरिक्त सहानुभूति पाने के इरादे से निर्देशक ने ऐसा किया। इसे निर्देशक का ‘ गणतांत्रिक अधिकार’ समझा जाय या उनके क्रिएटीविटी की तानाशाही?
रही बात सेन्जिनी की , तो चूंकि वह आदिवासी है तो इतना तो उसे करना ही होगा क्योंकि गलती तो उसकी भी है।
क्या है सेन्जिनी की गलती?
उसकी गलती यह है कि वह ( इस देश में) पैदा हुई....