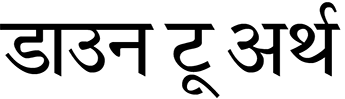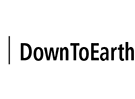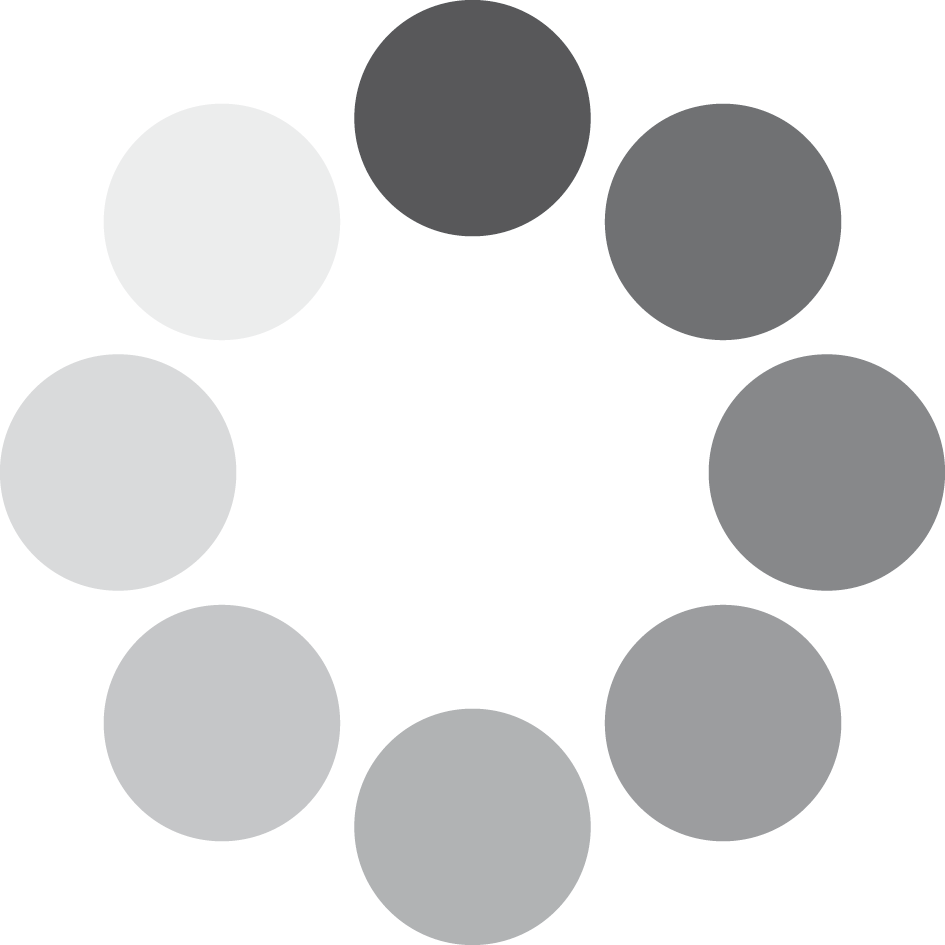कोस्टल रोड परियोजना से जूझता कोली समुदाय
पहले से ही अस्तित्व का संकट झेल रहा मुंबई का कोली समुदाय अब कोस्टल रोड परियोजना की वजह से खासा चिंतित है
On: Thursday 03 March 2022

 मुंबई के समुद्र किनारे रहने वाले कोली समुदाय के लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। फोटो: अलंकार
मुंबई के समुद्र किनारे रहने वाले कोली समुदाय के लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। फोटो: अलंकार
21वीं सदी के भारतीय महानगरों में मुंबई का कोली समुदाय विलक्षण है। इसकी जीवनशैली और जीवनयापन शहर में बसे हुए होकर भी पूर्णतः स्थानीय पारिस्थिकी और पर्यावरण पर आधारित है।
मुंबई के इतिहास-भूगोल-संस्कृति में कोली समुदाय का प्रभाव मजबूती से दर्ज है। मुंबई का तो नाम ही कोली समुदाय की प्रतिष्ठित देवी जिन्हें मुम्बा देवी कहा जाता है के नाम पर ही मुंबई पड़ा।
तट पर ही रचे-बसे हुए और समुद्री आखेट से पकड़ी मछिलयों पर आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े कोली समुदाय का मुंबई से इतना घनिष्ठ रिश्ता है कि उन्हें मुंबई महानगर का मूल निवासी समूह होने तक का औपचारिक दर्जा प्राप्त है।
बीते करीब पांच शताब्दियों में कोली समुदाय के लोगों ने मुंबई को सात अलग-अलग टापुओं को जोड़कर आधुनिक महानगर में बदलते देखा है। इन सातों टापुओं में कोली कई कोलिवाड़ों में रहते थे और इनमें से करीब 27 कोलीवाड़े अब भी जीवंतता के साथ मौज़ूद हैं।
इतने लम्बे समयकाल में वैसे तो कोलियों ने बहुत से उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन बीते दो-ढाई दशक कई मायनों में बहुत अलग साबित हुए हैं। बढ़ते शहरीकरण के दबाव तो बीसवीं सदी से जारी ही हैं, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन और बढ़ते जल-प्रदूषण ने भी कोली समुदाय के समुद्र से जाकर मछली पकड़ने के आधारभूत व्यवसाय को गहरे आघात पहुंचाए हैं।
कोली समुदाय का जीवनयापन सीधा-सीधा मछली एवं अन्य जल-मग्न प्रजातियों के पकड़ने एवं आगे उसके छोटे स्तर के विपणन और व्यापार पर आधारित है।
जिन रिहाइशी इलाकों को हम कोलीवाड़ा कहते हैं, दरअसल कोली स्वयं उन्हें 'गांवठन' ही बुलाते हैं। कोली गांवठन को अपनी संस्कृति और स्थायित्व की जमीन मानते हैं, लेकिन आधुनिक शहरी नियोजन की परिभषा में यह पूर्वाग्रह मज़बूत की है कि कोलीवाड़ा अस्थायी और शहर का अविकसित हिस्सा है और इसे झुग्गी-झोपडी जैसा समझकर भविष्य में रूपांतरित हो जाने वाला ही समझा जाता है।
कोली समुदाय मुंबई के समुद्री तट पर रहता-बसता ही नहीं, बल्कि तट से लगे अरब सागर से पूरी तरह गुथा हुआ है। इनका एक आवास अगर जमीन पर है तो दूसरा अपनी नाव में जिसपर रोज सवार होकर पुरुष दूर तक यात्रा करके मछलियां एवं अन्य प्रजातियां पकड़ कर लाते हैं और फिर महिलाएं इन्हें छांट कर बाजार में बेचती हैं।
मूलतः कोली परिवारों का इसी तरह जीवनयापन चलता है। जो कोली परिवार सीधा मछली पकड़ने-बेचने से संबद्ध नहीं भी हैं वह भी किसी न किसी रूप में इसी व्यवसाय से जुड़े हैं जैसे कि नावों की मरम्मत, जाल की सिलाई-बुनाई और या दुरुस्त करना, मछलियों को मुंबई के विभिन्न तटों पर नावों से उतारना, सुखाना या स्थानांतरित करना इत्यादि।
पूरा समुदाय ही समुद्र और तट के साथ जड़ित है। आधुनिकता की चकाचौंध वाले मुंबई में ज़्यादातर कोली अपनी देशज पहचान के साथ रहते ही दिखते हैं।
वेशभूषा, खान-पान, पर्व-त्यौहार इत्यादि अनेक बातों में कोली समुदाय आज के मुंबई में भी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ ही कायम है।
नई पुरानी पीढ़ी के अंतर हालांकि अब बढ़ने भी लगे हैं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा मछली पकड़ने का रोजगार अब अनेक संकटों में घिरकर लगातार कमजोर पड़ रहा है और इसीलिए नौजवान कोली अब अन्य कामों की ओर मुड़ते जा रहे हैं।
इसी कारण अब तो देश के अधिक वंचित लोग जो मुंबई पलायन करते ही रहे हैं, उनमें भी कई कोलियों के साथ मजदूर के रूप में जुड़ते जा रहे हैं और इन्हीं कोलीवाड़ों में जगह पा रहे हैं।
शताब्दियों से कोलीवाडे जीवंत हैं, क्योंकि समुद्र उनका पोषण कर रहा है। लेकिन आज कोलीवाड़े हों या कोली समुदाय या फिर समुद्र, तीनों ही तेजी से रूपांतरित हो रहे हैं।
छोटी-छोटी नावों से समुद्र में मछलियां पकड़ने जाने वाले कोलियों का सामना आज बहुत बड़े-बड़े आकार के राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मशीनीकृत व्यावसायिक ट्रॉलरों से हो रहा है जो न केवल अत्याधिक मछलियां पकड़कर पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि उनके अति-सूक्ष्म जालों की चपेट में अव्यस्क मछलियों और उनके अण्डों तक के आने से कुल मिलाकर मछलियों की संख्या पर बहुत अधिक दबाव बन चुका है।
इस बड़े पूंजीगत व्यावसायिक बदलाव का सीधा दुष्प्रभाव छोटे स्तर पर मछली पकडने वाले कोली मछुआरों पर आ गया है।
मुंबई के बढ़ते प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सीधा असर मुंबई तट के आसपास की समुद्री सेहत पर स्पष्ट दिखता है, जिसका गंभीर परिणाम सीधा कोली समुदाय पर आ चुका है।
वैश्विक तापमान वृद्धि एवं जल-प्रदूषण के कारण तट के पास मछलियों का मिलना लगातार न सिर्फ घटता जा रहा है अपितु मछलियों की विविधता भी बिल्कुल सीमित होकर रह गयी है।
बीसवीं सदी की तुलना में आज कोली मछलियां पकड़ने समुद्र में अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा दिनों तक के लिए जाते हैं ताकि बेहतर गुणवत्ता वाली खेप पकड़कर ला सकें और बेहतर आमदनी हो सके।
इस लम्बी और सुदूर यात्रा की लागत भी अत्यधिक बढ़ गयी है। चाहे श्रम के रूप में गिनी जाए या नाव में इस्तेमाल होने वाले डीजल ईंधन के रूप में। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्री तूफानों की तीव्रता एवं बारम्बारता बढ़ी है उसके खतरे तो खौफनाक रूप से बढ़ चुके ही हैं। ऐसी बहुआयामी कठिनाइयों के कारण सामुदायिक पेशा अत्यधिक अनिश्चित हो गया है।
पिछले दशक भर से तो मुंबई को नयी पहचान देने वाली दो बड़ी परियोजनाएं ही मुंबई की सबसे पुरानी पहचान वाले कोली समुदाय को पूरी तरह हाशिये पर धकेल दे रही हैं।
बांद्रा-वर्ली समुद्र-सेतु या उसका एक और विशाल स्वरुप जिसे कोस्टल रोड का नाम दिया गया है। ये दोनों ही परियोजनाएं तट के बिल्कुल नजदीक समुद्र तल से ऊंची उठी ऐसी लम्बी-लम्बी सड़कों का निर्माण है, जिनकी नींव समुद्र में रखी शिलाओं और स्तम्भों पर टिकी हुई हैं।
इनके निर्माण का मुख्य तर्क ये कहकर दिया गया है कि मुंबई में बढ़ते वाहनों की वजह से जो शहर की परिवहन व्यवस्था और सड़कों पर भीड़ का दबाव है उसे कम किया जा सकेगा।
कोली मछुआरों की इन परियोजनाओं से बहुत संजीदा शिकायतें हैं। फिलहाल तो इसके निर्माण के समय ही समुद्र में आने जाने से कोलियों को रोका जा रहा है, जिससे उनके रोजगार की बड़ी हानि हो रही है। परियोजना पूरी होने पर समुद्र तक जाने के वैसे ही अन्य रास्ते स्थायी तौर पर अवरुद्ध या दुर्गम होने वाले हैं जिनसे हमेशा ही कोली मछुआरे समुद्र में प्रवेश करते हैं।
और तो और समुद्र और जमीन के बीच वो हिस्से जिनमें कम गहरे पानी में बेहतरीन मछलियां और लॉबस्टर जैसे जीव भी कोली मछुआरों को आसानी से उपलब्ध होते रहे हैं वह अब कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत मिटटी-कंक्रीट आदि से पाटकर समुद्र से काट दिए जा रहे हैं।
पिछले कुछ वर्षों से और विशेष तौर पर कोरोना काल में कोली कोस्टल रोड परियोजना के साथ संघर्ष कर रहे हैं। कोलीवाड़ों में और शहर भर में लम्बे लम्बे सामुदायिक जत्थे आंदोलनरत होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अव्वल तो परियोजना ही रोकी जाए या फिर कोलियों की समस्याओं का निराकरण समय रहते पूरी परियोजना का हिस्सा बनाया जाए जिससे न सिर्फ रोजगार बचें, बल्कि पूरी कोली अस्मिता को अस्तित्व के संकट से बचाया जा सके।
भविष्य ही बताएगा कि मुंबई के मूल निवासियों के संघर्ष की क्या परिणति होगी। धीरे धीरे शहर के अन्य जागरूक नागरिकों का साथ भी कोली पा रहे हैं।
अकादमिक जगत भी कोलियों के साथ जुड़कर ऐसी अनेक समस्याओं से नए-नए ढंग से जूझने के प्रयासों को शोध स्तर पर समझने के प्रयास कर रहा है। यह लेख एक ऐसे ही एक प्रोजेक्ट (टैपेस्ट्री) TAPESTRY से उभरे बृहद शोध का हिस्सा है जो आईआईटी-मुंबई के साथ मिलकर किया जा रहा है।
लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज में राजनीति विज्ञान के शिक्षक है।