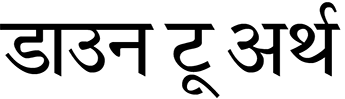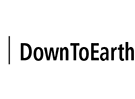किसके पास हैं आदिवासियों के इन सवालों के जवाब
पूरी दुनिया में आदिवासियों की कुल आबादी लगभग 48 करोड़ है, जिसका लगभग 22 फीसदी आदिवासी समाज भारत में रहता है
On: Wednesday 17 March 2021

 Photo: SIMON WILLIAMS
Photo: SIMON WILLIAMS भारत का इतिहास ऐसे अनेक संघर्षों और सत्याग्रहों से जाना जाता है, जिसने न केवल 'आदिवासियत' और ‘जल जंगल जमीन‘ के उनके अधिकारों को शब्द और अर्थ दिया, बल्कि भारत के निर्माण की ऐसी बुनियाद रख दी, जिसे आदिवासी समाज के स्वाभिमान, स्वायत्तता और संस्कृति से जुदा नहीं किया जा सकता।
आदिवासी समाज के अपने जल-जंगल-जमीन के स्वायत्तता के लिए सशस्त्र संघर्षों और अहिंसक सत्याग्रहों के संक्षिप्त इतिहास ने हमेशा से उन सवालों को समाज और सरकार के समक्ष खड़ा किया जिसका सपना और समाधान सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक स्वायत्तता थी और आज भी है।भारत की स्वाधीनता के लिए हुए आंदोलनों में इन ऐतिहासिक संघर्षों का अर्थ यह भी था/है कि एक स्वायत्त समाज के रूप में उन्हें स्वशासन और आत्मनिर्णय का संवैधानिक अधिकार मिले।
संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरी दुनिया में मूलवासियों/आदिवासियों की कुल जनसंख्या लगभग 48 करोड़ है, जिसका लगभग 22 फीसदी आदिवासी समाज भारत देश में रहता है। जनसंख्या और जंगल-जमीन पर स्वामित्व के दायरों के दृष्टिगत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारतीय गणराज्य की भूमिका निःसंदेह आदिवासी समाज के लिए और अधिक जवाबदेहपूर्ण होनी चाहिए।
भारत देश में आदिवासियों के अधिकारों और उन अधिकारों के मान्यताओं के सवाल, आदिवासी विद्रोहों के सफल इतिहास से समझा-जाना जा सकता है। गौरतलब है कि ब्रितानिया औपनिवेशिक व्यवस्था नें आदिवासियों के अधिकारों को मान्य करते हुए वर्ष 1874 में घोषित 'अनुसूचित जिला अधिनियम' के अंतर्गत इन क्षेत्रों में संवेदनशील प्रशासन के नये मानदंड बनाए, ताकि मूलनिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
बाद में भारत सरकार अधिनियम (1935) के अनुसार इन क्षेत्रों में संवेदनशील और जवाबदेह सरकारी शासन-प्रशासन के लिए राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। कालांतर में इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए गठित 'जनजातीय सलाहकार परिषद' को आदिवासी ग्रामसभाओं का प्रतिनिधि परिषद मानते हुए वैधानिक अधिकार भी दिए गए।
स्वाधीनता के पश्चात अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) के अधिकारों के सर्वोच्च वैधानिक संरक्षक के रूप में भारत के राष्ट्रपति ने दो आदेश जारी किए हैं - (1) अनुसूचित क्षेत्र (खंड-क, राज्य) आदेश 1950; तथा (2) अनुसूचित क्षेत्र (खंड-ख, राज्य) आदेश 1950 (संशोधित)। इस तरह अनुसूचित क्षेत्रों की प्रतिनिधि सभा के रूप में 'जनजातीय सलाहकार परिषद' का गठन और राज्यपाल को विशेष वैधानिक अधिकार सुनिश्चित कर दिए गए।
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार - देश में कुल भोगौलिक क्षेत्र का लगभग 11 प्रतिशत पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 का विशेष वैधानिक और सुरक्षात्मक महत्त्व है।
इसका अर्थ यह भी है कि भारत के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के अधिकार केवल इसलिए् महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि वे विशेषधिकार संपन्न पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बल्कि इसलिए विशेष हैं कि इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को ही भारत का प्रथम समाज माना गया है। भारत के संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य के लिए पांचवीं अनुसूची के इन ग्रामसभाओं के प्रस्ताव और अभिमत वास्तव में लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है।
आदिवासी बाहुल्य और वृहद् अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में राज्यपाल को जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श से अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं अनुसूचित क्षेत्रों में सुप्रशासन के लिए विनियम निर्माण की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन विगत सात दशकों के संक्षिप्त इतिहास में न तो देश के जनजातीय सलाहकार परिषदों से कोई अतिमहत्वपूर्ण सुझाव आए और ना ही राज्यपालों को सुप्रशासन के लिए विनियम निर्माण करना पड़ा।
इन्हीं दशकों के दौरान अधिकांश राज्यों ने अपने भूमि कानूनों में संशोधन कर आदिवासियों की भूमि हस्तांतरण/अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया, नए खदान और ख़निज विकास अधिनियम (2015) के माध्यम से आदिवासियों की अपनी जमीन में हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र में खदान खोल दिए गए, जन सुरक्षा अधिनियमों के अंतर्गत विकास का विरोध करने वाले सैकड़ों आदिवासियों को बंदी बना लिया गया और वनाधिकार कानून (2006) के सुरक्षात्मक प्रावधानों के बावज़ूद आदिवासियों के लाखों दावे निरस्त कर दिए गए।
मालूम नहीं कि सरकारों के इन क़दमों से 'सुप्रशासन' स्थापित हुआ अथवा नहीं किन्तु, इन कार्रवाइयों पर आदिवासी हितों के लिए नियुक्त और जवाबदेह महामहिम राज्यपालों द्वारा कभी कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए गए।
यथार्थ यह है कि पांचवी अनुसूची द्वारा राज्यपालों को प्रदत्त व्यापक शक्तियों को अनुच्छेद 163 के द्वारा सीमित कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल द्वारा 'सुप्रशासन' स्थापित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग, मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से करेंगे।
पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों में जनजातीय मंत्रणा परिषद के पदेन प्रमुख - राज्य के मुख्यमंत्री ही हैं और प्रशासनिक रूप से वे मंत्री परिषद के भी प्रमुख हैं। ऐसे में राज्य शासन और मंत्रणा परिषद के किसी भी निर्णय को 'सुशासन' और 'जनजातीय विकास' के विरुद्ध मानना अथवा साबित करना राज्यपाल के लिए लगभग असंभव है।
देश के निर्माताओं नें अनुसूचित जनजातियों के अनुत्तरित सवालों के राजनैतिक जवाब में उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए व्यापक संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किए। वास्तव में ये प्रावधान, आदिवासी समाज को स्वाधीनता के आंदोलन में शामिल होने और इसे जनांदोलन बनाने के लिए दिए गए लिखित-अलिखित आश्वासनों के परिणाम थे।
भारत की स्वाधीनता के सात दशकों के पश्चात विविध जनजातीय विकास योजनाओं के कागजी लक्ष्य और जमीनी उपलब्धियों के बीच बढ़ते फ़ासले के बीच खड़ा आदिवासी समाज भौंचक है और ठगे जाने के गहरे अहसास से भरा हुआ है।
दुर्भाग्य से आज भी जनजातीय क्षेत्रों में विकास का मूल्यांकन सामान्यतया आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के नाम पर पूंजी निवेश के आधार पर किया जाता है न कि 'विकास के अधिकारों' के लिए संविधान में दर्ज़ आदिवासियों के 'स्वायत्तता ' के राजनैतिक मूल्यों के अनुसार।
अपनी विख्यात पुस्तक 'आदि धरम' में अग्रणी आदिवासी नेता डॉ रामदयाल मुंडा मानते थे कि "आदिवासियों के लिए तथाकथित मुख्यधारा का आकर्षण वास्तव में भ्रांतिपूर्ण और विरोधाभासों से भरा है... आदिवासियों के लिए इस तथाकथित मुख्यधारा मे जाने का सुनिश्चित परिणाम होगा सदा-सर्वदा के लिए गुलामी स्वीकार करना। "
अफ़सोस है कि भारत में आदिवासी समाज के स्वायत्तता , आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक अस्मिता के सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। अनुसूचित क्षेत्र की संवैधानिक अवधारणा और उसके संवैधानिक कवच के ठीक विरुद्ध, आदिवासी समाज को विपन्न बना देने वाले क़ानूनों और नीतियों और व्यवस्थाओं के बनते-बिगड़ते अक्स में इसे देखा-समझा जा सकता है।
वास्तव में आदिवासी समाज के लिए स्वायत्तता, राज्य के मौजूदा व्यवस्थाओं को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने का कारगर माध्यम है और होगा। इसीलिए स्वायत्तता, आदिवासियों के सदियों से अनुत्तरित उनके अनेक सवालों का जवाब है जिसे स्थापित किए बिना कोई भी कल्याणकारी राज्य, लोकतांत्रिक होने का दावा कर ही नहीं सकता।
आज मौजूदा व्यवस्थाओं को औपनिवेशिक विधानों और प्रावधानों से परे रखकर ही हम भारत में आदिवासी समाज और आदिवासियत को उनका खोया हुआ स्थान और स्वाभिमान सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब सरकार और शेष समाज यह स्वीकार करे कि आदिवासी समाज के लिए ‘स्वायत्तता' प्रथम राजनैतिक अपरिहार्यता है।
विगत पूरी सदी से आदिवासी समाज को वंचित घोषित और साबित किए जाने के जो प्रयास हुए उसका संवैधानिक प्रायश्चित भी ‘स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के अधिकारों' से ही संभव था और है। किन्तु ऐसा नहीं हो पाने का अर्थ उस पूरे समाज को नैतिक-राजनैतिक रूप से हमेशा के लिए गवां देना ही साबित होगा, जिसके जिम्मेदार समाज और सरकार दोनों होंगे।
(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं)