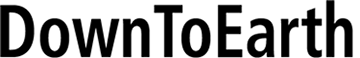
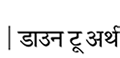
राजस्थान के रेतीले इलाके में देसी फल-सब्जियों का स्वाद टटोलती एक दिलचस्प यात्रा



वो जगह एकदम उजाड़ थी। हर तरफ रेतीली, पथरीली जमीन। जो सड़क हमें बीकानेर जिले के कोलायत ब्लॉक तक ले जा रही थी, उसके दोनों ओर कीकर और आक दिखाई पड़े थे। लेकिन हमारे लिए यह बहुत उत्साहजनक नजारा नहीं था। तीन दिन की यात्रा में हम राजस्थान के पारंपरिक या कहें देसी भोजन के बारे में जानने निकले थे। ऐसी चीजें जिन्हें यहां के लोग सदियों से उगा और खा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें बस कीकर और आक के पेड़ ही दिख रहे थे। कीकर को तो बकरियां भी नहीं खाती हैं और आक भोजन से ज्यादा औषधि के तौर पर जाना जाता है।
इसी उधेड़बुन के साथ हम बीकानेर से 90 किलोमीटर दूर कोलायत तहसील के भेलू गांव पहुंचे। यहां एक जगह है गोदारो की ढाणी। यह 30 बीघा बेतरतीब-सी जमीन चार भाईयों की हैं। हमारी मुलाकात उन्हीं में से एक भाई बाबूराम से हुई। बाबू राम अपनी कुर्सी पर बैठा एक छोटा, धारीदार फल छील रहा था। आसपास बिछी चारपाईयों पर यह कच्चा फल सूखने के लिए पड़ा था।
यह काचर नाम का फल था, जो खरबूजे से मिलता-जुलता फल है और स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है। इस इलाके में काचर का इस्तेमाल आमचूर की तरह होता है। बाबूराम इन फलों को सुखाकर व्यापारियों को बेचता है। ये व्यापारी इसका पाउडर, जिसे काचरी कहते हैं, बनाकर शहर के बाजारों में बेचते हैं। हमने बाबू राम से वह पौधा दिखाने के लिए कहा जिन पर काचर उगता है। बाबूराम और बच्चे, शैतान और मोती हमें खेत में लेकर गए। यह बेल खेत में अपने आप उग जाती है। इसमें सैकड़ों बीज होते हैं और एक भी फल खेत में रह जाए तो अगले साल खुद-ब-खुद उग जाती है।
घूमते-फिरते हमें एक बात और पता चली कि काचर यहां उगने वाला एकमात्र फल नहीं है। तपती दोपहर में हम जैसे ही खेत में पहुंचे, हमें रस भरी काकडिया भी मिले। इन्हें भी काचर की तरह सुखाकर रख लिया जाता है। शैतान और मोती हमारे लिए खेत से कुछ जंगली टिंडा (टिंडसी) भी ढूंढ़ लाए। इस फल को भी काटकर-सुखाकर रखा जाता है ताकि बाद में सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सके।
इसके बाद हम पास के खेत में गए, जहां हमें कुम्बट का पेड़ देखने को मिला। चूंकि, इसका मौसम गुजर चुका था, इसलिए इस पर फल ज्यादा तो नहीं थे पर कुछ शाखाओं से कुछ फलियां लटक रही थीं। इन फलियों के बीजों को कुमटिया कहते हैं। इनके साथ-साथ हमने खट्टे लाल बेर भी खाए। काफी घूमने-फिरने के बाद थक कर हम खेजरी के पेड़ के नीचे पानी पीने बैठ गए। पास में ही एक औरत ग्वार फली इकट्ठा कर रही थी। परिवार में सबसे बड़े भाई बुद्धाराम, जो हमारे लिए पानी लाए थे, उन्होंने बताया कि पहले जब इस इलाके में सूखा पड़ता था, तो खेजड़ी के पेड़ की छाल को पीसकर उसका इस्तेमाल आटे की जगह किया जाता है। सूखे की सबसे ज्यादा मार खाने-पीने की चीजों पर पड़ती थी और ऐसे में खेजड़ी की छाल जैसी चीजें खाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता था।
बहरहाल, तपती दोपहर में हम अपने मेजबानों के घर पहुंचे और उन्होंने हमें भोजन करने को कहा। जितनी देर में खाना आता, उस बीच हमें थोड़ी और काकडी और मतीरा खाने को मिला। ये देसी तरबूज दिल्ली के तरबूज जितना लाल व मीठा नहीं था और इसे सब्जी की तरह भी पकाया जा सकता है। इस बीच खेत से आई ताजी मूंगफली भी भुन चुकी थी। गुड़ वाली मीठी चाय के साथ हमने इनका स्वाद भी चखा। इसके बाद हमें बाजरे की बड़ी-बड़ी रोटियों के साथ ग्वार और काचर की मसालेदार सब्जी और दही परोसा गई। ऐसी ठेट दावत कहां मिलेगी!
भारी पड़ा फसलों का गणित
ये चीजें मानसून पर निर्भर इस इलाके की खेतीबाड़ी का अहम हिस्सा रही हैं। ज्वार, बाजरा और ग्वार यहां की प्रमुख फसल हैं। लेकिन यह परिवार सिंचाई के नए साधन अपना चुका है और अब अन्य फसलें भी उगा रहा है। इस बार इन लोगों ने व्यापार के लिहाज से मूंगफली की खेती की है। पिछली बार प्याज भी उगाई थी। वाणिज्यिक खेती में मुनाफा ज्यादा है इसलिए यह परिवार इसे तेजी से अपना रहा है। काचर और इसके बीजों से होने वाली करीब आठ हजार रुपये की कमाई के मुकाबले इस साल लगभग मूंगफली से उन्हें पांच लाख रुपए और ग्वार से 50 हजार रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है।
इस रेतीले, शुष्क इलाके में हमारे लिए बहुत कुछ नया था, जिसे देखने-समझने के लिए हम भेलू गांव से पूरब की ओर नोखड़ा गांव की तरफ बढ़े। यह क्षेत्र केर नामक फल के लिए जाना जाता है। यहां हमारी मुलाकात 50 वर्षीय नारायण सिंह से हुई जो पिछले तीस साल से केर के फलों का व्यापार कर रहे हैं। इस कंटीले पेड़ से फल इकट्ठे कर महिलाओं और बच्चों को रोजगार मिल जाता है। निजी और सामुदायिक दोनों तरह की भूमि से ये केर प्राप्त कर लेते हैं। नारायण सिंह गांव के उन चार लोगों में से हैं, जो 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इनसे केर खरीदते हैं। कड़वापन दूर करने के लिए इन फलों को कुछ दिनों नमक के पानी में रखा जाता है। बाद में ये फल 100 रुपए किलो तक बिकते हैं। इनके खरीदार आकार पर विशेष ध्यान देते हैं और सबसे छोटा फल सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि उनमें बीज नहीं होते ।
नोखड़ा गांव के लोगों ने हमें खाने-पीने की और भी कई पारंपरिक चीजों के बारे में बताया। ऐसा ही एक कंटीला बीज है भुरूट। अकाल के दिनों में इसे भी आटे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमें फोग के पेड़ के बारे में भी पता चला जो वहां तो नहीं दिखा, लेकिन हमें बताया गया कि जैसलमेर के रास्ते में इसके काफी सारे पेड़ मिल जाएंगे। गर्मियों में इसके फल और फूलों का इस्तेमाल रायता और कढ़ी बनाने में किया जाता है।
अगले दिन हम लोग जैसलमेर के लिए निकल गए। वहां हम शहर से कुछ पांच किलोमीटर दूर चुंडी नाम के गांव में पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात 75 बीघा जमीन के मालिक 25 साल के खेवड़ा से हुई। हालांकि, उसे फोग के पेड़ के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन उसने इलाके में उगने वाली खाने-पीने की कुछ जंगली चीजों के बारे में हमें बताया। उनकी रसोई में टुम्बा के दुर्लभ बीज भी थे। आमतौर पर टुम्बा का फल जानवरों को खिलाने के काम आता है। लेकिन उन्होंने इन बीजों को अच्छी तरह उबालकर इंसान के खाने लायक बना दिया था। खेवड़ा की पत्नी ने हमें बताया कि वे बाजरा के आटे में इन बीजों को मिलाकर रोटियां बनाते हैं, जो बहुत करारी और पौष्टिक होती है। परिवार के लोगों ने हमें संभाल के रखी खाने-पीने की ऐसी कम से कम 10 देसी चीजें दिखाईं। परिवार के लोगों के लिए ये चीजें बहुत खास हैं। यह बात हमें तभी समझ आ गई, जब नौ साल के महिपाल ने जल्दी से ये पैकेट वापस अंदर रख दिए क्योंकि छोटे बच्चे इन पर झपटने लगे थे।
खेवड़ा ने बहुत चाव से हमें पीलू के मीठे फल के बारे में बताया। इस इलाके में बारिश के बाद रेत के टीलों पर जंगली मशरूम भी उगते हैं। इन्हें भी सुखाकर पीस लेते हैं और आटे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, हमें उन मशरूमों का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि यहां बारिश कभी-कभार ही होती है पर रिसर्च बताती हैं कि बरसात के बाद यहां 48 किस्म के मशरूम उगते हैं।
हमने खेवड़ा से हमें उसके खेत पर ले जाकर खेजरी का पेड़ दिखाने को कहा। वह हमें एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठाकर हमें खेत तक ले गया, जो रेत भरकर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हालांकि, उसका खेत जमीन एक सूखा टुकड़ा मात्र था लेकिन वहां रेत के खनन से वह काफी पैसे कमा चुका था।
यद्यपि इस परिवार को खानपान से जुड़ी कई परंपरागत चीजों की जानकारी थी, लेकिन समय के साथ वे भी कई चीजें भूल चुके थे। परिवार में किसी को भी खीप के बारे में नहीं मालूम था। खीप की फली का इस्तेमाल सब्जी की तरह किया जाता था। लेकिन आज उन्हें सिर्फ यही मालूम है कि उस पेड़ की पतली डंडियों का इस्तेमाल झोपड़ी की छत बनाने या अंतिम संस्कार में किया जाता है।

पीछे छूटते पारंपरिक स्वाद
यहां से हम पत्थर तोड़ने का काम करने वाले मजदूरों के समुदाय से मिलने निकल गए। यहां हमें अहसास हुआ कि खेवड़ा उन गिने-चुने लोगों में है जो स्थानीय भोजन के बारे में कम से कम कुछ तो जानते हैं। करीब पांच किलोमीटर दूर बेलदारों की ढाणी में आमतौर पर लोग बाजार से लाई सब्जियां ही खाते हैं। भोरा राम नाम के एक नौजवान ने हमें बताया कि इन स्वादष्टि जंगली चीजों को खोजना बहुत मेहनत का काम है और इसमें समय भी बहुत लगता है। ज्यादातर लोग बाजार से सब्जियां खरीद लाते हैं, जबकि आसपास के इलाके में ये आसानी से मिल सकती हैं। लोग एक किलो मशरूम के लिए 200 रुपये खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन उसे इकट्ठा करना नहीं चाहते। फिर भी परंपरागत फल-सब्जियों से हमारा परिचय कराने वाले भगवान राम ने हमसे वादा किया कि अगली बार वे हमें कई अन्य दुर्लभ भोजन खिलाएगा। हालांकि, इस इलाके में केर नहीं मिलता लेकिन वे इस फल से लड्डू बनाने का तरीका बताते हैं। लेकिन उनकी बातों से ये साफ था की ऐसी परंपरागत चीजें आजकल लोगों की रसोई के बजाय उनकी स्मृतियों में अधिक पाई जाती हैं।
जोधपुर में स्कूल ऑफ डेजर्ट साइंस के निदेशक एसएम मोहनोत यह जानकार हैरान थे कि हमें आजकल भी लोगों के घरों में इतना पारंपरिक भोजन मिल गया। वह कहते हैं, “अब गांव के लोग अब परंपरागत भोजन पर निर्भर नहीं हैं। यह स्वादष्टि आहार तो बस अतीत की निशानी भर रह गया है।” इस तरह का खानपान बाजारों से दूर मुख्यत: ढाणियों तक ही सीमित है। राजस्थान के छोटे से छोटे गांव में भी अब बाजार की फल-सब्जियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्थानीय चीजें जैसे कुम्बट, केर और सांगरी तो आलू और प्याज से भी मंहगी हैं। कई चीजों के दाम तो सूखे मेवों के बराबर हैं। इन पुरानी चीजों का उत्पादन भी लगातार कम होता जा रहा है। क्योंकि एक ओर जहां खेती के लिए इस तरह के पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खेती व खनन की वजह से नए बीजों को जमने का मौका नहीं मिलता। आज से करीब 50 साल पहले जिस जमीन पर एक क्विंटल (100 किलो) पैदावार होती थी, उस जमीन पर अब मुश्किल से 10 किलो पारंपरिक चीजें उग पाती हैं। इस तरह की फल-सब्जियों को धोने, सुखाने और संभालकर रखने में भी बहुत समय और मेहनत लगती है। हालांकि, ऐसा नहीं है की सभी चीजे लुप्त हो रही है। उदाहरण के तौर पर, आज भी लोग सांगरी, केर और कुमटिया को बड़े जतन से जुटाते है और लंबे समय तक उपभोग के लिए संभालकर रखते हैं। लेकिन फोग, टिंडा, खीप जैसे चीजें तकरीबन गायब हो चुकी हैं। कुछ तो उग ही नहीं रही और कुछ को अब इकठ्ठा नहीं किया जा रहा है।
उम्मीद की किरण
बीकानेर में ‘उर्मुल’ ट्रस्ट के सचिव और मुख्य कार्यकारी अरविंद ओझा खाने-पीने की कई परंपरागत चीजों के भविष्य को लेकर फिर भी आशान्वित हैं। उनका मानना है कि राजस्थान में पर्यटन बढ़ने से इस तरह की चीजों की मांग बढ़ी है। यहां आने वाले मेहमान ट्रेडीशनल फूड का स्वाद चखना चाहते हैं। वह बताते हैं, “हम अपने स्वयं सहायता समूहों में पारंपरिक भोजन को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों सिखा रहे हैं कि ग्वार फलियों को सुखाकर रेगिस्तान की जायकेदार नमकीन के तौर पर कैसे बेचा जा सकता है। मेलों में इसे बेचा भी जाने लगा है। इन चीजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम सोलर ड्रायर्स लगाने की तैयारी कर रह हैं। इसके अलावा हम किसानों को लगातार इन पेड़-पौधों के बारे में बता रहे हैं, ताकि ये पेड़ पौधे आगे भी खेतों में बनी रह सकें। खेजरी का पेड़ साल भर में अंदाजन 10 हजार रुपए का फायदा देता है। भोजन के काम आने के अलावा इसकी छाया में फसलें अच्छी उगती हैं और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल पशुओं चारे के लिए भी किया जाता है।
परंपरागत स्वाद का हमारा तीन दिन का सफर जोधपुर के रेस्टोरेंट में जाकर खत्म हुआ, जहां आलू-पूड़ी और चाऊमीन जैसी प्रचलित चीजें परोसी जा रही हैं। यही चीजें तो हमें दिल्ली में मिलती हैं। शायद नोखड़ा गांव के बुजुर्ग खेराज राम ठीक ही कहते हैं कि दिल्ली फकीरों का शहर है। जंगल में उगने वाली देसी चीजें हम दिल्ली वालों की किस्मत में कहां! हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि राजस्थान के किसान अपने पारंपरिक खानपान को नहीं भूलेंगे। वैसे भी देश में ऐसी बहुत कम जगह हैं, जहां विविधता से भरपूर परंपरागत भोजन आज भी खानपान का हिस्सा है।
We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together.

Comments are moderated and will be published only after the site moderator’s approval. Please use a genuine email ID and provide your name. Selected comments may also be used in the ‘Letters’ section of the Down To Earth print edition.