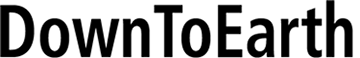
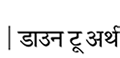
बैगा आदिवासियों के भोजन का अभिन्न अंग रहा सिकिया अनाज क्या अपनी पुरानी रंगत में लौट पाएगा?



बैगा जनजाति के लोग पारिस्थितिकविदों से कम नहीं होते। इस आदिवासी समुदाय के लोग अपने आसपास की सैकड़ों प्रजातियों को पहचानने एवं उनके इस्तेमाल के असंख्य तरीकों की जानकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित ढाबा गांव की ओर जाते हुए मेरा मुख्य उद्देश्य उनके पारंपरिक रूप से समृद्ध लेकिन सादे जीवन को करीब से जानना है। ढाबा डिंडौरी जिले के उन 52 गांवों में से है जहां की पहाड़ियों और जंगलों में बैगा जाति के लोग शताब्दियों से रहते आए हैं। ढाबा की ओर जाती हुई खड़ी ढलान पर चढ़ाई करने के क्रम में मेरी मुलाकात एक स्थानीय निवासी रंगूलाल से होती है। जैसे ही मैं सिकिया का नाम लेती हूं, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है।
सिकिया अनाज (वैज्ञानिक नाम डिजिटेरिया सैंगविनेलिस) बैगा जनजाति के लोग उगाते और चाव से खाते हैं। वह कहते हैं, “मुझे सिकिया खाए हुए एक अरसा बीत चुका है। अब यह मेरे गांव में नहीं पाया जाता।” यही नहीं, बाद में जब मैंने गांववालों से इस अनाज के बारे में पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि नई पीढ़ी के लोगों ने इसका स्वाद चखना तो दूर, इसके बारे में सुना भी नहीं था। और इसका मुख्य कारण है खेती की बदलती तस्वीर जिसने बैगा जनजाति को भी प्रभावित किया है।
यह आदिम आदिवासी जनजाति पारंपरिक रूप से “बेवाड़” (एक घुमंतू, काटो एवं जलाओ किस्म की खेती) किस्म की खेती करती आई है जिसमें लगातार तीन वर्षों तक फसलें उगाने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश की ही एक गैर लाभकारी संस्था निर्माण के सचिव नरेश बिस्वास का कहना है,“हालांकि वन विभाग के कर्मचारी एवं कृषि वैज्ञानिक इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते लेकिन बेवाड़ खेती जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करती है।” वह आगे बताते हैं कि बैगा अक्सर खेत को तैयार करने के लिए पहले “लैंटाना”(जिसे तानतानी के नाम से भी जानते हैं) की झाड़ियों को साफ करते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, वे बिना जुताई किए अनाजों की कई किस्मों को सीधा खेत में छिड़क देते हैं।
इस तरह से कभी-कभी तो एक खेत में अनाजों की 20 किस्में तक उग आती हैं। यह विविधता अब तक बैगाओं की पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करती आई है। हालांकि पड़ोस के गांव पौड़ी की जीराबाई बताती हैं कि अब सिकिया की खेती शायद ही कभी होती हो। वह कहती हैं, “फसल की कटाई के दौरान जो बीज जमीन पर गिर जाते हैं वे ही प्राकृतिक वृद्धि में मदद करते हैं।” शोधकर्ताओं से बातचीत से पता चलता है कि सिकिया एक बारहमासी जंगली घास की प्रजाति है जो अनुकूल मौसम होते ही मूल रूट स्टॉक से दोबारा उग आती है। हालांकि सिकिया का वृहद अध्ययन किया जाना अब भी बाकी है लेकिन बिस्वास का मानना है कि बेवाड़ खेती वाली जमीन में फसल विविधता का होना सिकिया के विकास के लिए जरूरी है। बैगाओं की थालियों से यह अनाज लगातार गायब होता जा रहा है। इसका कारण है बैगा परिवारों द्वारा बहु फसल (मल्टी क्रॉपिंग) को बंद करना। बौना गांव के सरपंच रामलाल रथूरिया कहते हैं “हम अब अरहर उगाते हैं क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं।”

बाकी जगहों पर खर-पतवार मानी जानेवाली सिकिया का इस्तेमाल बैगा सदियों से भोजन के रूप में करते आए हैं। सिकिया की खीर खासतौर पर प्रचलित है। इसके हल्के पीले दाने देखने में अन्य ज्वार के दानों से छोटे होते हैं। सिलपीड़ी गांव के हरिराम बताते हैं,“यह चावल से बेहतर तरीके से भूख मिटाता है। केवल 250 ग्राम सिकिया से मेरा दिनभर का काम चल सकता है।” इस गांव में अब भी बैगा जनजाति द्वारा सिकिया उगाई और इस्तेमाल में लाई जाती है। उसी गांव की एक दूसरी निवासी ग्वालिनबाई कहती हैं कि इसे पकाना भी आसान है। “स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए आपको बस दूध को उबालकर उसमें सिकिया की वांछित मात्रा डालनी होती है। यह हमारी रोग-प्रतिरोधी क्षमता को भी मजबूत रखता है।”
डूमर तोला गांव के साठ वर्षीय बुजुर्ग घुंथु कहते हैं,“मैंं रोज सुबह सिकिया खाता आया हूं। इसका स्वाद बाकी अनाजों से कहीं बेहतर है। हम अपने 2-3 हेक्टेयर के खेत में 300 किलो के आसपास सिकिया पैदा कर लेते हैं।”
“इस गौरवशाली अतीत के बावजूद बैगा समुदाय के बाहर लोग सिकिया के बारे में नहीं जानते। यही नहीं, सरकार द्वारा “न्यूट्री सिरियल” के रूप में बढ़ावा दिए जा रहे ज्वार अनाजों की फेहरिस्त में भी इसका नाम कहीं नहीं है। बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी संस्था से ताल्लुक रखने वाले कृष्ण प्रसाद ने इसी वर्ष भोपाल में आयोजित हुए “यूजिंग डाइवर्सिटी सीड फेस्टिवल” के दौरान बैगा समुदाय के लोगों से तब बात की थी जब वे इस दुर्लभ ज्वार के प्रदर्शन हेतु आए थे। उनका कहना है, “ सिकिया के जनसाधारण में प्रचलित न होने का एक कारण है इसके प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग का काफी मुश्किल होना। पारंपरिक रूप से बैगा महिलाएं इसका सख्त बाहरी छिलका निकालने के लिए एक लकड़ी की भारी छड़ी का इस्तेमाल करती आई हैं जिसे मूसर कहते हैं। इस अनाज के छोटे आकार की वजह से इसे कंकड़ों से अलग करना भी मुश्किल होता है।” वह आगे जोड़ते हैं कि सिकिया के प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त मशीनें बनाने की जरूरत है। इसे पोलिश ज्वार भी कहते हैं क्योंकि पोलैंड में किसान इस अनाज को उगाते एवं खाते तो हैं ही, इसका इस्तेमाल जानवरों के चारे के लिए भी होता है।
जर्मनी में भी सिकिया की खेती होती है। हमारी सरकार तो सिकिया को लेकर पूरी तरह से अंधेरे में है लेकिन बिस्वास एवं उनके ही जैसे कई अन्य लोग इस अनाज को लोकप्रिय बनाने में लगे हैं। बिस्वास ने इस अनाज के नमूने हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (आईआईएमआर) को भेजे हैं जहां इनकी पोषण क्षमता का विश्लेषण होना है। आईआईएमआर के निदेशक विलास तोनापी बताते हैं,“सिकिया एक क्रैबग्रास फिंगर मिलेट है। यह हमेशा से आदिवासी परंपरा का एक हिस्सा रहा है। हम इसके बारे में बस इतना जानते हैं कि इस अनाज में 12 प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन का होता है। विटामिन, कैल्सियम, आयरन एवं अमीनो अम्लों की जांच अभी जारी है।”
क्या सिकिया बैगाओं के इन गांवों के बाहर भी जिंदा रह सकती है? यह पता करने के लिए झारखंड के गोड्डा जिले के एक पैदाइशी बीज संरक्षक सौमिक बनर्जी एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवी, जबलपुर) के शोधकर्ता साथ मिलकर प्रयोगात्मक आधार पर इसकी खेती कर रहे हैं। जेएनकेवी के पादप विज्ञान विभाग के प्रमुख अजय सिंह गोंटिया बताते हैं, “पिछले वर्ष हमने सितंबर में सिकिया की बुआई की थी और फरवरी में फसल काटी।” उनका विभाग इस वर्ष भी सिकिया की खेती करेगा। लेकिन क्या ये कोशिशें यह सुनिश्चित कर पाएंगी कि बैगा लोगों की थालियों में एक बार फिर से सिकिया दिखे?

पिछले 60 वर्षों में, भारत की कृषि नीति ने चावल और गेहूं पर ध्यान केंद्रित किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से पॉलिश किए चावल और गेहूं की आपूर्ति ने भारतीयों की आहार संबंधी आदतें बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। डाउन टू अर्थ ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पाया कि गोंड आदिवासियों की चावल के प्रति रुचि बढ़ी है, चावल उन्हें बेहद पसंद है। (देखें: स्थानीय अनाज)। मंडला के डुंगारिया गांव के कांती पांड्रो को रोजाना चावल खाने की आदत पड़ गई है। इस तरह, मोटा अनाज जैसे बाजरा, जौ इत्यादि हमारी प्लेटों के साथ-साथ खेतों से गायब हो गए हैं। हालांकि,आज मोटे अनाज अपने उच्च पौष्टिक मूल्य के कारण बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अत्यधिक गर्मी और सूखे का सामना करने की इनकी क्षमता के कारण इन्हें पोषक अनाज कहा जाता है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में इन पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मोटा अनाज वापस लाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार केंद्र की पोषक अनाज योजना के तहत कोदो और कुट्टी को बढ़ावा दे रही है। मंडला में, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए) ने उपयुक्त प्रसंस्करण इकाइयां उपलब्ध कर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगभग 30-40 गांवों की पहचान की है। चेन्नई स्थित गैर-लाभकारी संगठन एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से मोटे अनाज आधारित व्यंजनों पर भी तकनीकी मार्गदर्शन ले रहा है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कई शहरी लोग अब पारंपरिक धान और गेहूं पर मोटे अनाज का समर्थन कर रहे हैं लेकिन फिर भी कम उत्पादन, कमजोर बाजार, कठिन प्रसंस्करण विधियों और उपभोक्ताओं की कम रुचि के चलते मोटे अनाज को प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है।
मंडला जिले के टिक्राबेरपानी गांव की एक किसान बुधिया बाई कहती हैं कि मोटे अनाज की प्रक्रिया मुश्किल है। बाई जैसी महिलाएं दम लगाकर एक पारंपरिक लकड़ी के औजार यानी मूसर से धान से भूसी निकालने में घंटों बिताती हैं। और फिर भी, बाई और पांड्रो जैसी महिलाओं ने मोटे अनाज को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है क्योंकि वे इसकी पानी संबंधी खपत को अच्छे से जानती हैं।
एएसए के कृषि कार्यक्रम प्रबंधक सुनील जैन के अनुसार, “लगभग 40 गांवों में करीब 1,250 किसान ऐसे सीमांत क्षेत्रों में मोटे अनाज की खेती में लगे हुए हैं, जहां और कुछ नहीं उगता है।” एएसए मोटे अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।
अनाज के पुनरुद्धार की कहानियां
मोटा अनाज जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर अत्यधिक लचीला है। रागी, बाजरा और अन्य मोटे अनाज सिंचाई के पानी की मांग को 33 फीसदी कम कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावी जिले में रागी की खेती किसानों के लिए दोहरा लाभ सुनिश्चित करती है
मकरा अनाज या पैनिकम रामोसम
आज से 30 साल पहले तुमकूर (कर्नाटक) के गांवों में मूंगफली का उत्पादन शुरू होते ही इस अनाज की पैदावार में कमी आई। एक तो मूंगफली के प्रसंस्करण की प्रक्रिया आसान थी, दूसरे उनमें अनाज के मुकाबले मुनाफा भी ज्यादा था। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण किसान फिर से मकरा अनाज की खेती करने लगे हैं। यह फसल सूखा एवं बाढ़ का मुकाबला कर लेती है।
काकुम अनाज या सेटेरिया इटैलिका
आंध्र प्रदेश के कुरनूल, कडपा और अनंतपुर जिलों में पुनर्जीवित किया गया है। कृषि विभाग ने 2016 में किसानों को फॉक्सटेल बाजरे के बीज की आपूर्ति एक आकस्मिक उपाय के रूप में तब की थी जब उनकी मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई थी। धीरे-धीरे, किसानों ने इसे अपनाया और अपने बीजों को भंडारित करना शुरू कर दिया। अब उनके लिए आय का एक अच्छा स्रोत बन चुका है।
चेना अनाज या पैनिकम मायलेसियम
इसे हिंदी में चेना कहते हैं। बीटी कपास जैसी वाणिज्यिक फसलों के आने से पहले उत्तरी कर्नाटक के सूखे इलाके में यह एक आम फसल थी। समय के साथ यह खेतों से गायब होती गई। कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले के कुंडगोल ताल्लुका के माटीघाटा गांव से सुनील नामक एक किसान ने वर्ष 2014 में पहली बार इस ज्वार की खेती की। इसमें मैसूर की एक संस्था सहज समृद्धि ने मदद की। आज कर्नाटक में डेढ़ हजार से अधिक किसान ज्वार की यह किस्म उगा रहे हैं।
रागी अनाज या इल्यूसाइन कोराकान
किसी समय भारत के कुल रागी उत्पादन का 64 प्रतिशत हिस्सा कर्नाटक से आता था। हालांकि वाणिज्यिक फसलों के आने की वजह से रागी की खेती में कमी तो आई ही, लोगों ने भी गेहूं एवं पॉलिश वाले चावल जैसे अन्य अनाजों की ओर रुख करना शुरू किया। मैसूर स्थित संस्था सहज समृद्धि ने छोटे किसानों के खेतों में फिरसे ज्वार आधारित बहु-फसल प्रणाली की तर्ज पर खेती शुरू की। इसके अंतर्गत रागी की कई “लैंडरेसेज” का वितरण भी किया गया। (मैसूर की संस्था “सहज समृद्ध” व हैदराबाद की संस्था “वसन” के सौजन्य से)
कंगनी या फॉक्सटेल मिलट
नगालैंड के फेक जिले के चिजामी गांव में चावल के साथ-साथ मोटा अनाज भी पारंपरिक नगा आहार का हिस्सा था। ये दोनों अनाज हाथ से कूटे जाते थे। हालांकि, चावल मिलों के आगमन के साथ चावल प्रसंस्करण का काम तो आसान हो गया, लेकिन बाजरा जैसे मोटे अनाज को संसाधित करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रही। इसके चलते चावल की खपत ज्यादा होती चली गई जबकि मोटे अनाज की खपत बहुत ही कम रह गई। (स्रोत : उत्तर पूर्व नेटवर्क-नगालैंड)
We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together.

Comments are moderated and will be published only after the site moderator’s approval. Please use a genuine email ID and provide your name. Selected comments may also be used in the ‘Letters’ section of the Down To Earth print edition.