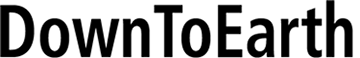
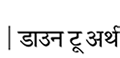
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर डाउन टू अर्थ द्वारा श्रृखंला प्रकाशित की जा रही है। इस कड़ी में प्रस्तुत है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर गांधी का दृष्टिकोण



दुनिया भर में पर्यावरणीय आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन बड़े पैमाने पर औद्योगिक उद्यमों और पूंजीवादी समाज के मूल्यों की आलोचना करने में लगे हुए हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में जागरुकता भी बढ़ रही है। लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन का ज्यादातर दुष्प्रभाव ग्लोबल साउथ (एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई, आदि देशों के निम्न-मध्य आय वर्ग वाले लोग) में रहने वाले गरीबों पर पड़ेगा। पर्यावरणीय आंदोलनों का सीधा संबंध गांधी या गांधीवाद से नहीं है। हालांकि, इस आंदोलन में जिन तरीकों को अपनाया जाता है और जो बहस होती है, उसमें अक्सर गांधीवादी तत्व शामिल होते हैं। एक उदाहरण मैक्सिको का जापातिस्ता विद्रोह है। ये विद्रोह सरकारी बलों के साथ हुए हिंसक टकराव के बाद, नागरिक प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। समाज को संगठित करने का इसका वैकल्पिक मॉडल स्वायत्तता, भागीदारी और सरकारी कार्यालय को सत्ता स्रोत के मुकाबले सेवा प्रदाता के रूप में देखने के सिद्धांतों पर आधारित है। जाहिर है, ये सिद्धांत गांधीवादी विचार से प्रेरित हैं।
भारत में अधिकांश पर्यावरणीय आंदोलन विकास के उन प्रतिमानों के जवाब में उभरकर सामने आए, जिसे देश ने आजादी के बाद अपनाया था। ये सभी आंदोलन आजीविका, भूमि, जल और पारिस्थितिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित हैं। इन आंदोलनों को लेकर उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से कई ने गांधीवादी तरीके अपनाए हैं। जैसे, सविनय अवज्ञा, तटीय रेत में खुद को दफना लेना, जल सत्याग्रह, लंबी पैदल यात्रा, भूख हड़ताल, राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं की भागीदारी, अधिकारियों के पास आवेदन भेजना, वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत और सर्वसम्मति बनाने के लिए ऑल पार्टी बैठकों का आयोजन। इस तरह के आंदोलनों के कई नेता सामाजिक परिवर्तन पर गांधी और उनके दृष्टिकोण से प्रेरित थे। पर्यावरणीय आंदोलन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर सामने आए। लोग मिट्टी, पानी और वन जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आगे आए। आर्थिक वैश्वीकरण के बाद, जिसमें कॉरपोरेट्स द्वारा अत्यधिक खनन कार्य किया जा रहा है, ऐसे आंदोलनों की तीव्रता बढ़ी। पश्चिम में शहरी मध्य वर्ग पर्यावरण आंदोलनों का नेतृत्व करता है। लेकिन भारत में ऐसे आंदोलन में शामिल लोग गरीब होते हैं और उनकी लड़ाई अस्तित्व और आजीविका के मुद्दों पर केंद्रित होती है। हालांकि, इस तरह के आंदोलनों के समर्थन में प्राय: समाज के सभी वर्ग के लोग भी आगे आते हैं।
गांधी को अक्सर एक पर्यावरणविद माना जाता रहा है, हालांकि उन्होंने कभी भी पारिस्थितिकी और पर्यावरण जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। ब्रिटिश काल में भी जंगल सत्याग्रह आम थे। हालांकि, हमारे पास ऐसे सबूत नहीं हैं, जिससे यह बताया जा सके कि क्या गांधी वाकई ऐसे आंदोलनों को लेकर चिंतित थे? पारिस्थितिकी विज्ञानी अर्ने नेस ने अपने पारिस्थितिकी सिद्धांतों को विकसित करने से पहले गांधी का अध्ययन किया था। गांधी ने कभी भी विकास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और उनके जीवन दृष्टिकोण में कार्बन पदचिह्न का स्थान बहुत ही कम था। उपभोक्तावाद के बजाय बुनियादी जरूरतों को सर्वोच्चता मिली, जो कइयों की नजर में प्रगति का प्रतीक है। यह एक गैर-भौतिकवादी और गैर-शोषक विश्वदृष्टि पर आधारित है, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच परस्पर आश्रित संबंध को दर्शाती है। गांधी का स्वदेशी विचार भी प्रकृति के खिलाफ आक्रामक हुए बिना, स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का सुझाव देता है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की निंदा की। गांधी ने कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित एक ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का आह्वान किया। भारत के लिए गांधी की दृष्टि प्राकृतिक संसाधनों के समझदारी भरे उपयोग पर आधारित है, न कि प्रकृति, जंगलों, नदियों की सुंदरता के विनाश पर। उनका प्रसिद्ध कथन “पृथ्वी के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं” दुनिया भर के पर्यावरणीय आंदोलनों के लिए एक उपयोगी नारा है। पर्यावरण से संबंधित गांधीवादी विचारों को उनके शिष्य जेसी कुमारप्पा के काम में और अधिक गहराई से देखा जा सकता है।
पर्यावरणीय आंदोलनों के रूप में हमने चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन देखा है। चिपको आंदोलन को विशेष रूप से अपने गांधीवादी जुड़ाव के लिए जाना जाता है। गांधी से अधिक, गांधी की शिष्या मीरा बहन और सरला बहन ने चिपको आंदोलन के नेताओं को प्रभावित किया था। इसी तरह, गांधीवादी विचार, उपयुक्त तकनीक और राजनीतिक-आर्थिक शक्ति का समान इस्तेमाल नर्मदा अभियान में देखा गया। जहां चिपको आंदोलन में स्थानीय समुदाय, महिलाएं और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल थे, वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की मदद से आदिवासी लोग कर रहे थे। बाबा आमटे और मेधा पाटकर जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेताओं ने साफ कहा है कि उन्हें मुख्य रूप से गांधी से प्रेरणा मिली है।
साइलेंट वैली बांध का विरोध उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और विनाशकारी विकास के विरोध जैसे विषयों पर आधारित था। इस आंदोलन का अहिंसक चरित्र भी उल्लेखनीय था। वंदना शिवा गांधीवादी पर्यावरणवाद के सबसे प्रमुख पैरोकारों में से एक हैं। उन्होंने एक भौतिक विज्ञानी और एक पर्यावरणविद (ईको-फेमिनिस्ट) के रूप में स्थिरता, आत्मनिर्णय, महिलाओं के अधिकारों और पर्यावरण न्याय के लिए काम किया है। उन्होंने जैव विविधता और बीज संप्रभुता की रक्षा के लिए नवधान्या नाम से एक नव-गांधीवादी पर्यावरण आंदोलन शुरू किया है। उन्होंने बीज सत्याग्रह की अवधारणा को गांधीवादी सत्याग्रह के नए रूप में लोकप्रिय बनाया है।
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ हुए आंदोलन ने भी अहिंसक दृष्टिकोण को अपनाया। एसपी उदयकुमार इस आंदोलन के नेता थे। वह मशहूर परमाणु-विरोधी कार्यकर्ता और शांति शोधकर्ता हैं। चिल्का में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी झील के स्वामित्व, आजीविका के खात्मे, कॉर्पोरेट द्वारा संसाधनों के व्यावसयिक उपयोग को लेकर सवाल उठा रहे थे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मछुआरों की भी भागीदारी देखी गई थी। राष्ट्रीय मिसाइल परीक्षण रेंज (नेशनल मिसाइल टेस्टिंग रेंज) के खिलाफ बालीपाल आंदोलन में भी प्रतिरोध के लिए अहिंसक रास्ता अपनाया गया था। लोगों ने सरकार के साथ असहयोग करने का फैसला किया। ग्रामीणों ने सरकार को कर और ऋण देने से इनकार कर दिया और कला को विरोध की अभिव्यक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उस निर्णय प्रक्रिया को चुनौती दी, जो स्थानीय विनाश की कीमत पर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को प्राथमिकता देती है। प्लाचीमाडा आंदोलन में भी गांधीवादियों ने अन्य वैचारिक धाराओं के लोगों के साथ काम किया। सभी जगह एक बात आम थी और वो यह कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग को लेकर जनता के पास आत्मनिर्णय का अधिकार हो और इस मामले में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण व सर्वोपरि हो।
अंत में कहा जा सकता है कि देश के पर्यावरणीय आंदोलनों में एक गांधीवादी विचार समाहित है। जैसे-जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, ये विचार उसमें समाहित होता चला गया। हालांकि, इस तरह के आंदोलनों को मूलत: जनसंघर्ष से ही प्रेरणा मिलती रही है। अस्तित्व और आजीविका की रक्षा के लिए होने वाले जनसंघर्ष ने ही आंदोलनों को बनाया, बढ़ाया है। दूसरा, कई आंदोलनों के नेताओं ने गांधी और उनके तरीकों को अपनाने की बात स्वीकारी है। तीसरी बात, आंदोलनों के लिए विदेशी फंडिंग की बजाय खुद के संसाधनों पर उनकी निर्भरता भी गांधीवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। चौथा, आंदोलन के दौरान होने वाली अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित बहस का चरित्र भी गांधीवादी था।
हम कह सकते हैं कि स्थानीय संप्रभुता और आजीविका संरक्षण, वैकल्पिक विकास, स्वदेशी ज्ञान को मान्यता, पंचायती राज संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के साथ विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता जैसी अवधारणाओं के निर्माण के लिए अक्सर पर्यावरणीय आंदोलनों में वामपंथ और गांधीवादी विचारों का मिश्रण समाहित होता है। पर्यावरण संकट की भयावहता को देखते हुए, भारत और दुनिया भर में यह स्वीकार किया जाने लगा है कि केवल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन से ही हम इस मुद्दे का हल निकाल सकेंगे। ये मूल्यों में बदलाव को न्यायसंगत बनाता है। आज अत्यधिक उपभोग के बजाय, गुणवत्तापूर्ण जीवन पर केंद्रित एक उत्तर-भौतिकवादी समाज की तलाश है, जो गांधीवादी विचार से प्रेरित है। कुछ हद तक यह हिंदू पारिस्थितिक दृष्टि भी दर्शाता है। इन सभी आंदोलनों में प्रभावित गरीबों की स्वयं संगठित होने की क्षमता पर भी जोर दिया गया था।
(लेखक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में प्रोफेसर हैं। वह गांधी शांति प्रतिष्ठान से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका “गांधी मार्ग” के संपादक भी हैं)
We are a voice to you; you have been a support to us. Together we build journalism that is independent, credible and fearless. You can further help us by making a donation. This will mean a lot for our ability to bring you news, perspectives and analysis from the ground so that we can make change together.
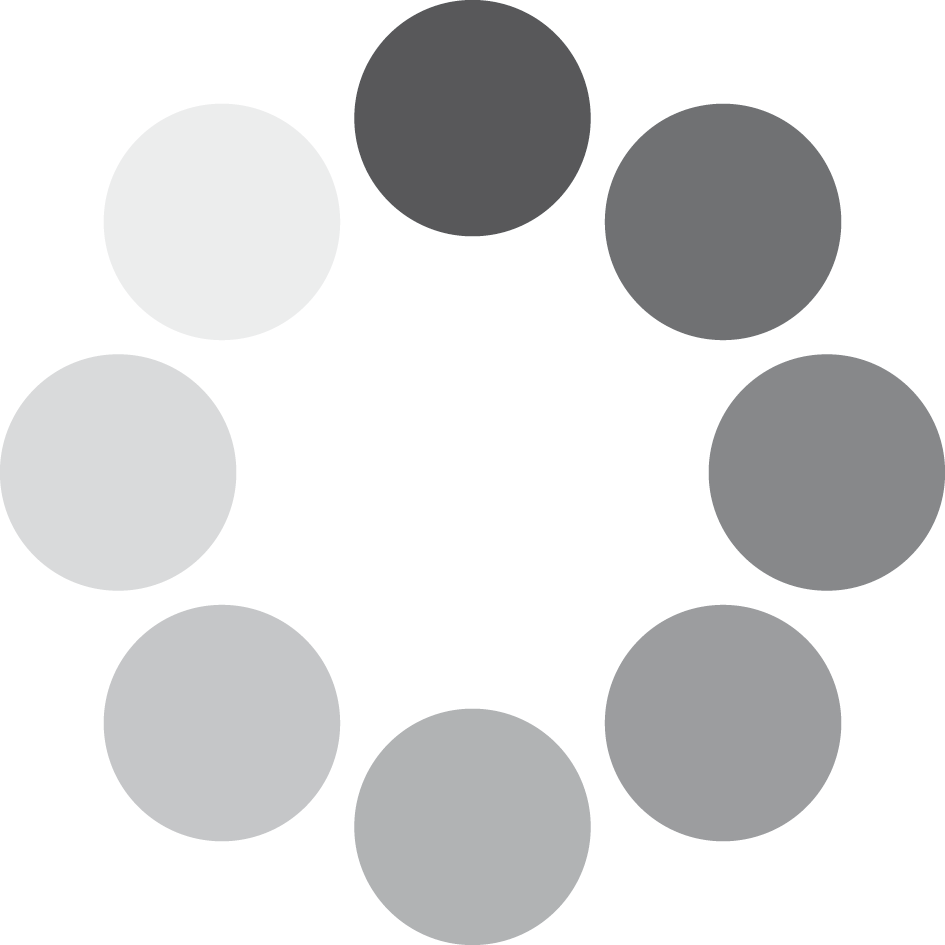
Comments are moderated and will be published only after the site moderator’s approval. Please use a genuine email ID and provide your name. Selected comments may also be used in the ‘Letters’ section of the Down To Earth print edition.