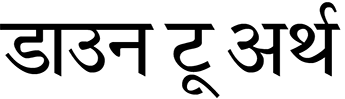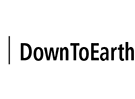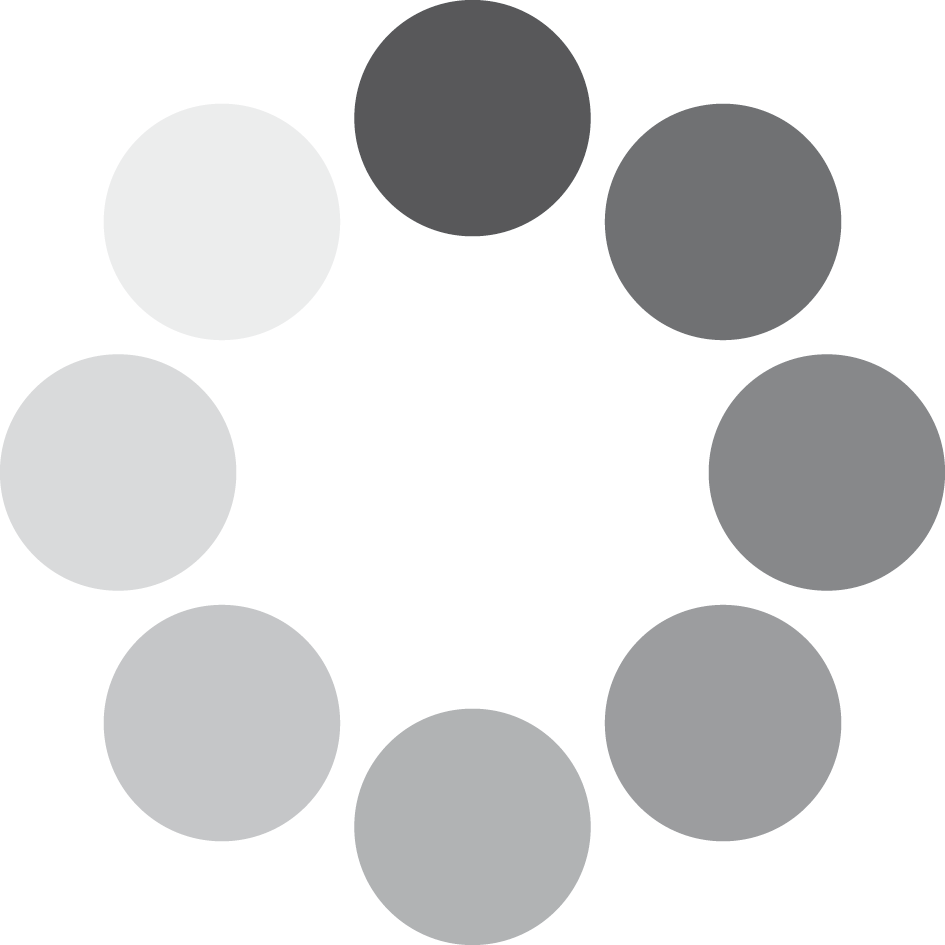जरूरत से तीन गुना ज्यादा है देश में अनाज का उत्पादन
डाउन टू अर्थ ने कृषि व कृषि शिक्षा की दशा पर देशव्यापी पड़ताल की। प्रस्तुत है, इस सीरीज की दूसरी कड़ी में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कार्यकारी निदेशक जीवी रामानजनेयुलू का लेख-
On: Tuesday 13 August 2019

 फोटो जीवी रामेजेनेयुलू के फेसबुक से लिया गया है।
फोटो जीवी रामेजेनेयुलू के फेसबुक से लिया गया है। भारत की कृषि यहां की ऋतु, वातावरण और किसानों की आय स्थिति पर आधारित है। अभी जो भी तकनीकी भारत में किसानों के सहयोग के लिए आ रही है उसमें इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता है। विदेशों में बड़ी जोत वाले खेतों पर काम करने के लिए काफी भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यहां मेहनत ज्यादा है और छोटे किसान भारी मशीनों या तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विदेशों में कई जगह जहां की मिट्टी अलग है, वहां पर दिन काफी लंबे होते हैं और मशीनों का काफी देर तक काम करना होता है।ऐसे में छोटे किसान इस मशीन का बोझ नहीं उठा सकते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 80 फीसदी लघु और सीमांत किसानों की प्रति महीने आय महज 5,000 रुपये है।
देश के 54 फीसदी लोग प्रत्यक्ष और देश का हर नागरिक अप्रत्यक्ष तरीके से कृषि पर ही निर्भर है। तमाम उद्योग-धंधे भी कृषि पर ही आधारित हैं। ऐसे में यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। कृषि का महत्व कम नहीं हुआ है, उसका महत्व बना हुआ है। यह जरूर है कि कृषि में निवेश बहुत कम हो गया है, जिसके कारण कृषि संकटग्रस्त है। यदि पीछे की तरफ देखिए तो 1980 में जहां बजट में कृषि पर 20 फीसदी खर्च का प्रावधान था वह अब घटकर महज 3 फीसदी रह गया है। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इसी से चल रही है। लेकिन सबसे दुखद पहलू है कि किसानों को ध्यान में रखकर शोध और तकनीकी तैयार नहीं की जा रही।
मेरा मानना है कि इस वक्त आईसीएआर और देश के अन्य शोध संस्थान अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। 1960-70 के दशक में आईसीएआर का बड़ा योगदान था। लेकिन तब समस्या और थी, अब परिस्थितयां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब कृषि को आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी बनाने की चुनौती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 80 फीसदी लघु और सीमांत किसानों की प्रति महीने आय महज 5,000 रुपए है। वे महंगी और बड़ी तकनीकी का बोझ नहीं उठा सकते।
यदि कृषि में निजी निवेश को देखा जाए तो पहले किसानों के जरिए हो रहे निवेश पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूरे देश में 14.8 करोड़ हेक्टेयर जमीन मौजूद है वहीं, किसान प्रति एकड़ सालाना 40 हजार रुपए खर्च कर रहा है। यह भी निजी निवेश है। इसका आकलन हमने कभी नहीं किया है। किसान यह निवेश अपने जोखिम पर कर रहा है। इसके निवेश को सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है। शोध, तकनीकी, क्रेडिट, संरचना, परिवहन, वर्षा जल संचयन जैसी श्रेणियों में सरकार को निवेश करना चाहिए। यह बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया में खेती सिर्फ सरकारी निवेश पर ही टिकी हुई है।
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी कमोडिटी जरूरी कमोडिटी है और इनकी कीमत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। ऐसे में इनकी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भी सरकारी प्रयास होने चाहिए। यह भी ध्यान देने लायक है कि देश के महज पांच राज्यों से ही सर्वाधिक सरकारी अनाज की खरीदारी होती है। इसलिए खाद्य और उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी का आधार भी बदले जाने की जरूरत है। जिसके खेत की मिट्टी का उपजाऊपन जितना ज्यादा हो, उसे ही सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो राज्य जितना ज्यादा उर्वरक इस्तेमाल कर रहा है, वहीं सबसे ज्यादा अनाज की खरीदारी होती है। देश के अनाज की आधी सरकारी खरीदारी सिर्फ पंजाब और हरियाणा से होती है। इसके अलावा शेष आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से। ऐसे में 80 हजार करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी और करीब 3 हजार करोड़ रुपए उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ इन्हीं राज्यों को दी जा रही है।
पहली कड़ी में आपने पढ़ा- ऐसे तो न खेती बचेगी और न ही तालीम
एक और चुनौती हमारे बीच आ खड़ी हुई है कि नई पीढ़ी खेती के करीब तभी जाना चाहती है जब उसे आर्थिक फायदा हो। यह आज की सबसे बड़ी मुसीबत है। इसके अलावा एक सामाजिक समस्या यह है कि खेत के मालिक और अनाज पैदा करने वाले किसान के बीच रिश्ता खराब हो रहा है। क्योंकि सिर्फ खेत के मालिकों को ही सारी सुविधाओं की बात हो रही है जबकि योजनाओं के असल फायदे जमीन पर खेती करने वालों के खाते में जाना चाहिए। यह बिल्कुल अनुचित है। मिसाल के तौर पर खेती-किसानी की मुश्किल को कम करने के लिए ही सरकार 75 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की बात कर रही है। यह पैसे किसके खाते में जाएंगे? यह खेत मजदूर और वास्तविक खेती करने वालों के खाते में नहीं जाएंगे। यह पैसे जमीन मालिकों के खाते में जाएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो खेती छोड़कर दिल्ली या लंदन में रहते हैं, जबकि उनके खेतों पर किसानी कोई और कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि जमीन मालिक और खेतिहर किसान के बीच एक कानूनी करार हो। इससे यह भी पता चलेगा कि असल में खेती कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग सिर्फ जमीन मालिक हैं।
दूसरी बड़ी समस्या पानी के लिए लड़ाई है। इसलिए अभी वर्षा जल संचयन के प्रयासों को न सिर्फ तेज करना होगा बल्कि जमीन पर इन कामों के उतारना होगा। खराब होती मिट्टी और पानी की कमी को देखते हुए हमें जैविक खेती की तरह शिफ्ट होना चाहिए। साथ ही साथ देश के शोध संस्थानों का सारा प्रयास इसी तरफ होना चाहिए। यदि देखा जाए तो इस वक्त देश का उत्पादन 29 करोड़ टन है। यदि देश की कुल आबादी तीन वक्त खाना खाए तो भी 9 करोड़ टन अनाज की ही जरूरत होगी। हम अपनी जरूरत से तीन गुना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। आमदनी न होने और गरीबी के कारण लोग यह अनाज नहीं खरीद सकते। इसीलिए सरकार को इन्हें सस्ता अनाज मुहैया कराना पड़ता है। सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हुनरमंद बनाने और उन तक तकनीक पहुंचाने पर काम होना चाहिए। आज खाने की थाली में देखिए तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है। जरूरत है कि अब हम पोषण के बारे में सोचे। मिट्टी-पानी को ध्यान में रखकर दूसरी चीजें भी उगाएं।
(जीवी रामानजनेयुलू सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के कार्यकारी निदेशक हैं। लेख विवेक मिश्रा से बातचीत पर आधारित)