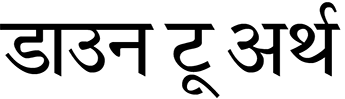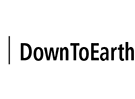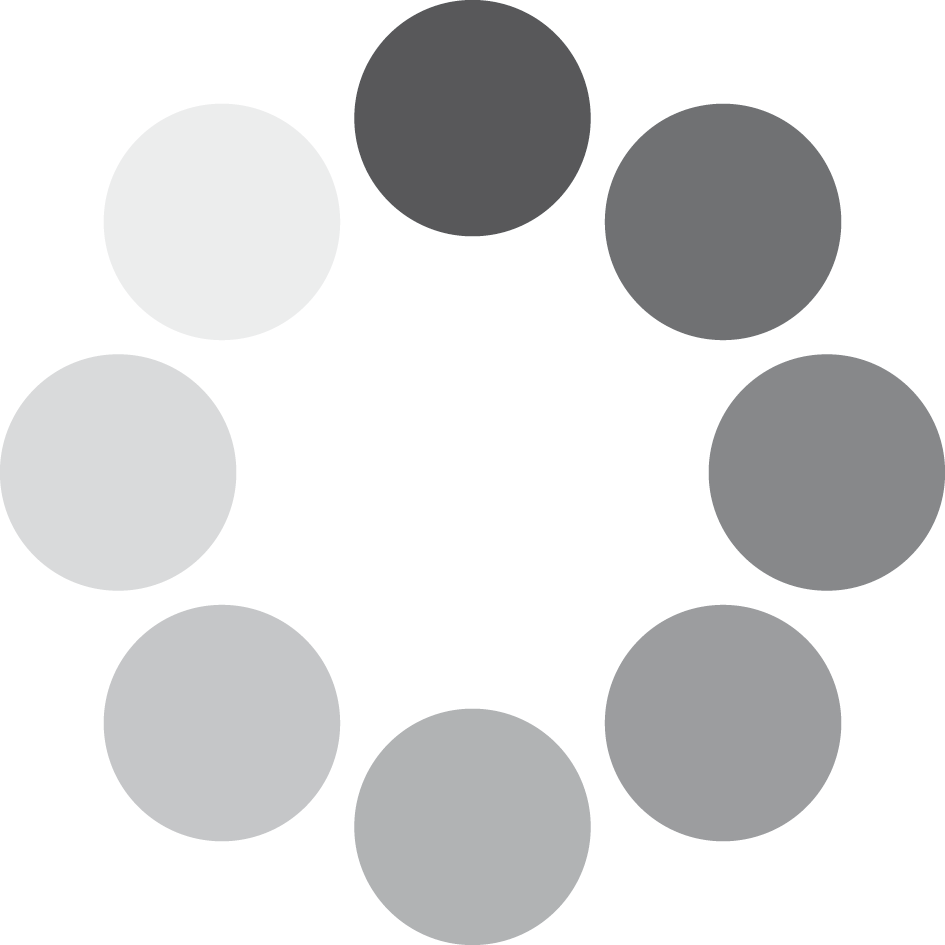पाम ऑयल: अदृश्य पदार्थ को सस्टेनेबल बनाने का प्रयास
पाम ऑयल का उत्पादन इस प्रकार करना चाहिए कि मानवाधिकारों का हनन न हो और प्रकृति और जैवविविधता को कम से कम नुकसान पहुंचे
On: Monday 13 May 2024

प्रतिभा बवेजा
आज ज्यादातर शॉपिंग कार्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, डिटर्जेंट जैसी चीजें देखी जाती हैं। हममें से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि रोजमर्रा की इन चीजों में एक सर्वव्यापक पदार्थ होता है, और वह है पाम ऑयल (पाम का तेल), जिसे अक्सर इसके कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
पाम ऑयल की कई खूबियां हैं, जैसे इसका सस्ता होना, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी, टिकाऊ होना, और प्रति हेक्टेअर अधिक उपज। इन सभी खूबियों के कारण पूरी दुनिया में प्रॉसेस्ड (तैयार) फुड, कॉस्मेटिक के सामान, पर्सनल केअर उद्योग और साफ-सफाई के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
इसका प्रयोग यहां तक कि बायॉफ्यूल में भी किया जाता है। अपनी इन खास खूबियों के कारण पाम ऑयल अन्य सभी वनस्पति तेलों से बेहतर है, इसलिए इसकी भारी मांग व खपत होती है और इस मांग और खपत में आगे भी कमी आने की कोई संभावना नहीं है।
भारत कच्चे पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। इस भारी मांग के पीछे कई कारण हैं जैसे भारत में पैकेज्ड फुड और कॉस्मेटिक सामान की मांग का लगातार बढ़ना, फुड प्रोसेसिंग में भारत की बड़ी भागीदारी और यहां से विकसित देशों को पैकेज्ड फुड का निर्यात।
भारत की कुल वनस्पति तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 70% है। भारत पाम ऑयल मुख्यतः इसके प्रमुख उत्पादक देशों इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता है। दुनिया भर में पाम ऑयल की भारी मांग ने इन विकासशील देशों को एक आकर्षक आर्थिक अवसर प्रदान किया है ।
मांग और दुविधा
पाम ऑयल की खेती में पेड़ लगाने के लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता होती है। जमीन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, खास कर इंडोनेशिया और मलेशिया के नम और गरम वर्षा वनों में बेतहाशा कटाई हुई है। वर्ष 1995 से 2015 के बीच इंडोनेशिया में हर वर्ष पाम की खेती के लिए एक लाख हेक्टेयर वन काटे गए। यह वन मिट्टी की सेहत, वर्षा की नियमितता और जैवभूरासायनिक चक्रों (बायोकेमिकल साइकिल) को बनाए रखते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक हैं।
ये वन सुंदालैंड, वैलेसिया और भारत-बर्मा के हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, सूंड़ वाले बंदर (प्रोबोसिस मंकी), जावा और सुमात्रा के राइनो जैसे जीव-जंतु रहते हैं। प्राकृतिक वास के नष्ट और कम होने के कारण इन जीव-जंतुओं के अस्तित्व को खतरा है।
एफएओ के अनुसार, दुनिया भर के वनों में लगभग 662 बिलियन टन कार्बन जमा है, जो जीवाश्म ईंधन में जमा कुल कार्बन से ज्यादा है। ऐसे में वनों की कटाई को रोकना जलवायु समस्या का एक सर्वमान्य और सस्ता समाधान है। पेरिस समझौते के जलवायु से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वस्थ वनों की कार्बन की छंटाई की क्षमता को मजबूत बनाना जरूरी है। पशुमांस और सोया समेत पाम ऑयल वनों की कटाई से होने वाले आधे से ज्यादा उत्सर्जन (emission) के लिए जिम्मेदार है, इसलिए प्रकृति और जलवायु दोनों की देखभाल करते हुए पाम ऑयल उद्योग को सस्टेनेबल बनाना जरूरी है।
पाम ऑयल की खेती से पर्यावरण के खतरों के अलावा मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी सामाजिक चुनौतियां पनपी हैं। बहुत-से मजदूरों को कड़ी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है। इन खतरों पर भी सावधानीपूर्वक विचार करना जरूरी है।
सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम
पाम ऑयल का उत्पादन बंद कर देना उचित समाधान नहीं है, क्योंकि उच्च उपज के कारण यह बाकि फसलों में सबसे ज्यादा लाभदायक है। इसलिए पाम ऑयल का उत्पादन इस प्रकार करना चाहिए कि मानवाधिकारों का हनन न हो और प्रकृति और जैवविविधता को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसी का नाम सस्टेनेबिलिटी है। दुनिया भर में पाम ऑयल की बढ़ती मांग और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संतुलन कायम करना जरूरी है। पाम ऑयल कीआपूर्ति श्रृंखला (supply chain) में कई भागीदार होते हैं, जिनके सहयोगात्मक प्रयास से पाम ऑयल का उत्पादन जिम्मेदारी के साथ करना ही समझदारी है।
इसी दिशा में राउंडटेबल ऑन सस्टेनेबल पाम ऑयल (आरएसपीओ) का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य पाम ऑयल उद्योग में सस्टेनेबिलिटी की ओर बदलाव लाना है। RSPO से प्रमाणित सस्टेनेबल पाम ऑयल कार्यक्रम (सीएसपीओ) के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि पाम ऑयल के उत्पादन में वनों को नुकसान ना पहुंचे और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी ना हो। भारत में, उत्पादकों के खेत से सीएसपीओ का आयात के साथ-साथ घरेलू प्रमाणित आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
पाम ऑयल की आपूर्ति श्रृंखला स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि कंपनियों को खेतों की जानकारी हो और वे इसकी स्पष्ट जानकारी दें पाये। इस तरह की आपूर्ति श्रृंखलाएं सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम हैं। भारत की भारी मात्रा में आयात को देखते हुए कच्चा पाम ऑयल खरीदने वाली भारतीय कंपनियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि आपूर्ति श्रृंखला स्पष्ट और पारदर्शी हो।
अंत में, भारत में भी पाम ऑयल के घरेलू उत्पादन के दौरान वे सभी कार्य करने चाहिए जो इस उद्योग को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए जरूरी हों, जैसे की मिल से निकलने वाले गंदे पानी (पीओएमई) का उपचार। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर भागीदारी के साथ स्थानीय समुदायों का बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण करना आवश्यक है।
हम क्या कर सकते हैं?
यह सच है कि पाम ऑयल उद्योग को सस्टेनेबल करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तन की जरूरत है। किंतु, बाजार में बदलाव लाने की वास्तविक ताकत उपभोक्ताओं के हाथों में है। उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद से पाम ऑयल की सस्टेनेबल मांग प्रभावित होती है और अपने ब्रांड की छवि को लेकर सतर्क कंपनियों पर दबाव पैदा होता है।
इसी दबाव से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में नियम लागू किये जा रहे हैं, जिनके तहत उत्पादन के दौरान वनों की कटाई प्रतिबंधित है। सजग उपभोक्ता उत्पादों के लेबल को पढ़ेंगे और सस्टेनेबल स्रोत से प्राप्त वस्तुएं ही चुनेंगे। वे उन कंपनियों का समर्थन करेंगे जो पाम ऑयल के स्रोत स्थान की स्पष्ट जानकारी देती हों।
ऐसे उपभोक्ताओं के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पाम ऑयल बायर्स स्कोरकार्ड (पीओबीएस ) भी उपलब्ध है जिसकी सहायता से वे सस्टेनेबल पाम ऑयल मंगाने वाली कंपनियों की पहचान कर उनका समर्थन कर सकते हैं।
उपभोक्ता खुद सामूहिक प्रयासों, और कार्यशालाओं का आयोजन कर जागरूकता फैला सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी पर चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। वे कंपनियों से पाम ऑयल आयात में पारदर्शिता के साथ-साथ उत्पाद कार्य को सस्टेनेबल बनाए रखने का आग्रह कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक शक्तिशाली साधन है, जिसकी सहायता से वे कंपनियों को यह संदेश दे सकते हैं कि प्रकृति संरक्षण एक ऐसा मूल्य है, जिसे वे अपने उपभोग विकल्पों में शामिल करना चाहेंगे।
निष्कर्ष
पृथ्वी की घटती प्राकृतिक संपदा और जलवायु के संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए, खेती और जमीन के परिवर्तन से होने वाले उत्सर्जनों को रोकने के लिए पाम ऑयल उद्योग को सस्टेनेबल बनाना आवश्यक है। हमें सजग उपभोक्ता बनना चाहिए और लोगों को जानकारी देते हुए आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। सस्टेनेबल मांग बना कर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पाम ऑयल के उत्पादन के लिए प्रकृति और जलवायु की कुर्बानी न दी जाए। सजग उपभोक्ता साथ मिलकर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं!
लेखक डॉ. प्रतिभा बवेजा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के सस्टेनेबल बिजनेस की एक्सपर्ट हैं
यह लेख सस्टेनेबल पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के #BePalmWise अभियान का एक हिस्सा है।