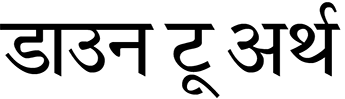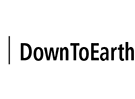कोयला उत्खनन का अर्धसत्य
कोयला उत्खनन से उस क्षेत्र का क्या हाल होता है? कोरबा के उदाहरण से समझिए, जहां वर्ष 1951 में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ
On: Thursday 02 July 2020

 साभार : विक्रम नायक (एकता परिषद)
साभार : विक्रम नायक (एकता परिषद) कोयला उत्खनन के स्थापित तर्क - विकास, रोज़गार, बिजली उत्पादन और राजस्व के अवसरों से जुड़े हुये हैं। इन तर्कों के अपने सत्य, असत्य और अर्धसत्य हैं। भारत सरकार (2018) के अनुसार शत-प्रतिशत गांवों में बिजली की आपूर्ति पूरी कर दी गयी है। वैसे तो सरकारी रिपोर्टों और आंकड़ों में यह लक्ष्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, लेकिन विश्व बैंक (2018) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों तक अभी भी बिजली नहीं पहुंच पायी है। अर्थात कोयले के उत्खनन, बिजली के उत्पादन और आपूर्ति के बीच का फासला न केवल वाद-विवाद का विषय है, बल्कि शोध का विषय यह भी है कि कोयले के उत्खनन से बिजली के उत्पादन, वितरण और फिर मुनाफे के मध्य लाभार्थी कौन है और वंचित कौन?
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को एक महत्वपूर्ण बिजली उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति करने वाले कोरबा जिले के बहुसंख्यक आदिवासी समाज नें इसकी क्या क़ीमत चुकाई है, बेहतर होगा वहां के जमीनी हकीकत से इसे समझा जाए।
भूवैज्ञानिक मानते हैं कि गोंडवाना सीरीज के चट्टान, बेहतरीन कोयले के प्रमुख स्रोत हैं। संयोगवश, कोरबा जिले का लगभग 30 फ़ीसदी भौगौलिक क्षेत्र इसी गोंडवाना सीरीज़ के चट्टानों से बना है। यह क्षेत्र करतला के उत्तर, कोरबा के पूर्व और कठघोरा के उत्तर में विस्तारित है। आज कोरबा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है।
वर्ष 1951 में कोरबा मे कोयले का उत्खनन शुरू हुआ। वर्ष 1958-59 में भिलाई इस्पात संयंत्र में आपूर्ति के लिये कोरबा के कोयला खदान क्षेत्रों के विस्तार में जिन गावों का विस्थापन हुआ उन्हें बताया गया कि देश के विकास के लिये उनका यह छोटा सा त्याग हमेशा याद रखा जाएगा। आदिवासी समाज ने भोलेपन से इस बात को स्वीकार कर लिया और देशहित में अपने जंगल और जमीनों से जुदा हो गये।
फ़िर एक-एक कर खदान खुलते गये - मौजूदा खदानों का विस्तार हुआ और हर बार उजाड़ने से पूर्व ग्रामवासियों को यही बताया गया कि देशहित में उनका यह योगदान हमेशा याद रखा जायेगा। आदिवासी समाज ने, न सिर्फ अपनी संस्कृति गवां दी बल्कि उनके अपने जल जंगल और ज़मीन के स्वामित्व के सवाल भी संविधान और विधानों के संहिताओं के बावज़ूद देशहित में पूरी तरह खारिज़ कर दिये गये।
कोरबा जिले का बड़ा भूभाग, संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत है - जहाँ पंचायत (विस्तार उपबंध) अधिनियम 1996 के अनुसार आदिवासी ग्रामसभाओं को विशेषाधिकार दिये गये हैं। छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहाँ इस क़ानून के लागू होने के लगभग 24 बरस बाद भी इसकी पूरी नियमावली नहीं बन पायी है। देशहित में अपना जल जंगल और जमीन दांव पर लगाने वाले बहुसंख्यक आदिवासी समाज के हिस्से आज केवल और केवल विपन्नता, उपेक्षा और ऐतिहासिक अन्याय है।
खदानों को संपन्नता और रोज़गार से जोड़ने के राजनैतिक तर्क और उसकी सामाजिक-आर्थिक विफ़लताओं का एक केंद्रबिंदु है- कोरबा जिला। कोरबा जिला सांख्यिकी विभाग (2018) के अनुसार लकड़ी के उत्पाद, सूती तथा रेशमी वस्त्र उद्यम, चमड़े के सामान आदि बनाने वाली इकाईयां समाप्त हो चुकी हैं। अर्थात स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक रोज़गार के अवसर बरसों पहले समाप्त घोषित हो चुके हैं।
कोरबा के जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार वर्ष 2017 में कोयला खदानों मे कार्यरत श्रमिकों की संख्या लगभग 14 हजार थी, जबकि इसी दौरान पंजीकृत बेरोज़गारों की संख्या इससे कई गुनी अधिक थी। यह आंकड़े बताते हैं कि खदानों के खुलने का अर्थ, स्थानीय लोगों के लिए न तो बढ़े हुये रोजगार के अवसर हैं और न ही यह ग़रीबी से मुक्ति का मार्ग है। आज कोरबा जिले के लगभग 40 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जिनमें से बहुसंख्यक आदिवासी ही हैं - आखिर उनकी इस ग़रीबी के जवाबदेह कौन है?
यह महज़ संयोग नहीं कि देशहित में उनके योगदान को देखते हुये ही भारत के पूर्व प्रगतिशील प्रधानमंत्री नें आदिवासी समाज को 'राष्ट्रीय मानव' तक कहा था। कहना मुश्किल है कि ऐसा उनके योगदान के लिये कहा गया अथवा आदिवासी समाज के मिटते हुये अस्तित्व को संरक्षित रखने के लिये चिंता व्यक्त की गयी। बहरहाल, संविधान के वायदे और कायदे, बहुसंख्यक आदिवासी समाज के लिये अर्थहीन ही साबित हुये हैं।
केंदई गांव की रुक्मिणी बाई कहतीं है कि बहुत हो चुका - एक बार तो सरकार और समाज साफ़ साफ़ कह ही दे कि मुट्ठी भर मुआवज़े के एवज में और क्या क्या हमसे लेना चाहते हैं। क्यों नहीं सरकार हमें मुट्ठी भर ही सही, अब तो ऐसी जमीन और जंगल का अधिकार दे जिसे फिर कोई छीन न पाये। हम अपनी संस्कृति और स्वाभिमान दोनों गवां चुके।
अगली पीढ़ी को देने के लिये आज इन निहत्थे हाथों में कुछ भी नहीं सिवाय उम्मीदों के जिसे अधिग्रहण का एक सरकारी फ़रमान खारिज़ कर सकता है। रुक्मिणी बाई मानती हैं कि ये नीलामी, धरती के नीचे दबे कोयले की नहीं बल्कि उस धरती के ऊपर सदियों से रह रहे निर्दोष आदिवासी समाज की है - जो विकास की बोलियों में दांव पर लगा है।
जिस विकास और रोज़गार के चकाचौंध वायदों के साथ वर्ष 1981 में गेवरा की कोयला खदान खोदी गयीं - वो सब कोयले के गुबार में धुंधले हो गये। गेवरा के खदान में गेट नंबर -1 पर खड़ा मंगतू राम कहता है कि जब तहसीलदार नें हमारी धनहा जमीन के बदले 3 लाख के मुआवज़े की पेशकश की तब ऐसा लगता था कि विकास और संपन्नता स्वयं चलकर हमारे दरवाज़े पर आयी है। लेकिन ज़मीन हमेशा के लिये खो देने का गहरा भय भी था। फिर एक दिन बिना कहे-सुने हमारे ज़मीन की घेराबंदी शुरू हो गयी।
फ़रमान आया कि 1 लाख रूपए के मुआवज़े के कागजातों पर दस्तखत करने कोरबा जाना पड़ेगा। हमें मालूम हुआ कि हम सब पराजित घोषित कर दिये गये हैं। मंगतू राम कहते हैं कि चौकीदार का यह ओहदा, मुझ जैसे बेरोज़गारों को शर्मसार करने के लिये काफ़ी है। मालूम नहीं मैं किस जमीन की और क्यों चौकीदारी कर रहा हूँ।
छत्तीसगढ़ के हरेक 12 कोयला खदानों में रुक्मिणी बाई और मंगतूराम आपको मिल ही जायेंगे। उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं - उससे क्या फर्क पड़ता है। फ़र्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता कि देशहित के नाम, उनके जंगल - ज़मीन की नीलामी किसने कर दी। फर्क पड़ना चाहिये था उस पूरी व्यवस्था को जिसने संविधान के वैधानिक वायदों और क़ायदों के ख़िलाफ़ उस पूरे आदिवासी समाज को विकास के चक्रव्यूह में निहत्थे खड़ा कर दिया -जहां देशहित के अर्थ कुछ भी हो सकते हैं। अंततः फर्क पड़ा तो केवल उस आदिवासी समाज को जिसके पास देशप्रेमी साबित होने के अलावा आज शायद और कोई दूसरा विकल्प है ही/भी नहीं।
(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक हैं)