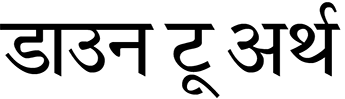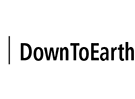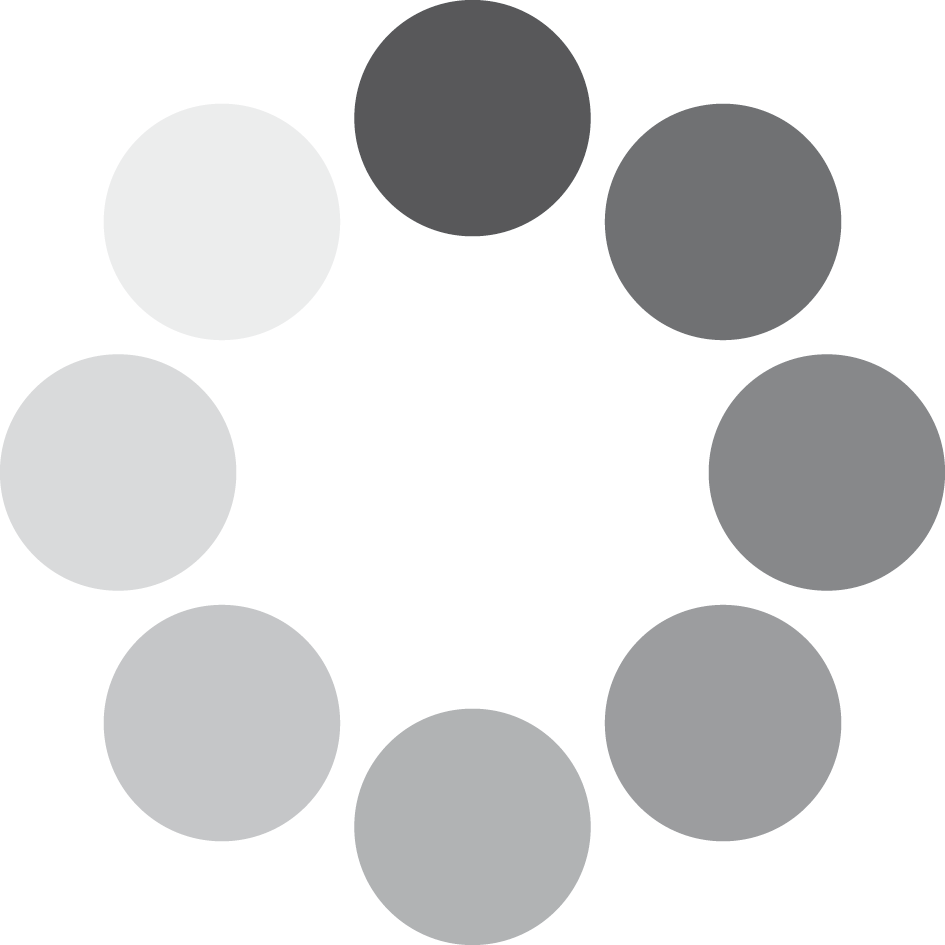सोलर पंप स्कीम पर पुनर्विचार की जरूरत
पीएम कुसुम योजना से भूजल दोहन बढ़ेगा, इसलिए इस स्कीम को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है
On: Wednesday 14 August 2019

 Photo: Creative commons
Photo: Creative commons केंद्रीय नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम योजना) के जरिए ही 17 लाख 50 हजार ऑफ ग्रिड पंप और 10 लाख ग्रिड पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 27750 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पंप लगेंगे। इसके अलावा 10 गीगावाट छोटे सोलर पावर प्लांट भी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार 34422 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगी।
इसका सीधा सा मतलब है कि 25750 मेगावाट सौर ऊर्जा से 3 हॉर्सपावर के 1.15 करोड़ पंप या 5 हॉर्सपावर के 70 लाख पंप चलाए जा सकते हैं। वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पंप खेतों में लगे हुए हैं। इनमें से 2.1 करोड़ पंप बिजली से चलते हैं और 90 लाख पंप डीजल से चलते हैं। कुसुम स्कीम के तहत इनमें से एक तिहाई से एक चौथाई पंप को तीन साल के भीतर सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।
बेहद तेजी से होने वाले इस परिवर्तन की कल्पना इसलिए साकार हो सकती है, क्योंकि बड़े व मध्य वर्गीय किसानों के लिए ये पंप खरीदना काफी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 30-30 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी, जबकि सस्ती ब्याज दरों पर 30 फीसदी लोन दिया जाएगा और किसान को केवल 10 फीसदी पैसा खर्च करना होगा। लेकिन क्या इतनी तेजी से होने वाले इस परिवर्तन से फायदा होगा नुकसान?
अगर इसका सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो थोड़े समय के लिए किसान की आमदनी बढ़ाने में यह योजना सार्थक साबित होगी। डीजल के मुकाबले सौर ऊर्जा सस्ती है। बिहार जैसे राज्य में जहां किसान डीजल पंप का इस्तेमाल अधिक करते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर पंप उनकी सिंचाई लागत को कम कर सकते हैं। इससे किसान अधिक से अधिक फसल बो सकता है, बल्कि ऐसी फसल भी बो सकता है, जिसमें पानी का इस्तेमाल अधिक होता है, इससे उसकी आमदनी बढ़ेगी।
पंजाब में, जहां पंप चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, किसानों को सालाना लगभग 7000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी जाती है। वहां सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप का इस्तेमाल बढ़ा कर इस सब्सिडी का बोझ कम किया जा सकता है। साथ ही, किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली कंपनियों को बिजली बेच कर अतिरिक्त आमदनी भी कर सकेंगे।
सोलर पंप का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सोलर का समय और सिंचाई का समय आपस में मेल खाता है। यानी कि, जब धूप की तेजी अधिक होती है, वही समय सिंचाई का भी होता है। इससे किसानों को लगभग छह घंटे तक सिंचाई के लिए बिजली मिल जाएगी। उन्हें सिंचाई के लिए रात-रात भर जागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में किसानों को सिंचाई के लिए रात में बिजली दी जाती है। कुल मिलाकर किसानों के लिए यह स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन क्या लंबे समय के लिए यह किसानों के हित में है?
भारत में सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारत में जमीन से निकाले जा रहे कुल पानी में से 90 फीसदी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता हैऔर भारत की कुल कृषि भूमि में से 70 फीसदी की सिंचाई भूजल से ही की जाती है। इससे जहां किसान की आमदनी और अन्न की उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन इससे भूजल का जमकर दोहन हो रहा है। यही वजह है कि कई राज्य में भूजल स्तर काफी गिर गया है। साथ ही, पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है और स्थिति काफी अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है।
भूजल स्तर उन राज्यों में अधिक गिरा है, जहां किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है या उनसे बिजली की कम कीमत ली जा रही है। ये राज्य हर साल लगभग 50 हजार करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दे रहे हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में लगभग 60 फीसदी जलभृत (एक्वाफायर) 2032 तक संकट पूर्ण स्थिति में होंगे। ऐसे में, बड़ी संख्या में लगने वाले सोलर पंपों से स्थिति और बिगड़ेगी, खासकर तब, जब भूजल के इस्तेमाल पर नियंत्रण नहीं होगा और कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी।
जैसे कि- जब किसान डीजल से पंप चलाता है तो उसका ध्यान डीजल की कीमतों पर रहता है और वे कम से कम पंप चलाता है, लेकिन यदि इसकी जगह सस्ते सोलर पंप लगा दिए गए तो वे पंप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे। जहां तक पंजाब हरियाणा की बात है तो यहां बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी इतनी अधिक है कि सरकारें किसानों को सोलर पंप लेने के लिए प्रेरित करेंगी, इससे भी भूजल दोहन बढ़ेगा।
कुल मिलाकर कुसुम स्कीम में भूजल दोहन को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्कीम से केवल भूजल दोहन ही बढ़ेगा। इसलिए इस स्कीम में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए।
पहला, यह स्कीम राज्यों में सिंचाई व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। लेकिन कुसुम उन्हीं राज्यों में लागू की जानी चाहिए, जो भूजल दोहन पर नियंत्रण और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का भरोसा दें।
दूसरा, सोलर पंप लेने वाले किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन अनिवार्य की जाए। भूजल इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाए, खासकर पंप साइज व बोरवेल की गहराई की निगरानी की जाए। साथ ही, किसानों को पानी का कम से कम खपत करने वाली फसल को बोने के लिए प्रेरित किया जाए।
तीसरा, ऑफ ग्रिड-सोलर पंप उन्हीं इलाकों में लगाने की इजाजत दी जाए, जहां ग्रिड नहीं पहुंचे हैं और भूजल प्रचुर मात्रा में है। बल्कि जहां भूजल प्रचुर मात्रा में है, वहां भी ऑफ ग्रिड सोलर पंप का इस्तेमाल गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए भी किया जाए या कोई ऐसा सामुदायिक मॉडल बनाया जाए, जिससे पानी की बर्बादी कम हो और अधिक से अधिक लोग पानी का इस्तेमाल कर सकें।
चौथा, ग्रामीण फीडरों का सोलराइजेशन पसंदीदा समाधान होना चाहिए, क्योंकि यह न केवल सबसे किफायती ह, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी प्रदान करेगा। हालांकि, यह बिजली दरों में वृद्धि के साथ होना चाहिए, जो भूजल दोहन को नियंत्रित करने और कृषि सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
अंतिम, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए, बिजली नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सौर पंपों और सौर ऊर्जा संयंत्रों से ग्रिड को आसानी से जोड़ने की अनुमति हो। साथ ही, किसानों को नियमित रूप से भुगतान किया जाए।
अक्षय ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा है, लेकिन यह हमेशा हरित समाधान की ओर नहीं ले जाती है। स्वच्छ ऊर्जा को हरित ऊर्जा बनाने के लिए समाधानों को व्यापक रूप से एकीकृत तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए।