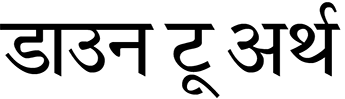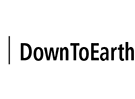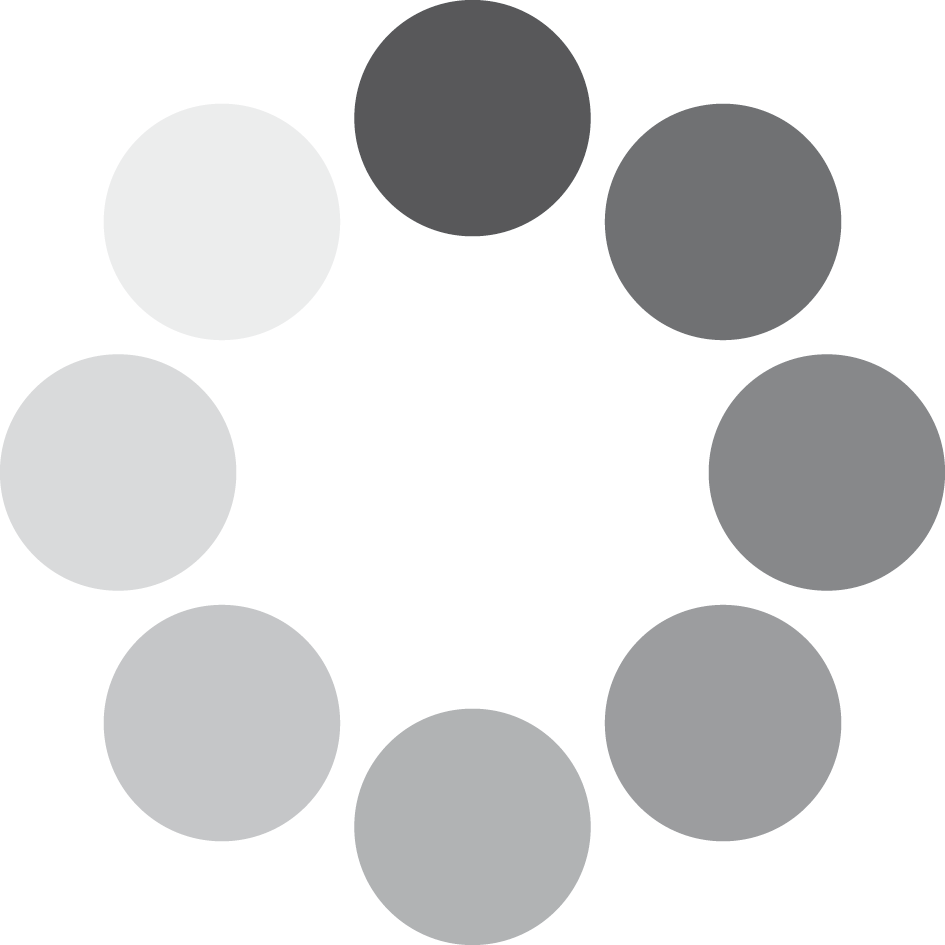डाउन टू अर्थ खास: जहां-जहां हैं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, वहां के लोग हैं ज्यादा बीमार
उत्पादन से लेकर इस्तेमाल और फिर ठिकाने लगाने तक प्लास्टिक उन लोगों के लिए खतरनाक है, जो लगातार इनके संपर्क में आते हैं
On: Thursday 25 April 2024
 “अगर आप यहां स्वास्थ्य जांच शिविर खोलने आए हैं तो प्लांट से झुंड में मजदूर जांच कराने आएंगे। यहां के बहुत सारे मजदूर त्वचा और श्वास से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं,” यह बात रफीक (बदला हुआ नाम) ने कही। रफीक ने हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नेफ्था टर्मिनल में एक दशक से अधिक समय तक काम किया है।
“अगर आप यहां स्वास्थ्य जांच शिविर खोलने आए हैं तो प्लांट से झुंड में मजदूर जांच कराने आएंगे। यहां के बहुत सारे मजदूर त्वचा और श्वास से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं,” यह बात रफीक (बदला हुआ नाम) ने कही। रफीक ने हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नेफ्था टर्मिनल में एक दशक से अधिक समय तक काम किया है।
नेफ्था, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रक्रिया के दौरान निकलता है और दुनिया के लगभग सभी प्लास्टिक निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रफीक बताते हैं, “पिछले लगभग दो वर्षों से मुझे श्वास में गंभीर संक्रमण है और डॉक्टर के मुताबिक इसकी संभावित वजह जहरीले पदार्थों का नाक के जरिए भीतर पहुंचना है।”
रफीक का मामला इकलौता नहीं है। साल 2020 में सिंहपुरा सिथाना गांव के सरपंच सतपाल सिंह ने अपने गांव में चल रहे रिफाइनरी प्लांट पर भूगर्भ जल को प्रदूषित करने, वायु गुणवत्ता खराब करने और आसपास के गांवों के लोगों की सेहत पर बुरा असर डालने का आरोप लगाते हुए प्लांट के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में मामला दर्ज कराया था।
इस संबंध में कौंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च-नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें उन्होंने पाया कि वर्ष 2015 से 2019 तक रिफाइनरी ने 8,500 लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाला है।
सतपाल सिंह बताते हैं कि यह प्लांट, राज्य की संपत्ति है और केस वापस लेने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी राजनीतिक दबाव बनाया गया था। नतीजतन 2021 में केस वापस ले लिया गया। हालांकि, केस तो वापस ले लिया गया है मगर इसकी वजह से प्लास्टिक के जीवन चक्र के साथ जुड़े जहरीले तत्व चर्चा के केंद्र में आ गए।
सभी प्लास्टिक या पॉलीमर (बड़े अणु) मोनोमर (एक अणु) को जोड़कर बनाया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। मनचाहा रंग, गुणवत्ता, आकार और मजबूती पाने के लिए प्लास्टिक के बहुलीकरण के दौरान कुछ (रंग, पूरक) जोड़े जाते हैं और प्रक्रिया में मदद के लिए अन्य (उत्प्रेरक, रोगन, घुलनशील) पदार्थों को शामिल किया जाता है।
 साल 2021 में एनवायरमेंटल साइंस एंड रिसर्च में छपे एक अध्ययन के मुताबिक, प्लास्टिक बनाने में 10,500 पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है।
साल 2021 में एनवायरमेंटल साइंस एंड रिसर्च में छपे एक अध्ययन के मुताबिक, प्लास्टिक बनाने में 10,500 पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है।
अध्ययन बताता है कि मोनोमर (प्लास्टिक बनाने के ब्लॉक) की तुलना में प्लास्टिक बनाने में ज्यादा संयोजी और प्रसंस्करण तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है।
इनमें से 55 प्रतिशत चिन्हित तत्व प्लास्टिक संयोजी, 39 प्रतिशत प्रसंस्करण में मददगार तत्व और 24 प्रतिशत मोनोमर की श्रेणी में आते हैं।
बुरा तो ये है कि इस्तेमाल किए गए पदार्थों में से 30 प्रतिशत तत्व सूचना के अभाव में अपने कार्य को लेकर गैर-वर्गीकरणीय होते हैं। यह अनिश्चितता इसलिए है क्योंकि कंपनियां अपने व्यापार की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक निर्माण प्रक्रिया और इसमें इस्तेमाल होने वाले तत्वों को छिपाती हैं।
प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नार्वे और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं के समूह प्लास्टकेम प्रोजेक्ट के एक अध्ययन में अनुमान लागाया गया है कि वर्ष 2021 और 2024 के बीच प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की संख्या बढ़कर 16,000 हो गई है।
विशेषज्ञों का हालांकि यह भी मानना है कि प्लास्टिक उद्योग में प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र तक 25,000 रसायनों का इस्तेमाल होता होगा।
इनमें से अधिकांश तत्व जहरीले होते हैं। इनमें बिसफेनोल (जैसे बिसफेनोल-ए या बीपीए), प्रति और पॉलीफ्लोरोआकाइल पदार्थ, थैलेट, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट और ऑर्गेनोफॉस्फेट फ्लेम रिटार्डेंट शामिल हैं।
प्लास्टिक में कुछ पदार्थ तो ऐसे ही मिल जाते हैं। इन्हें गैर इरादतन जोड़े गए पदार्थ (एनआईएएस) कहा जाता है। प्लास्टिक के उत्पाद प्राथमिक पैलेट को पिघला कर तोड़ मरोड़ कर बनाए जाते हैं।
इसी प्रक्रिया में एनआईएएस को इसमें मिला दिया जाता है और फिर यह पॉलीमर का हिस्सा हो जाते हैं। रिसाइक्लिंग या जलाने की प्रक्रिया में ये पॉलीमर में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि, एनआईएएस अज्ञात होते हैं इसलिए उनके प्रभाव के बारे में भी कुछ पता नहीं है। प्लास्टिक में मौजूद ये रसायन, प्लास्टिक बनने से लेकर इसकी रिसाइक्लिंग प्रक्रिया से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
उत्पादन के वक्त खतरा
प्लास्टिक के निर्माण के स्तर पर होने वाले प्रदूषण को समझने के लिए दिल्ली के गैर-लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने उन शहरों के स्वास्थ्य के आंकड़ों का विश्लेषण किया जिन शहरों में रिफाइनरी प्लांट हैं। भारत के 13 राज्यों में 21 पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी हैं। प्लास्टिक उद्योग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री उत्तरोत्तर काम करते हैं और चूंकि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला नेफ्था पेट्रोकेमिकल उद्योग से आता है, तो अक्सर दोनों उद्योग एक-दूसरे के करीब स्थित होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-5), 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि रिफाइनरी के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर रिफाइनरी से असर पड़ता है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि 13 राज्यों में से जिन आठ राज्यों में पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, उन राज्यों के उन जिलों में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में सांस के संक्रमण की घटनाएं अधिक हैं, जहां रिफाइनरी प्लांट हैं। हेल्थ सर्वे में त्वचा से संबंधित बीमारियो के आंकड़े दर्ज नहीं किए जाते हैं, जबकि पानीपत में स्थित रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूरों और इसके आसपास रहने वाले लोगों में ये एक आम समस्या है। इस तरह के तथ्य कई और अध्ययनों में भी सामने आए हैं। एन्वायरमेंटल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन कहता है कि पेट्रोकेमिकल उद्योगों के निकट रहने का संबंध कैंसर रोग से है।

इस्तेमाल के दौरान खतरा
चूंकि एडिटिव्स आमतौर पर पॉलीमर मैट्रिक्स से बंधते नहीं हैं, तो वे बाहर निकल जाते हैं और सांस के जरिए (पैकेजिंग सामग्री के जरिए हवा में फैले कण), भोजन के साथ (खराब गुणवत्ता वाले प्लास्टिक के कंटेनर में रखा भोजन खाने से) और त्वचा के छिद्रों को जरिए मानव शरीर के भीतर प्रवेश कर जाते हैं।
बहुत सारे अध्ययनों में प्लास्टिक के सामानों से भोजन, पेय पदार्थ और पर्यावरण में रसायनों के फैलने को लेकर पड़ताल की गई है। शोध बताते हैं कि रसायन के रिसाव में कई तत्व काम करते हैं। इनमें प्लास्टिक में रखे भोजन का तापमान (प्लास्टिक के कंटेनर में गर्म तरल पदार्थ रखने से कंटेनर से रसायन का रिसाव हो सकता है), पीएच वैल्यू (अम्लीय भोजन प्लास्टिक के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे रसायन का रिसाव हो सकता है) और प्लास्टिक में कितने वक्त तक सामान रखा जा रहा है, आदि शामिल हैं।
प्लास्टिक में जो सामान्य एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं, वे बीपीए और थैलेट हैं। बीपीए एक पहचाना अंतःस्रावी अवरोधक है, जो प्रजनन विकार, मोटापा और केंसर के खतरों से जुड़ा हुआ है। वहीं, थैलेट, हार्मोलनल असंतुलन, मानसिक असामान्यता और प्रजनन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव से संबंधित है।
प्लास्टिक में शामिल अन्य एडिटिव्स मसलन रोगाणुरोधी घटक और ज्वालारोधक, न्यूरोटॉक्सीसिटी और प्रतिरक्षा तंत्र में गड़बड़ी से जुड़े हुए हैं।
रिसाइक्लिंग के दौरान जोखिम
हालांकि, रिसाइक्लिंग को अहम समाधान के तौर पर प्रचारित किया जाता है, लेकिन प्लास्टिक से निकलने वाले जहरीले पदार्थ इस चरण में भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिल्ली के एक गैर-लाभकारी संगठन टॉक्सिक लिंक्स द्वारा इसी साल जारी की गई एक रिपोर्ट कहती है कि रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बने उत्पादनों में स्वीकार्य सीमा से अधिक हानिकारक रसायन पाए जाते हैं। अध्ययन के लिए रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से बने सामान लिए गए और उन्हें तीन वर्गों खाद्य के रखरखाव में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद, खिलौने और मिश्रित इस्तेमाल के उत्पाद में बांटा गया।
इसके बाद इनमें पांच प्रकार के रसायनों, बीपीए, नॉनिलफेनॉल, क्लोरिननेटेड पैराफिन, थैलेट और भारी धातुओं की मौजूदगी की जांच की गई। जांच में 15 नमूनों में से 10 नमूनों में रसायनों की मौजूदगी के संकेत मिले, 10 नमूनों में से 6 नमूनों में एक से अधिक रसायन की मौजूदगी थी और इनमें दो नमूनों में भारी मात्रा में रसायन पाए गए थे।
इसके अलावा प्लास्टिक रिसाइक्लिंग इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के शरीर में नाक और चमड़े के छिद्रों के जरिए रिसाइकल किए गए प्लास्टिक में मौजूद कार्सिनोजेनिक धातुओं मसलन आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम के शरीर में प्रवेश करने का खतरा रहता है।

वैश्विक संधि
विश्वभर में प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के नेतृत्व में बातचीत चल रही है, लेकिन तेल, गैस और प्लास्टिक उत्पादन करने वाले कुछ देश मसलन सउदी अरब, रूस और चीन एक प्रभावशाली संधि में रोड़ा डाल रहे हैं। यह संधि न केवल प्रदूषण खत्म करने बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी बात करती है।
हालांकि, बहुत सारे देशों और देशों के समूहों ने प्लास्टिक के निर्माण के साथ अन्य सभी प्रकार के उत्पादनों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है।
इनमें से एक कानून यूरोपीय संघ का रजिस्ट्रेशन, इवेलुएशन, ऑथोराइजेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल (आरईएसीएच) है। इसके तहत अगर एक कंपनी यूरोपीय संघ में प्रति वर्ष एक टन या उससे अधिक मात्रा में उत्पादन या रसायनों का आयात करती है, तो उसे यूरोपियन केमिकल्स एजेंसी (ईसीएचए) के तहत उन रसायनों का पंजीयन कराना होगा।
पंजीयन प्रक्रिया में रसायनों के गुणों और उनके इस्तेमाल के बारे में विस्तृत सूचना देना और इसके संभावित दुष्प्रभावों के आंकड़े उपलब्ध कराना शामिल हैं। पंजीकृत रसायनों के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए ईसीएचए, उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का अध्ययन करता है। भारी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले तत्व (एसवीएचसीएस) जैसे सर्किनोजेन, प्रजनन पर असर डालने वाले जहरीले धातु और म्युटाजेन आरईएसीएच के तहत प्राधिकार के अधीन हो सकते हैं।
ऐसी कंपनियों को इन तत्वों के इस्तेमाल या बाजार में इन्हें छोड़ने के लिए ईसीएचए से आधिकारिक अनुमति लेनी होगी और अगर सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, तो इन तत्वों के इस्तेमाल को सीमित किया जा सकता है या फिर इनका इस्तेमाल बंद भी हो सकता है।
आरईएसीएच, यूरोपीय संघ को कुछ खतरनाक रसायनों के उत्पादन, बाजार में उतारने या उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने का अधिकार देता है अगर वे रसायन मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए अस्वीकार्य स्तर पर जोखिम भरे हैं।
ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, चीन व ताइवान अन्य देशों के पास रसायन के इस्तेमाल और प्लास्टिक उद्योग में उपयोग होने वाले रसायनों को नियंत्रित करने के लिए नियम हैं। इनमें से कुछ देशों में तो नियमावली आरईएसीएच जितनी विस्तृत है।
साल 2023 में यूएनईपी में दी गई प्रस्तुति के मुताबिक, भारत, प्लास्टिक पॉलीमर का उत्पादन कम करने या बंद करने के लिए किसी भी तरह की सीमा तय करने/बाध्यकारी लक्ष्य के खिलाफ है। हालांकि, भारत ने कुछ कड़े उपाय अपनाने पर सहमति जताई है, जिसमें प्लास्टिक उत्पादन में चिंताजनक रसायनों के इस्तेमाल को नियंत्रित करना शामिल है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन समस्या है और संधि में प्रबंधन उपायों मसलन उठाव, प्रसंस्करण, रिसाइकल न हो सकने वाले कूड़े से ऊर्जा उत्पादन और उन्हें ठिकाने लगाने पर फोकस होना चाहिए। यद्यपि भारत में आरईएसीएच जैसा कोई कानून नहीं है, हां, रसायनों के पंजीयन, मूल्यांकन और इस्तेमाल को शासित करने के लिए कुछ नियमावलियां हैं।
मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल्स रूल्स 1989 एक अहम नियमावली है। इसके तहत आयात या निर्यात किए गए खतरनाक रसायनों का पंजीयन कराना होता है, लेकिन देश के भीतर तैयार किए गए रसायनों के इस्तेमाल पर इस नियमावली में चुप्पी है। यह नियमावली हादसों को रोकने, पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने का आदेश देता है।
इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो (जो रसायन समेत बहुत सारे उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए मानदंड तैयार करता है) ने उत्पादन, प्रयोग और प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग में रसायनों के इस्तेमाल के लिए कोई सीमा तय नहीं की है।
अधिनियम की जरूरत
केंद्रीय रसायन और खाद मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी क्षमता में से 67 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन को समर्पित है। देश में निर्माण उद्योग के नियमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाने की जरूरत है। भोजन को रखने में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के स्टैंडर्ड को लेकर अधिसूचना है लेकिन इसका पालन हो रहा है कि नहीं इसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है।
प्लास्टिक की रिसाइक्लिंग के लिए भी मानक है लेकिन इस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। इस क्षेत्र में पारदर्शिता बहुत अहम है। व्यापार की गोपनीयता की आड़ में रसायनों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने की प्रवृत्ति बंद करने की जरूरत है और ऐसी स्थिति में बौधिक संपदा अधिकारों को लेकर विशेषज्ञों के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है।