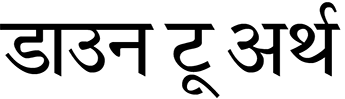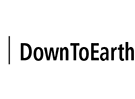नजरिया: मुसीबतें बढ़ा रहे हैं सीमेंट-कंक्रीट से बने भवन, बदलनी होगी मानसिकता
भवन निर्माण प्रक्रिया में बिना आमूलचूल बदलाव किए जलवायु परिवर्तन के वैश्विक व राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं
On: Tuesday 10 October 2023

 इलस्ट्रेशन: योगेन्द्र आनंद / सीएसई
इलस्ट्रेशन: योगेन्द्र आनंद / सीएसई भारत में सीमेंट और कंक्रीट के पक्के घर बनाने की प्रक्रिया करीब 110 साल पहले शुरू हो गई थी, पर सत्तर-अस्सी के दशक में बड़े शहरों में इसका चलन तेजी से बढ़ा। शुरू में सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के बने घर लोगों के बीच स्टेटस सिंबल थे। पश्चिम के अनुकरण और दिखावे ने इनके गुण-दोषों पर पर्दा डाल दिया। साफ, चमकदार और सफाई की मेहनत से छुटकारा देने वाले ये घर लोगों को खूब भाए। पत्थरों के टुकड़े, लोहे और सीमेंट से बनी कंक्रीट की छत और दीवारें दिन में अपनी क्षमता के अनुसार सूरज की गर्मी को सोखती हैं। फिर जैसे-जैसे रात ढलती है, कंक्रीट ऊष्मा को बंद घर में अंदर छोड़ती है, जिससे पक्के घर जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाते हैं।
कंक्रीट के बने घरों के बेतरतीब गर्म होने के कड़वे अनुभव को भारत ने आधुनिकता के नाम पर दरकिनार कर बड़े पैमाने पर आत्मसात कर लिया। अगले कुछ दशकों में बिल्डिंग डिजाइन के अंतरराष्ट्रीयकरण की आंधी में स्थानीय परंपरागत घर निर्माण के तरीके उड़ गए जो विभिन्न क्षेत्रों की मौसमी जरूरतों और अतिशयों को झेल पाने के गुणों से हजारों वर्षों में विकसित हुए थे। मिट्टी की मोटी और कुचालक दीवारें, घर के बीच में आंगन, घर के बाहर चारों ओर छायादार बरामदा, दो स्तरों की खुली और जालीदार खिड़कियां आदि भारतीय घरों की विशेषताएं थीं जो स्थानीय मौसम और जगह के हिसाब से सैकड़ों वर्षों के दौरान विकसित हुई थीं।
वैश्वीकरण की अंधी दौड़ में घर निर्माण की सारी स्थानीय शैलियां पश्चिम के भवन निर्माण के तरीके के बड़े पैमाने के सामान्यीकरण की भेट चढ़ गईं। कंक्रीट के जंगलों में पंखे, एसी और कूलर लगने लगे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में इजाफा कर एक अलग तरह की वैश्विक समस्या को बढ़ा रहे हैं। स्थानीय उपलब्ध सामान जैसे मिट्टी, स्लेट, चूना, फूस, कच्ची ईंट और खपरैल के बने घरों के जाने के साथ घर से आंगन, ओसारा और उसके साथ मौसम, पानी, हवा के साथ घर का तारतम्य की समृद्ध समझ व तकनीक चली गई।
पश्चिम की नकल की भेड़चाल में हमने न मौसमी जरूरत का ध्यान रखा और न ही इस्तेमाल होने वाली सामग्री का। नतीजतन, घर निर्माण की विविध और समृद्ध शैलियों का स्थान आधुनिक बॉक्सी शैली ने ले लिया। तभी तो आजकल गुवाहाटी जैसे पहाड़ी और बारिश वाले शहर की इमारतें अक्सर उत्तरी भारत के गुरुग्राम या दक्षिण भारत के चेन्नई, बंगलुरु या फिर पश्चिम के अहमदाबाद जैसी दिखती हैं या फिर यूरोप या उत्तरी अमेरिका के किसी भी शहर की इमारतों की तरह कांच के आवरण से लकदक।
यहां तक कि मरुभूमि में भी बॉक्सनुमा घर बन रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग की अवधारणा पर बने इक्का दुक्का इमारतों को छोड़ दें तो लगभग सभी इमारतें स्थानीय मौसम की अनुरूपता को दरकिनार कर पाश्चात्य शैली में बनीं हैं या बन रही हैं। पक्के और लंबे वक्त तक चलने की लालसा में प्रधानमंत्री आवास जैसी सरकारी योजनाओं में भी एक कमरे के ही सही, पक्के मकान बनने लगे हैं। फूस के घर की शांति और ठंडक लोग भूलने लगे।
जलवायु परिवर्तन के दौर में पक्के घर
जलवायु परिवर्तन में दौर में स्थानीय घर निर्माण के तरीकों के स्थान पर संपूर्ण भारत खासकर, शहरी क्षेत्रों में लोहा, सीमेंट, कंक्रीट और कांच आधारित घर निर्माण की पश्चिमी पद्धति एक बड़ी गलती साबित हो रही है। गर्मी में जिसकी शुरुआत अब बसंत में ही हो जा रही है, ये बॉक्सनुमा घर जरूरत से ज्यादा तप रहे हैं। इनमें रहना या काम करना दुरूह होता जा रहा है। इसके चलते एयर कंडिशन की बेतहाशा जरूरत और उसी अनुपात में ऊर्जा की खपत बढ़ रही है।
एयर कंडिशनिंग के ज्यादा इस्तेमाल से गर्म हवा घरों के बाहर सड़क और गलियां को गर्म करती है और परिणामस्वरूप हमारे शहर “हीट आइलैंड” के केंद्र बन रहे हैं। मौजूदा आधुनिक घर निर्माण के तरीकों की दोहरी मार ऊर्जा की अधिक खपत और “अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट” के रूप में पड़ रही है जिसके कारण शहरों का तापमान आसपास के मुकाबले पांच डिग्री सेन्टीग्रेड तक बढ़ जाता है। हमारे शहर धीरे-धीरे कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं। बड़े शहरों के बाहर एक नए शहर का निर्माण ऐसा प्रतीत होता है जैसे परती जमीन पर ताश के पत्तों सरीखी खड़ी बहुमंजिला इमारतें हीटिंग टावर हों।
1990 के दशक में मुक्त अर्थव्यवस्था अपनाने के साथ ही भारत की वास्तुकला तेजी से बदलनी शुरू हुई। घरों से आंगन, छायादार बरामदे, स्थानीय सामग्री से बनी मोटी दीवारें जिसमें सुरखी, चूना, गुड़, मसूर की दाल, पत्थर आदि इस्तेमाल होते थे, गायब होने लगे। जगह की कमी, महंगाई, तेज गति से निर्माण का दवाब आदि कारणों से भवन निर्माण की पश्चिमी शैली को व्यापक मान्यता मिलती चली गई। इनसे हमारे देश के वास्तुविदों और इंजीनियरों को पकी-पकाई शैली मिल गई जिसकी नकल करने में लोगों ने खुद की मौलिकता को तिलांजलि दे दी।
एक अनुमान के मुताबिक, क्षेत्रीय जरूरत के हिसाब से स्थानीय शैली में बने घरों की अपेक्षा पश्चिमी शैली में बने पक्के घरों में बिजली की पंद्रह गुना तक ज्यादा आवश्यकता होती है। इसका एक अच्छा खासा हिस्सा घर को ठंडा करने में खप जाता है। इससे जहां एक तरह शीतलन में ज्यादा ऊर्जा खप रही है, वहीं एसी की गर्म हवा और कांच की खिड़कियों से परावर्तित सूरज की किरणें बाहर का तापमान कई डिग्री तक बढ़ा देती हैं और इस पॉजिटिव फीडबैक के कारण ऊर्जा की जरूरतें उत्तरोतर बढ़ती जा रही है।
यूनाइटेड नेशन की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कुल कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 40 प्रतिशत भवन और भवन निर्माण से आता है जिसमें कहीं न कहीं स्थानीय परम्परागत घर निर्माण की शैली से दूरी और अत्यधिक ऊर्जा जरूरतों से लैस घरों का भी योगदान प्रमुख है।
लोहा, सीमेंट, कंक्रीट और कांच आधारित पाश्चात्य भवन निर्माण शैली ने न सिर्फ हमारे घरों का भौतिक स्वरूप बदला है, बल्कि अनेक पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं खड़ी कर दी हैं जिसमें गली, फुटपाथ, पार्क समेत अन्य खुली जगहों का कंक्रीटीकरण प्रमुखता से शामिल है। बेतहाशा खुली जगहों के पक्कीकरण के कारण शहरों में बारिश के पानी और उसके भूमिगत जल के रूप में बदल जाने के संतुलन को बुरी तरह से प्रभावित हुआ और नतीजा थोड़ी सी भी बारिश के बाद हमारे शहर तैरने लगे।
शहरी बाढ़ अब बारिश के दिनों में हर साल प्राकृतिक आपदा का स्वरूप लेने लगी है। मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम, पंचकूला सरीखे शहरी क्षेत्र बाढ़ की त्रासदी का शिकार बनते जा रहे हैं। एक दौर था जब हमारे गांवों को शहरों से जोड़ने वाली खरंजा सड़कें बनती थीं। अब गांव की विभिन्न योजनाओं में भी पक्की कंक्रीट की सड़कें शामिल हो गईं हैं। पक्कीकरण की होड़ में हम यह भूल गए कि यह धरती बारिश के पानी को सोखती है और उसी से हमारा भू-गर्भ जल रिचार्ज होता था।
बेतहाशा आधुनिक भवन निर्माण के कारण सीमेंट, पत्थर और लोहे की मांग बढ़ती जा रही है। सीमेंट और कंक्रीट निर्माण के लिए गिट्टियों वाले पहाड़ बड़े स्तर पर तोड़े जा रहे हैं। अकेले सीमेंट उत्पादन से सालाना वैश्विक कार्बन डाईऑक्साइड का लगभग 5 प्रतिशत तक उत्सर्जित होता है। कंक्रीट बनाने और जमाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी की खपत होती है, जो दुनिया के औद्योगिक जल उपयोग का लगभग दसवां हिस्सा सोख लेता है। रेत भवन निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसके लिए अवैध खनन द्वारा नदियों की पेटियां खाली होती जा रही हैं जिसके चलते नदी तंत्र, भूमिगत जल, बहाव की दिशा और प्रवृति और जल संग्रहण के आपसी संतुलन बिगड़ने से बड़े स्तर पर पानी की समस्याएं सामने आ रही हैं।
पेरिस समझौते के आलोक में भवन और भवन निर्माण से कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी तरफ नेशनल कूलिंग प्लान के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में केवल 8 प्रतिशत भारतीय घरों में एयर कंडिशनिंग की सुविधा है, पर 2040 तक ऐसे घरों की संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो 2070 तक “जीरो इमिशन” लक्ष्य के राह में बड़ी बाधा है। ऐसी परिस्थिति में भवन निर्माण, उसके इस्तेमाल और रखरखाव की प्रक्रिया में बिना आमूलचूल बदलाव किए जलवायु परिवर्तन के वैश्विक और राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करना संभव प्रतीत नहीं होता।
ऐसा करने के लिए मौसम के मुताबिक, स्थानीय सामानों से घर बनाने की क्षेत्रीय शैली को एक बार फिर से जीवित करने की जरूरत है। इस दिशा में पॉलिसी और अकादमिक स्तर पर काम भी शुरू हुआ है, जिसमे ग्रीन बिल्डिंग के लिए क्षेत्रीय दिशा-निर्देश और मानक भी तय किए गए हैं पर अभी भी वर्नाकुलर आर्किटेक्चर के लिए माहौल नहीं बन पा रहा है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्वीकार्यता अहम है।
आज भले ही हॉलो ब्रिक बनाने में हमने छोटे स्तर पर ही सही दीवारों के तापमान को कम करने में सफलता हासिल की है। दूसरी तरफ अपने फूस के घरों को किसी शहर के पिकनिक स्पॉट या ढाबे में तब्दील कर दिया हो पर सच्चाई यही है कि अब भी हम व्यापक रूप से माचिस के डिब्बों जैसा ही कंक्रीट के घर बना रहे हैं और वहीं रहकर गुजारा कर रहे हैं। जरूरत है अपनी शैली को परिष्कृत और परिमार्जित कर अपनाने की जिससे हम जलवायु परिवर्तन का सामना करते हुए टिकाऊ विकास की दिशा में कदम उठा सकें।
(कुशाग्र राजेंद्र एमिटी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट विभाग के प्रमुख व विनीता परमार विज्ञान शिक्षिका एवं “बाघ विरासत और सरोकार” पुस्तक की लेखिका हैं)