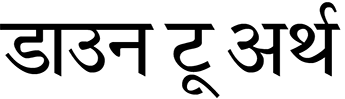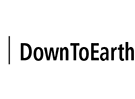पंचायती राज के शेष अर्थ
पंचायतों और ग्राम सभाओं की लगभग आधी आबादी अपने उपेक्षित अधिकारों के अंधेरों में अब भी असहाय है
On: Tuesday 25 April 2023

 साभार: विक्रम नायाक
साभार: विक्रम नायाक पंचायती राज की नैतिक अवधारणा में ग्राम सभा और पंचायत, व्यवस्था तंत्र की परिधि का केन्द्रबिन्दु है। भारत जैसे महान समाजवादी गणराज्य में - लोगों की जो भूमिका, जवाबदेही, अधिकार और अधिकारों की मान्यता 'पंचायती राज' के विधानों में दर्ज है, वह ऐतिहासिक हो सकती थी, यदि पंचायती राज के संवैधानिक भावनाओं और संभावनाओं के दायरे में कम से कम 'जल जंगल और जमीन' के कानूनों के औपनिवेशिक काया और आत्मा में भी परिवर्तन किया जाता।
इस दृष्टिकोण से पंचायती राज को राजनैतिक सहूलियत के मुताबिक मानना–न-मानना और उनके प्रत्याशित-अप्रत्याशित परिणामों ने संगठित रूप से इसे अब तक तो 'जल जंगल और जमीन' पर तो वंचितों के अधिकारों के संभावित समाधानों को लगभग असफल ही साबित किया है।
स्वाधीन भारत के जमीन और जंगल संबंधी अधिकांश कानून और उसे लागू करने वाला तंत्र प्रामाणिक रूप से औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त है। सेंटर फॉर पालिसी रिसर्च में लैंड राइट्स इनिशिएटिव की प्रमुख नमिता वाही और उनकी टीम के द्वारा भारत सरकार और चुने हुए 8 राज्य सरकारों के माध्यम से लागू कानूनों - उनकी प्रक्रियाओं और परिणामों का अध्ययन किया गया।
यह भूमि संबधी शोध बताता हैं कि भारत सरकार तथा 8 राज्यों के जिन 480 भूमि कानून का अध्ययन किया गया उनमें से लगभग 100 से अधिक भूमि कानून वर्ष 1947 के पूर्व के हैं। इसीलिये कुछ हद तक इन कानूनों को लागू करने वाला भूमि प्रशासन तंत्र भी औपनिवेशिक संहिताओं से बाध्य है।
अर्थात मौजूदा भूमि प्रशासन तंत्र के विधान और व्यवहार कुछ मायनों में औपनिवेशिक हैं। अर्थात भारत के 7.5 लाख से अधिक गांवों में रहने वाले लोगों के भूमि अधिकारों और आजीविका से जुड़े सवाल-जवाब का संदर्भ और समाधान तंत्र, औपनिवेशिक है। अर्थात भूमि अधिकारों के संकेतक, वैधानिक-उपनिवेश बनाम भूमि-प्रशासन तंत्र के स्थायी विरोधाभासों के रूप में चिरस्थायी चुनौतियां बनी हुई हैं।
अर्थात इसका समग्र परिणाम यही हुआ कि गांवों में रहने वाली 65 करोड़ आबादी के जमीन संबंधी सरोकार - औपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र से समाधान के मुगालते में थे /रहे हैं/और शायद बने रहेंगे।
जंगल के औपनिवेशिक कानूनों का चेहरा और चरित्र तो और भी संदिग्ध है। वास्तव में आदिवासी समाज को जंगल-जमीन में ‘अतिक्रमणकर्ता’ घोषित करना - भारतीय वन अधिनियम (1927) और औपनिवेशिक वन प्रशासन की सफलता रही तो उसके सापेक्ष सबसे बड़ी असफलता इस औपनिवेशिक कानून का जारी रहना है।
दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी कानून ने 8 करोड़ से अधिक लोगों को उनकी अपनी ही मातृभूमि में ‘अतिक्रमणकर्ता’ घोषित नहीं किया, जैसा भारत के मौजूदा औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम (1927) ने किया।
लेकिन भारतीय वन अधिनियम (1927) इस मायनों में भी ऐतिहासिक है कि वनों के संरक्षण की उनकी तमाम सदाशयताओं और छद्म दावों और भ्रामक आंकड़ों और उन पर निर्मित तथाकथित वन-संरक्षण की परियोजनाओं के साथ-साथ भारत में वन का क्षेत्रफल तो उत्तरोत्तर बढ़ता रहा, लेकिन जंगलों की सघनता और जैवविविधता लगातार गिरती ही रही है। तो फिर (अ)संवैधानिक वन कानून और उसे लागू करने वाले (औपनिवेशिक) वन प्रशासन की सफलता किसे और क्यों माना जाया जाए?
सवाल शेष है कि क्या ‘जल-जंगल और जमीन’ पर लोगों के गणतांत्रिक समाजवादी अधिकारों की राह में वैधानिक उपनिवेशवाद सबसे बड़ी बाधा है ? या पंचायती राज की पूर्ण अवधारणा और अपूर्ण वैधानिक प्रावधानों के अंतर्द्वंद ही केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के लिये (स्व)निर्मित अवसर है ?
या लोगों के अपने ही नागरिक अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता ही उसके अपात्र होने का अभिशाप है? या स्वयं राज्य ही, संसदीय विशेषाधिकारों के सापेक्ष गांवों के गणतांत्रिक अधिकारों को अप्रासंगिक मान चुका है? दरअसल इनमें से और इसके अलावा, व्यावहारिक गणतंत्र से जुड़े और अब तक अनुत्तरित सभी सवालों का उत्तर तलाशे और तराशे बिना 'पंचायती राज' सजीव शब्दों और भावनाओं के साथ अपनाया और लागू किया जा सकता है - इसमें संदेह के वाजिब कारण हैं।
झारखण्ड में वर्ष 1947 में ताना भगतों के कृषि भूमि के सुरक्षा के लिये लागू भूमि कानून (दी रांची डिस्ट्रिक्ट ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947) अथवा नागालैंड में वर्ष 1970 से लागू परंपरागत कृषि भूमि सुरक्षा कानून (दी नागालैंड जूमलैंड एक्ट 1970) अथवा पंजाब में शामलात भूमि पर दलितों के अधिकारों को स्थापित करता वर्ष 1961 का भूमि कानून (पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट 1961) अथवा वर्ष 1979 से कर्नाटक के आदिवासियों और दलितों के भूमि की सुरक्षा के लिये लागू कानून (दी कर्नाटक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब (प्रोहिबेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरटन लैंड) एक्ट 1979) आदि का अनुपालन जिस व्यवस्था के अकर्मण्यता और अयोग्यता के आखेट है, वह अब तक अनुत्तरित खड़े वाजिब संदेहों के प्रासंगिक और जीवित प्रमाण हैं।
यह वाजिब संदेह ही भारत के सबसे वंचित आदिवासी और दलित समाज को यह अधिकार और अवसर देता है कि वह राज्य आयोजित/ प्रायोजित व्यवस्थागत अक्षमताओं को न केवल उजागर करे बल्कि ऐसे हरेक कानूनों का सार्थक विकल्प भी राज्य के सामने रखे।
गौरतलब है कि देश के अनेक पंचायतों ने सार्थक विकल्पों को सरकार और समाज के सामने रखा और सरकार को जनतांत्रिक निर्णय लेने के लिये सफलतापूर्वक प्रेरित भी किया। उड़ीसा में नियमगिरि, केरल में प्लाचीमाडा, महाराष्ट्र में मेंढ़ालेखा और छत्तीसगढ़ में लोहंडीगुड़ा इसके ऐतिहासिक और सफल उदाहरण हैं।
वास्तव में यह सभी प्रकरण और उसमें ग्राम सभाओं / पंचायतों के माध्यम से हासिल सफलतायें यह साबित करती हैं कि ग्राम सभाओं / पंचायतों के सुझावों को मौजूदा औपनिवेशिक कानूनों और उनकी विसंगतियों को समाप्त करने का माध्यम बनाया जा सकता है और ऐसा होना भी /ही चाहिए।
ऐसे में आप इस आधे-अधूरे निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि गणतंत्र स्थापित करने में राज्य तो सफल ही रहा, लेकिन समाजवादी गणतंत्र के बरक्स जनता अपने अधिकारों और दायित्वों को भूल गई। यकीनन समाजवादी गणराज्य के 74 बरस में गणतंत्र पूरी तरह प्रतिबद्ध और परिपक्व हो ही जाने चाहिये थे / लेकिन ऐसा नहीं हो पाना - सामूहिक असफलता से कहीं अधिक सामूहिक नैतिक - राजनैतिक शून्यता हैं, जिसके परिधि में राज्य के परम पवित्र संवैधानिक मूल्य हैं, लेकिन केंद्र में हो सकने वाले पंचायतों और ग्राम सभाओं की लगभग आधी आबादी अपने उपेक्षित अधिकारों के अंधेरों में अब भी असहाय है।
सात दशकों के गणतंत्र के बाद अब उसे निर्णायक व्यवस्था तंत्र में स्थापित अथवा विस्थापित करना केवल राज्य का नहीं बल्कि शेष समाज का भी संवैधानिक दायित्व है - और होना ही चाहिये। भारत के लगभग 750,000 इन ग्रामसभाओं और महात्मा गांधी के शब्दों में भारतीय प्रजातंत्र की बुनियादी इकाईयों (ग्रामसभाओं) का सार्थक अमृत महोत्सव तो उसके साथ ही आरंभ होगा।
(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं)