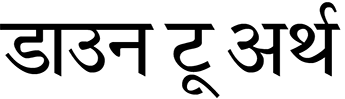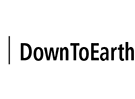ग्रामीण विकास का अर्धसत्य
गावों से उम्मीदों की गठरी बांधे जिन लाखों वंचितों ने शहरों को अपना अस्थायी आशियाना बनाया, एक महामारी की आशंका ने उसकी वास्तविकता को बेनकाब कर दिया है
On: Thursday 28 May 2020
.jpg)
 साभार: विक्रम नायक, एकता परिषद
साभार: विक्रम नायक, एकता परिषद महात्मा गांधी, आजीवन मानते रहे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। ‘हिन्द स्वराज’ के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को न केवल बेबाकी से देश और पूरी दुनिया के समक्ष रखा किया बल्कि भारत के राजनैतिक और आर्थिक स्वाधीनता के लिये संघर्षरत लाखों-करोड़ों लोगों को भारत के भावी विकास का मार्ग भी दिखा दिया। फिर कुछ बरसों के बाद 1934 में जिन अनेक मतभेदों के आधार पर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया, उनमें एक प्रमुख था - भारत के भावी विकास के लिए सबसे उपयुक्त साधन और उसकी शुचिता। राष्ट्रपिता मानकर भी ग्रामीण भारत के उत्थान के उनके विचारों और मार्ग को लगभग पूरी तरह खारिज़ किया जाना एक ऐसी अक्षम्य उपेक्षा है जिसके लिये समाज और सरकार दोनों ही जवाबदेह हैं।
महामारी के त्रासदी से हताश होकर गावों की ओर लौटते लाखों लोगों का कारवां, जिस सपने को गवां चुका है उसे जिलाने में सरकार और समाज कितना सक्षम है, यह आज के मौजूदा दौर का सबसे कठिन अनुत्तरित प्रश्न है। कठिन इसलिये कि किसी गलत दिशा में हमनें जाने-अनजाने एक लंबा रास्ता तय कर लिया है। और अनुत्तरित इसलिये कि अपने मार्ग को गलत न मानने की राजनैतिक जिद, व्यवस्था को बाध्य करती है कि गलत को भी सही कहे और साबित करे । समाज का संत्रास इससे कहीं और अधिक गहरा है, जहाँ यह स्वीकारने में कहीं हिचक ही नहीं रही कि गावों से श्रमशक्ति का पलायन उनके शहरों को सस्ते मजदूर मिलने का वांछित परिणाम है।
इसलिये ग्रामीण विकास एक ऐसा सपना रह गया जिनके नाम पर मंत्रालय संचालित करने की औपचारिकता तो विगत दशकों से जारी है लेकिन एक गहरी 'नीतिगत शून्यता' को लगभग नज़रंदाज़ करते हुये दबे पांव आगे बढ़ने के छद्म अहसास के साथ।
वह भी तब, जब विगत लगभग चार दशकों से अमूमन सभी नीतियों और नियतियों का ज़ाहिर-अजाहिर लक्ष्य ‘ग्रामीण समाज’ के त्याग और खून-पसीने से सभ्य शहरी समाज के तथाकथित विकास की बुनियाद रखना था। एक अनुमान के मुताबिक़ विगत पांच दशकों में औसतन प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक गांव को गवांते हुये हमनें शहरीकरण का जो नायाब नमूना खड़े किया है, उसमें इन ग्रामीणों की नयी बस्तियों को शहरी (झुग्गी) बस्तियों का नया नाम देने के अलावा और कोई उल्लेखनीय सफ़लता है ही नहीं।
वास्तव में ये नामहीन और सम्मानहीन बस्तियां, आधुनिकता के झूठे आवरण में लिपटे शहर और शहरवासियों द्वारा उस सस्ते श्रमशक्ति के प्रति उपेक्षा की जिंदा मिसालें हैं, जिसे 1956 में भारतीय संसद द्वारा पारित ‘द स्लम एरिया (इम्प्रूवमेंट एंड क्लीयरेंस) एक्ट’ के वैधानिक प्रतिबद्धतताओं के बावज़ूद भी कभी शिद्दत से लागू नहीं किया जा सका। यदि भारत में आज शहरों (लगभग 8000) से कहीं अधिक तथाकथित वैध-अवैध 'झुग्गी बस्तियों' (लगभग 40000) की संख्या है तो इसे शहरीकरण के साथ साथ ग्रामीण विकास की भी समग्र विफ़लता माना जाना चाहिये। शेष परिस्थितियों में सुधार तो उसके बाद ही संभव है।
गावों से उम्मीदों की गठरी बांधे जिन लाखों वंचितों ने शहरों को अपना अस्थायी आशियाना बनाया उसकी वास्तविकता को एक महामारी की आशंका ने आज़ पूरी तरह से बेनक़ाब कर दिया है। आधुनिक भारत के स्वप्नदर्शी योजना के स्मार्ट महानगरों और उसके मालिकों नें इन झुग्गी बस्तियों के साथ जो व्यवस्थागत अन्याय किया है उसकी पीड़ा मौजूदा महामारी से कहीं अधिक गहरी और स्थायी है।
बहरहाल, शहरी विकास की आधी-अधूरी नीतियों और ग्रामीण विकास की नीतिगत शून्यता के जिस दौर में सरकार और समाज 'विकास' के जिन लक्ष्यों को हासिल करने का दावा कर रहे है, वर्तमान महामारी और उससे उपजी लाचारी नें उसे पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है। हम एक ऐसे दोराहे पर आकर निहत्थे खड़े हो गये हैं जहाँ शहरी और ग्रामीण विकास दोनों की वास्तविकतायें पूरी तरह छद्म साबित हो चुकी हैं।
महामारी की अनिश्चितता और असुरक्षा से निराश होकर, लगातार 11 दिन तपते धूप में भूखे प्यासे बिहार के अपने गांव लौटीं मालती देवी कहती हैं कि मेरी नज़र में 'सपनो की दिल्ली' पूरी तरह से बेनक़ाब हो चुकी है। महामारी से अधिक पीड़ा, उस अपमान का है जिसे मुझ जैसे लाखों लोगों ने देखा और महसूस किया है। मुंबई से गिरते -पड़ते गांव वापस आये मध्यप्रदेश के माखन सिंह अहिरवार कहते हैं कि पेट और परिवार पालने की मज़बूरी नें मुझे जिन झुग्गी बस्तियों में धकेल दिया था, उस पीड़ा और उपेक्षा की दुनिया को अब शायद हमेशा के लिये पीछे छोड़ आया हूँ। मालती और माखन उस पूरी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिन्हें उनकी विपन्नता ने नहीं बल्कि सभ्य समाज के लालच नें उस दुनिया में धकेल दिया जहाँ एक महामारी भर नें उन्हें 'दूसरे दरजे' के नागरिक होने का गहरा अहसास करवा दिया।
एकता परिषद द्वारा लगभग 35000 मज़दूरों के साथ किया सर्वेक्षण बताता है कि अब तक मात्र 28 फ़ीसदी श्रमिक ही वापस अपने आजीविका के लिये शहर जाना चाहते हैं। यदि इसे केवल मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष न माना जाये तो भी इसे लाखों श्रमिकों द्वारा गावों में फैले अपनी जड़ों के प्रति जिंदा हुये लगाव और सुरक्षा के गहरे अहसास का प्रमाण मानना ही चाहिये । दुर्भाग्य से यह पक्ष समझ पाने में हमारी सामूहिक असफ़लता किसी ऐसे असंतोष को भड़का सकती है जिसे राजनैतिक तौर पर मौजूदा नीतियों और नीयतों से नियंत्रित करना लगभग असंभव है और होगा।
भारत में एक यथार्थपरक ग्रामीण विकास नीति, लगभग दो-तिहाई ग्रामीण जनसंख्या का एक ऐसा सपना है जिसे आज साकार करने की ज़रूरत है। यह नीति इसलिये आवश्यक है क्यूंकि - भूमि और कृषि और वनसंपदा आधारित बहुसंख्यक लोगों के लिये यह संस्कृति और आजीविका की बुनियाद है। इन संसाधनों पर उनका वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करना ही होगा। इस कार्य मे कोताही का अर्थ यह मान लिया जायेगा कि समाज और सरकार, ग्रामीण भारत के प्रति गंभीर नहीं है। इसका अर्थ यह भी होगा कि ग्रामीण भारत के विकास की कोई रूपरेखा है ही नहीं, अर्थात ग्रामीण भारत के विकास के लिये महात्मा गाँधी और उनका दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अब समसामयिक नहीं रहा।
भारत में ग्रामीण विकास नीति का दायरा इतना व्यापक होना ही चाहिये कि 'विकास' को गावों के पिछड़ापन बनाम शहरों के संपन्नता के संकुचित सोच से बाहर लाया जा सकें। विकास का अर्थ यदि 'पिछड़े और संपन्न' के बीच का फ़ासला भर रह गया तो यह मान लेने के पर्याप्त कारण होंगे कि जाने-अनजाने हम फिर उन्हीं मार्गों पर लौट जायेंगे जहाँ से चलकर यहाँ तक आये थे।
वास्तविकता यह है कि ग्रामीण विकास की बुनियादी इकाइयों को सरकार और समाज नें विकास के किसी भी पैमानों से पूरी तरह खारिज़ कर दिया है। इसीलिये भारत मे ‘ग्रामीण विकास की नीति' की तलाश और तराश आज़ादी के सात दशकों के बाद भी अधूरी है। गावों के गौरव को शहरी विकास के लिये बलि देने की प्रथा, अब तो समाप्त होनी ही चाहिये। आज हिन्द स्वराज को स्वीकरना नई उम्मीदों की ओर पहला कदम होगा ।
(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक हैं)