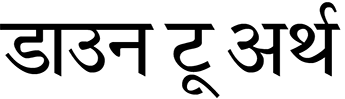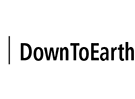साहित्य में पर्यावरण: संरक्षण की लोक साहित्य परम्परा
समाज सहज भाव में अपनी लोकभाषा में साहित्य रचता रहा है और पर्यावरण की चिंता वहां सदियों से है
On: Wednesday 13 October 2021

 इलस्ट्रेशन: रितिका बोहरा
इलस्ट्रेशन: रितिका बोहरा - बाबूलाल दाहिया-
लोक साहित्य जन साहित्य है, गाँव का साहित्य, या ,यूं कहें कि खेती किसानी का साहित्य है। क्योकि 60- 70 फीसदी जनसंख्या आज भी खेती पर ही निर्भर है। यही कारण है कि यदि शहर का आदमी गेहूँ ,चावल खरीदने जाता है तो उसका मात्र 10- 12 शब्दों में ही काम चल जाता है।
या तो वह झोला लेगा या बोरा लेगा? साइकिल लेगा या रिक्शा पकड़ेगा? मोल-भाव, वाट, तराजू पैसा-दाम आदि बस इतने शब्दों में उसके घर गेहूँ चावल आ जायगा।
किन्तु वहीं अनाज जब किसान खेत मे उगाता है तो खेत की तैयारी से लेकर उसके भंडार गृह में संचय के लिए अनाज के आते-आते लगभग दो ढाई सौ शब्द का इस्तेमाल होता है। पर यह शब्द किसी भाषा के नहीं बल्कि बोलियों के होते हैं।
नर वानर से उबर कर विकसित रूप में मनुष्य भले ही एक करोड़ वर्ष से इस धरती में हो किंतु 99 लाख नब्बे हजार वर्ष वह बिना खेती के ही रहा। खेती का इतिहास मात्र 10 हजार वर्ष पुराना ही है। और व्यवस्थित खेती तो ईसा पूर्व 800 वर्ष के आस-पास ही शुरू हुई जब लौह अयस्क की खोज हो गई। तभी से वह मैदान में कुंआ खोदकर वहां बसने लगा। क्योंकि लोहा के खोज के पहले प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी बस्तियां थीं वह सभी किसी नदी के किनारे ही बसी थीं और उसी का पानी पीती थीं।
किन्तु उसके खेती के बिस्तार के साथ -साथ लौह अयस्क आ जाने से अन्य कुटीर उद्योग भी विकसित हुए , जिससे गाँव मे वस्तु विनिमय का एक कृषि आश्रित समाज ही बना और उसी अनुभव जनित ज्ञान का मौखिक परम्परा में जो साहित्य रचा गया या जो मौखिक परम्पराए विकसित हुईं, लोक परम्पराए और लोक साहित्य कहलाये, पर रसायन युक्त आधुनिक पर्यावरण विध्वंसक खेती के पहले जितनी भी खेती थी वह सब लोक विज्ञान या लोक परम्परा से निकली पर्यावरण संरक्षण की ही खेती थी जिसमे कदम कदम पर पर्यावरण का संरक्षण था। क्योंकि वह वर्तमान सेठ की खेती के बजाय समूचे गाँव के पेट की खेती होती थी। उसमे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन नही संरक्षण होता था।
यह जरूर है कि लिपि के अभाव में उनके अनुभव य अनुसन्धान का प्रलेखी कारण नही हो सकता था। पर अगली पीढ़ी तक उनका खोजा हुआ ज्ञान उपयोगी रहे अस्तु हमारे कृषक पूर्वज उसे कहावतों में सूत्र बद्ध कर देते थे। जो आज भी यदा-कदा लोकोक्तियों कहावतों में लोक कंठ से मुखर होते रहते हैं। यहां कुछ उदाहरण समीचीन होंगे। खेती किसानी में सबसे जरूरी था जल संरक्षण। इसीलिए कहा जाता था कि - पानी नही तो ,किसानी नहीं। इसी से वर्षा आधारित खेती में जल संरक्षण का बहुत बड़ा महत्व था।
तालाब बनवाना पुण्य का कार्य माना जाता। तालाब कोई बनवाये पर उद्देश्य हमेशा सार्वजनिक ही था। उससे समूचे गाँव का जल स्तर बढ़ता था। यही कारण था कि अनेक बघेली बोली के लोकगीतों में ससुराल आई नई बहू अपने श्वशुर य जेठ से घर के समीप तालाब बनवाने की इच्छा व्यक्त करती है।
उधर खेती में देखा जाय तो यदि आषाढ़ से क्वार माह के बीच बतर आने पर खेत की एक-दो बार जुताई हो जाये तो तीन माह की वर्षा का सारा जल खेत सोख लेता था।
उससे जहां गाँव का जल स्तर बढ़ता था वही गेहूं चना आदि रवी की फसल के लिए उस खेत मे पर्याप्त नमी भी संचित हो जाती थी। लेकिन लोक साहित्य के कहावत में आकर वह पर्यावरण संरक्षण में कैसे उपयोगी बनता? इस कहावत में देखें :
“ गोहूँ भा काहे?”
“असाढ़ के दुइ बाहे।”
अब इस कहावत में एक अन्तर कथा है। एक गाँव के किसी भूभाग में सभी किसानों की एक जैसी भूमि थी। पर एक किसान के खेत का गेहूं अन्य किसानों के खेत के अपेक्षा बहुत अच्छा था। जब किसान खेत घूमने गए और उस खेत को देखा तो उससे पूछने लगे कि “क्यो भाई ? जमीन तो सभी किसानों की एक जैसी है,पर तेरे खेत मे इतना अच्छा गेहूं क्यो हुआ है?” उसने बताया कि मैने आषाढ़ में मानसूनी बारिश के बाद अपने खेत की दो बार अड़ी और खड़ी जुताई कर दी थी। अस्तु सारी नमी खेत मे संचित होती गई इसलिए मेरा गेहूं तुम सभी से अच्छा है। पर तुम सब ने मेरी तरह नही किया था।
इसी तरह एक कहावत सावन मास पर भी है कि :
“सामन बाहे।
गोहूँ गाहे।।”
अर्थात, सावन में बतर में आने पर यदि जुताई कर दोगे तो तुम्हारे खेत मे गेहूँ की उपज अच्छी होगी। किन्तु हमारे बघेली लोक साहित्य में एक आलसी किसान पर भी एक कहावत कही गई है। कहते हैं कि तीन माह तक रहने वाली वर्षा ऋतु की अवधि में बीच-बीच मे जब कई बार चार-पाँच दिन का सूखे का मौसम आया तो उसका लाभ उठा बांकी कृषक तो अपने खेत की जुताई करते रहे जिससे उनके खेत मे नमी संचित होती रही। पर एक आलसी किसान ऐसा भी था जो सारी वर्षा ऋतु तक तो हाथ में हाथ रखे बैठा रहा परन्तु जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तो खेत की 2-3 बार जुताई कर रहा था। लेकिन जब पड़ोस के किसानों ने देखा तो परिहास उड़ाते हुए कहने लगे कि-
“बाहे नही तय एक आषाढ़।
अब का बहते बारम्बार।।”
अर्थात, ‘तुमने आषाढ़ में जब समय था तब खेत मे एक बार भी हल नही चलाया था जिससे वर्षा का पानी सोख कर खेत नमी संचित कर लेता? पर अब तुम्हारा खेत जब रूखा हो गया है तो कई बार जुताई कर रहे हो ? अब इस जुताई से भला क्या लाभ रह गया है?’ अब तो हरित क्रान्ति आने के पश्चात खेती की पद्धति ही बदल गई है। प्राचीन समय में अदल-बदल या मिलमा खेती ऐसी खेती थी जिसमे पूरी तरह खेत की उर्वरता का टिकाऊ पना एवं पर्यावरण संरक्षण था। प्रथम वर्ष यदि खेत मे चना बोया जाता तो दूसरे वर्ष कोदो य फिर ज्वार की मिलमा खेती। इस खेती से खेत की उर्वरता हमेशा बनी रहती।
चने की जड़ो में उतपन्न बैक्टीरिया अगर खेत मे नत्रजन पैदा कर देते तो कोदो के डंठल सड़ कर दूसरे वर्ष के लिए उसे उपजाऊ बना देते। इसी तरह ज्वार की मिलमा खेती ऐसी पर्यावरण संरक्षक खेती थी जिसमे ज्वार के खेत मे ही कई तरह के अनाजो की पैदावार हो जाती थी।
उसमे मिलमा बोने से जहा तिल से तेल, अम्बारी से रस्सी गेरमा, उड़द मूग से बारा मुगौरा और अरहर से दाल की आपूर्ति होती वही गर्म ताशीर की ज्वार को लोग जाड़े के दिनों में नवम्बर से फरवरी तक रोटी या दलिया के रूप में खाते जिससे शीत जनिति बीमारी से भी बचाव होता। पर खेत की उर्वरता में कोई भी अन्तर न आता। क्योंकि लोक साहित्य के कहावत रूपी हिदायत के अनुसार ही एक खास गैप में ज्वार की खेती की जाती थी। ताकि उसके नीचे के गैप में दो फीट के झाड़ी नुमा उड़द-मूंग भी हो जाय और ऊपर के गैप में चार फीट की तिल व पाँच फीट की अम्बारी भी। किन्तु मार्च में पकने वाली दुबली पतली अरहर तब अपना बिस्तार करे जब नवम्बर में ज्वार, तिल, मूग, उड़द वगैरह कट जाए। पर कहावत थी कि -
कदम-कदम पर बाजरा, दादुर कुदनी ज्वार।
जे जन ऐसा बोइहैं, उनके भरें कोठार।।
दादुर कुदनी ज्वार का आशय यहाँ लगभग डेढ़ दो फीट के दूरी पर ज्वार को बोने से है जितनी लम्बी मेढ़क की छलांग होती है। तभी तो उस ज्वार के ऊपर और नीचे के फासले पर सभी अनाज उग कर किसान के कुठले को भरेंगे?
क्योंकि ज्वार का पौधा 7 फीट ऊँचा होता है। पर उसी की तरह लम्बी तिल और अम्बारी भी लम्बवत बढ़ती हैं। इस तरह हमारे बघेली साहित्य और परम्परा में पर्यावरण संरक्षण की अनेक मौखिक परम्परा एवं मुहावरे लोकोक्तियाँ कहावतें हैं। जो समय- समय पर अगली पीढ़ी को निर्देशित करती रहती थीं।
अगर कैथा फल को दशहरा तक न खाने,आंवला को कार्तिक की इच्छा नवमी तक उपयोग न करने की बन्दिश थी या अचार चिरोंजी को अक्षय तृतीया तक नही तोड़ा जाता था तो उसके पीछे यह तर्क था कि वह समय के पहले समूल नष्ट न हो जाये, बल्कि उनका वंश परिवर्धन भी हो? क्योंकि कैथा दशहरा के आस-पास पकता है और चिरोंजी का फल बैसाख के शुक्ल पक्ष में ही।
इसी तरह आंवला में भी औषधीय गुण कार्तिक के बाद ही आते हैं। आज आयुर्वेद की बहुत सारी कम्पनियां हैं जिनके द्वारा थोक में जमीन से जड़ी बूटियों को उपार्जित िकया जाता हैं।
किन्तु हमारे बघेली क्षेत्र के ग्रामीण परम्परा में उपार्जन के एक दिन पहले हल्दी चावल लेकर विदोहन करने वाला जाता और उस औषधि के पास हल्दी चावल रख कर बिनती करता कि “ हे अमुक औषधि! हम तुम्हे चिकित्सा के लिए कल भोर में ले जाए गे ? तुम हमारे लिए फल दाई बनना” इस तरह इन सब परम्पराओ से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह उपार्जन कर्ता उस औषधि को किस मात्रा में बिदोहित करता रहा होगा? यहां तक कि यदि कोई लकड़ी काटने या फल तोड़ने के लिए भी पेड़ में चढ़ता तो उसके पहले पेड़ के चरण छूने का उपक्रम करके ही चढ़ता था।
इसी तरह कुछ औषधियों को तो अर्धरात्रि में नग्न होकर उसके जड़ को बिदोहित किया जाता था। इसलिए हमारी बघेली परम्परा में कदम - कदम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हीन विदोहन था जो पर्यावरण संरक्षण का ही पर्याय था।
(लेखक साहित्यकार और लोकपरंपरा के जानकार हैं)