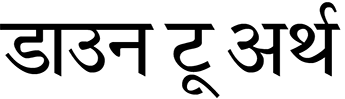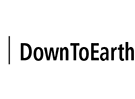पर्यावरणीय संकट काल में मार्क्सवाद और वैकल्पिक विकास-विमर्श
मार्क्स का विमर्श उन्नीसवी सदी में रहा है, जबकि पर्यावरण का प्रश्न बीसवी सदी में उभर कर सामने आया है, लेकिन उनके कुछ विचारों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाता है
On: Thursday 31 August 2023

 जोशीमठ में भूधंसाव का सिलसिला जारी है। फोटो: सन्नी गौतम
जोशीमठ में भूधंसाव का सिलसिला जारी है। फोटो: सन्नी गौतम कभी जमीन धंस जा रही है। कभी भी तूफान आ रहा है, कभी नदियां मचल जा रही हैं और कभी भी पहाड़ बिखर जा रहा है। यह बेचैन धरती की छटपटाहट है। कब कौन सा प्राकृतिक संकट आ जाए, कहना कठिन हो गया है। दुनिया पर्यावरण से सम्बंधित गंभीर समस्याओं से जूझ रही है।
एक तरह से यह आपदाओं के बीच आ बैठी है। यह संकट आण्विक संकट से भी गंभीर है और इन सबके लिए वैश्विक पूंजीवाद को मासूम करार नहीं दिया जा सकता।
वैश्विक पूंजीवाद द्वारा मचाई गई प्रकृति की प्रचंड लूट-पाट को देखते हुए इसकी तीव्र आलोचना की जा रही है, और वैकल्पिक वैकासिक प्रतिमान के रूप में मार्क्सवाद से प्रेरित विकास प्रतिमान की भी बात की जा रही है।
ऐसे में यह जरुरी है कि समझा जाए कि मार्क्सवाद का पर्यावरणीय प्रश्नों पर किस तरह का विमर्श रहा है। वैसे यह एक आम धारणा है कि मार्क्स ने पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं लिखा है।
इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मार्क्स का विमर्श उन्नीसवी सदी में रहा है, जबकि पर्यावरण का प्रश्न बीसवी सदी में उभर कर सामने आया है। ऐसे में उस समय न तो आण्विक हथियारों की खोज ही हुई थी और न अन्य गंभीर रूप से हानिकारक रसायनों का चलन व्यापक स्तर पर प्रारंभ हुआ था।
लेकिन इसके बाद भी चिंतकों की एक धारा ऐसी भी है, जिसने मार्क्स के लेखन में पर्यावरणीय चेतना के तत्व देखे हैं। उन्होंने उनके लेखन और उनके विचारों में उपस्थित पर्यावरण से सम्बंधित अदृश्य या अप्रत्यक्ष लेखन को इस विमर्श के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया है।
जैसे एक जगह मार्क्स लिख रहे हैं- ‘यहाँ तक कि पूरा समाज, या सम्पूर्ण राष्ट्र पृथ्वी का स्वामी नहीं है। उन्होंने इसे मात्र अपने अधिकार में किया हुआ है, या फिर इसके लाभ पाने वालों में से एक हैं। इसलिए उसे चाहिए कि वह अगली पीढ़ी को यह पृथ्वी और बेहतर स्थिति में सौंपे।’
मार्क्स की इस पंक्ति पर विचार करने पर लगता है कि धारणीय विकास की अवधारणा से एक शब्द के रूप में मार्क्स भले अपरिचित रहे हों, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित और संयमित दोहन के प्रति उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। वे धरती की जीवंत निरंतरता को लेकर सजग थे।
‘जर्मन आइडियोलॉजी’ में एक जगह मार्क्स लिखते हैं- ‘मछली की सार्थकता उसके पानी में होने में है। और साफ पानी में रहने वाली मछलियों के लिए नदी की आवश्यकता है। ...लेकिन यह अब संभव नहीं रहा, क्योंकि नदियां अब फैक्ट्रियों की सेवा में लगा दी गई है।'
'...कपड़ों को रंगनेवाले जहरीले रंग, कचड़े, और साथ में उसमें चलने वाले स्टीमबोट, और उसमें बहाई जानेवाली नालियों ने मछलियों के इस जीवन को प्रभावित किया है।’ निश्चय ही प्रकृति में उपस्थित विविधता और सौन्दर्य उनकी लेखकीय चेतना का हिस्सा रहा है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, जो अलग-अलग सन्दर्भों में उनके लेखन और विचार में बार बार झलकता भी है।
इसी तरह से ‘ऑन द ज्यूज क्वेश्चन’ में वह कहते हैं- ‘निजी संपत्ति और पूंजी के अधिनत्व में अगर प्रकृति को देखें तो यह प्रकृति की अवमानना और उनके अपमान की तरह है...’. क्योंकि निजी संपत्ति की संस्कृति में सभी चीजें वस्तु में बदल दी गई है।
उसका संवेदनात्मक या जीवन-पक्ष उपेक्षित कर दिया गया है। पानी में मचलने वाली मछलियां हो या हवा में उड़ने वाली चिड़ियां या फिर जमीन पर इठलाते पेड़ सबकी एक कीमत लगा दी गई है। इन सबके जीवन-पक्ष को मृत घोषित कर दिया गया है। बिक जाना या खरीद लिया जाना ही इनका मूल्य रह गया है- इनके आन्तरिक मूल्य के लिए कोई जगह नहीं रही।
मार्क्स के पर्यावरणीय विचारों को समझने के लिए यह भी जरुरी है कि हम उनके राजनीतिक और आर्थिक विकास के प्रतिमानों को समझें, जिसमें पर्यावरणीय चेतना अन्तर्निहित होने की अधिक सम्भावना है। वे जब ‘अलगाव’ या ‘एलिनेसन’ की बात कर रहें हैं, तब इसका सन्दर्भ व्यापक हो जाता है।
एक औद्योगिक समाज की दुनिया ऐसे मजदूरों का समूह तैयार करती है जो अपने गांव, अपनी परंपरा, और उसमें मौजूद धारणीय जीवन शैली से कट जाता है। यह मनुष्य का मनुष्य से और फिर मनुष्य का समाज से होते हुए मनुष्य का प्रकृति से अलगाव है और अंततः मनुष्य प्रकृतिजन्य विविधता को खोते हुए पूंजी की दुनिया में मशीनीकृत होकर जीने को बाध्य हो जाता है।
यह मनुष्यता की सबसे बुरी दशा है। इसे ही हर्बर्ट मार्क्यूज ‘वन डायमेंशनल मैन’ कहते हैं- जहाँ जीवन के अन्य पक्ष भौतिक पक्ष के सामने दम तोड़ देते हैं. औधोगिक पूंजीवादी संस्कृति साम्राज्यवादी तरीके से कार्य करती है. यह लगातार अपना विस्तार करती जाती है- और इस क्रम में गाँव बदसूरत शहरों में बदलते जाते हैं, जंगल विलुप्त होते जाते हैं, नदियाँ सूखती जाती है, और पहाड़ उजड़ते जाते हैं.
एक अर्थ में देखें तो आधुनिक पूंजीवादी विकास प्रतिमान में प्रकृति का भयानक नुकसान अनिवार्यतः होना है, और मार्क्स ऐसे विकास के प्रतिमान को बदलने की बात करते हैं।
निजी संपत्ति उनके लिए बड़ा मुद्दा है और जिससे मुक्ति के बिना पर्यावरणीय समस्याओं का भी हल नहीं किया जा सकता। साथ ही मार्क्सवाद की सबसे अहम् भूमिका पर्यावरणीय आन्दोलन को दिशा और गति देने में सहायक है।
इन सबके बावजूद पर्यावरण के मुद्दे पर मार्क्सवाद की वैधानिकता बहुत सशक्त नहीं मानी जा सकती।
इसके दो कारण हैं- पहला कि अपने व्यावहारिक स्वरूप में जब इसे एक आर्थिक विकास का प्रतिमान स्थापित करने का अवसर मिला तो उसने भी प्रकृति का घनघोर दोहन किया और दूसरा कि पर्यावरणीय सन्दर्भों में मार्क्सवाद सैद्धांतिक तौर पर इतना मजबूत नहीं कि इस प्रश्न पर एक मजबूत विमर्श दे सके सिवाए आन्दोलन की प्रेरणा बनने के।
इसके कई कारण है, जैसे-
पहला, मार्क्स के दृष्टिकोण को ‘प्रोमेथियन’ कहा जा सकता है, जिसमें तकनीक को प्रधानता दी गई है और पर्यावरण का प्रश्न महत्व का नहीं है। मनुष्य उसके केंद्र में है। उसकी मुक्ति ही उनकी अंतिम लालसा है।
दूसरा, उनका विश्वास था कि अगर पर्यावरण का संकट है भी तो उसे विकसित तकनीकों की सहायता से दूर किया जा सकता है।
तीसरा, तकनीक के पर्यावरण पर जो भयावह परिणाम हैं, उस पर भी मार्क्स की लेखनी मुखर नहीं मानी जा सकती।
और चौथा कि उन्होंने अपने लेखन में जो कुछ पर्यावरण पर कहा भी है वह बस अनायास प्रकार की पंक्तियां मात्र हैं, उसमें व्यवस्थित अध्ययन का अभाव दिखता है. बस सन्दर्भों में कही गई बातें हैं न कि एक व्यवस्थित प्रबंध।
साथ ही मार्क्स के लेखन में बार-बार ‘प्रकृति पर आधिपत्य’ का भाव दिखता है, जबकि पर्यावरण के विमर्श का केंद्रबिंदु इस बात पर है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ सम्बन्ध ही सहयोग और सामंजस्य वाला होना चाहिए- प्रकृति को जीते जाने की भावना में विनाश के बीज होते हैं। यह विजयी होने का लक्ष्य ही मानवता के पराजय का कारण माना जाता है।
पूंजीवादी विकास प्रतिमान हो या साम्यवादी विकास प्रतिमान- दुनिया ने दोनों का ही पर्याप्त अनुभव लिया है। और पर्यावरणीय सन्दर्भों में दोनों का ही अनुभव बुरा ही रहा है।
एक समय सोवियत संघ और अमेरिका में आण्विक हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। दोनों के लिए आधुनिक तकनीक और विकास का बराबर का महत्व था। दोनों के लिए विज्ञान का जो दर्शन था, उसमें प्रकृति को जीत लिए जाने की होड़ लगी रही।
कौन चांद पर और अन्तरिक्ष में अपना परचम लहरा सकता है, कौन समुद्र को जीत सकता है- यह सब युद्धस्तर पर चला। और इन्हीं सब कारणों से पर्यावरणीय आन्दोलन से गहरे जुड़े लोगों और विचारधाराओं ने दोनों ही विकास के प्रतिमानों को अस्वीकृत किया और माना कि दोनों ने ही प्रकृति का भयंकर नुकसान किया है।
सोवियत संघ के पतन के बाद यह होड़ अब अमेरिका और चीन के बीच देखी जा सकती है। जरुरी है कि विकास के अन्य मौजूद वैकल्पिक प्रतिमानों के विमर्श को लोकप्रिय बनाया जाए।
प्राचीन भारतीय जीवन-दर्शन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिए जरुरी है कि यह वैश्विक पूंजी के सामने घुटने न टेके, जिसकी सम्भावना कम दिख रही।
भारत का पारंपरिक जीवन दर्शन गांव केन्द्रित है, जिसका ताना-बाना स्थानिकता और वहां के परिवेश से बुना है। यह अधिक समावेशी भी है और धारणीय भी। इसमें जंगल भी है, जंगली जीव भी, नदियां भी है और पहाड़ भी।
और इन सबको बचाने का जो भाव है, वह इसकी संस्कृति में निहित है। इसकी लोक परम्पराएं, और त्यौहार तक पर्यावरण के मूल्यों से युक्त है। समझे जाने की जरुरत है कि यह दुनिया आज ऐसी है तो इसलिए नहीं कि यही इसकी नियति थी, यह इसलिए है क्योंकि इसे ऐसी बनाई गई है। इसलिए इस बनाई गई दुनिया को फिर से एक सुन्दर दुनिया बनाई जा सकती है।
लेखक समाजशास्त्र विभाग, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लेख में प्रस्तुत विचार उनके स्वयं के हैं।