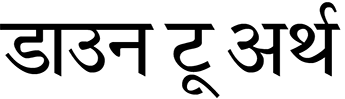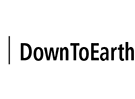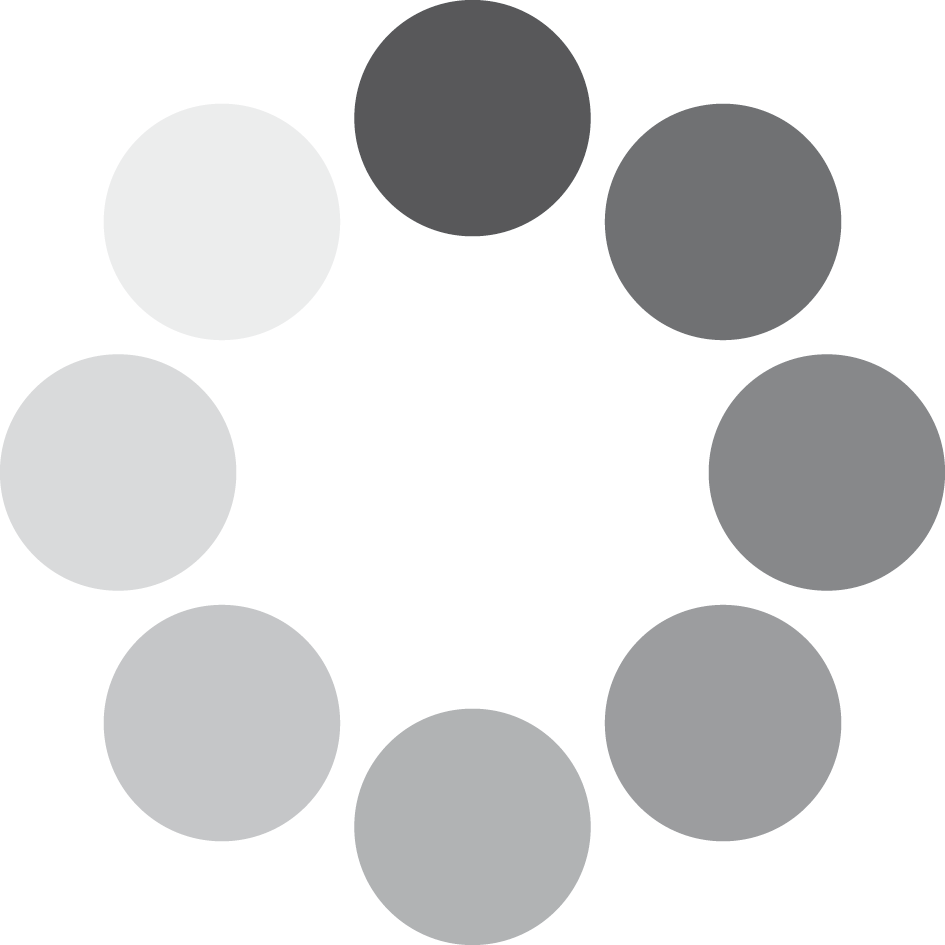भारत के हिमालयी क्षेत्र में मिली जंगली मशरूम की पांच नई प्रजातियां, जानिए क्यों हैं खास
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली में खोजी गई जंगली मशरूम की इन पांच प्रजातियों में लेसीनेलम बोथी, फाइलोपोरस स्मिथाई, रेटिबोलेटस स्यूडोएटर, फाइलोपोरस हिमालयेनस और पोर्फिरेलस उत्तराखंडाई शामिल हैं
On: Tuesday 14 May 2024

 फाइलोपोरस स्मिथाई, उत्तराखंड से खोजी गई मशरूम की पांच नई प्रजातियों में से एक है। फोटो: दास, कणाद एट अल/ साइंटिफिक रिपोर्ट्स (2024)
फाइलोपोरस स्मिथाई, उत्तराखंड से खोजी गई मशरूम की पांच नई प्रजातियों में से एक है। फोटो: दास, कणाद एट अल/ साइंटिफिक रिपोर्ट्स (2024) वैज्ञानिकों ने हिमालयी राज्य उत्तराखंड में जंगली मशरूम की पांच नई प्रजातियां खोजी हैं, जो विज्ञान के लिए भी नई हैं। इनके साथ ही वैज्ञानिकों ने मशरूम की दो अन्य प्रजातियों के भी भारत में पहली बार देखे जाने की पुष्टि की है। बता दें कि, मशरूम की यह प्रजातियां खाने योग्य नहीं हैं, लेकिन इन्हें हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और औषधि निर्माण के लिहाज से काफी उपयोगी माना जा रहा है।
भारत के हिमालयी क्षेत्र में कई प्रकार के जंगली मशरूम हैं, लेकिन इनमें से ऐसा कई हैं जिनके बारे में बेहद कम जानकारी मौजूद है। यह खोज इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि हिमालय क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से कितना समृद्ध है। ऐसे में संरक्षण के प्रयासों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। बता दें कि मशरूम की इन नई प्रजातियों की खोज बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम के प्रख्यात कवक विज्ञानी डॉक्टर कणाद दास के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा की गई है।
इस अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने उनके आकार, रंग, संरचना के साथ-साथ उनके जीन का भी अध्ययन किया है। इस खोज में बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड और टोरिनो विश्वविद्यालय, इटली के वैज्ञानिक शामिल थे। इन प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी अंतरराष्ट्रीय जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुई है।
इनमें से जंगली मशरूम की एक प्रजाति 'लेसीनेलम बोथी' रुद्रप्रयाग के बनियाकुंड में 2,622 मीटर की ऊंचाई खोजी गई है। वहीं ‘फाइलोपोरस स्मिथाई’ नामक प्रजाति भी बनियाकुंड में करीब 2,562 मीटर की ऊंचाई पर खोजी गई। वहीं मशरूम की दो प्रजातियां बागेश्वर जनपद में खोजी गई हैं। इनमें से एक ‘रेटिबोलेटस स्यूडोएटर’ 2,545 मीटर की ऊंचाई पर जबकि जंगली मशरूम ‘फाइलोपोरस हिमालयेनस’ करीब 2,870 मीटर की ऊंचाई पर मिली है। वहीं पांचवी प्रजाति ‘पोर्फिरेलस उत्तराखंडाई’ के मशरूम को चमोली के लोहाजंग में करीब 2,283 मीटर की ऊंचाई पर खोजा गया है।
इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने मशरूम की दो अन्य प्रजातियों लेसीनेलम सिनोअरेंटियाकम और जेरोकोमस रगोसेलस के भारत में पहली बार देखे जाने की पुष्टि की है।
भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि मशरूम पोषण के साथ-साथ औषधीय गुणों से संपन्न होते हैं। यह इम्युनिटी बढ़ाने के साथ शरीर की वायरस से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं।
दुनिया में कवकों की हैं 25 लाख से अधिक प्रजातियां
वैज्ञानिकों के मुताबिक मशरूम में प्राकृतिक रूप से मौजूद बायोएक्टिव तत्व हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण के साथ-साथ वायरस, सूजन और रक्त के थक्के को जमने से रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि यह तत्व मशरूम में प्राकृतिक तौर पर मौजूद होते हैं और वो ऐसे मशरूमों में भी पाए जाते हैं, जिन्हें ढूंढना आसान है।
बता दें कि यह मशरूम भी एक तरह के कवक या फंगी होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी की दुनिया में कवकों की 25 लाख से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें 90 फीसदी से भी ज्यादा से दुनिया अनजान है। इनके बारे में हमें कितनी कम जानकारी है यह इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक तौर पर दुनिया में अब तक कवकों की केवल 155,000 प्रजातियों को खोजा और दर्ज किया जा सका है। उनमें से भी करीब आधी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं यदि इनके औषधीय गुणों को देखें तो संक्रमण से बचाव के लिए कई दवाएं कवक से ही बनाई जाती है।
"स्टेट ऑफ द वर्ल्डस प्लांट एंड फंगी 2023" नामक रिपोर्ट के मुताबिक यह कवक पेड़-पौधों के अस्तित्व के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं। कवक की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं, जो पेड़ पौधों के साथ मिलकर रहती हैं। यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, माइकोरिजल कवक पौधों की जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे में पौधे पानी, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे खनिज पोषक तत्वों के बदले में कवक को कार्बन और वसा प्रदान करते हैं। वहीं कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी छाया में रहते हैं। यह रोगजनकों के प्रति पौधों की प्रतिरक्षा को उत्तेजित करके और उन्हें इससे बचाए रखें में मदद करते हैं।
हालांकि कवकों की जिन प्रजातियों के बारे में हमारे पास जानकारी मौजूद है उनमें कई प्रजातियां भूमि उपयोग में आते बदलावों और जलवायु परिवर्तन के चलते खतरों का सामना कर रही है। ऐसे में उनके अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर जोर देना जरूरी है।