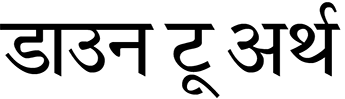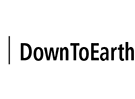वन विभाग बनाम वनाधिकार कानून
भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले तंत्र के चरित्र को एक बार फिर बेनकाब कर रहा है
On: Thursday 04 August 2022

 इलेस्ट्रेशन: साभार विक्रम नायक
इलेस्ट्रेशन: साभार विक्रम नायक वर्ष 1865, भारत में जब ब्रितानिया हुकूमत के द्वारा वनों और वन संसाधनों के दोहन के लिए वैधानिक बुनियाद रखी जा रही थी, तब भारत के लगभग 47 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र में जंगल थे, जिन पर आदिवासी और वनाश्रित समाज का सदियों से नैसर्गिक स्वामित्व रहा।
लेकिन, ब्रितानिया हुकूमत के प्रथम वन कानून (1865) ने हमेशा के लिये वनों, वन संसाधनों और वनभूमि को 'राजस्व' के साधनों में तब्दील कर दिया।
भारत के अनुमानतः 47 फीसदी वनक्षेत्र का भू-राजनैतिक स्वरुप तथा वनों से नैसर्गिक रूप से जुड़े आदिवासी समाज के अस्तित्व, अधिकारों और अर्थतंत्र को वर्ष 1865 के वन कानून के साथ ही सदा सर्वदा के लिये ‘सशर्त रियायतों’ में अपघटित कर दिया गया।
कालांतर में वर्ष 1927 के औपनिवेशिक भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत बाकायदा 'वन विकास निगम' की स्थापना की गयी, जिसका वैधानिक मकसद वनों और वन संसाधनों का दोहन था/ और जो आज भी है।
आज जब वन विभाग का वन विकास निगम ही वनों के दोहन के लिये वैधानिक रूप से जवाबदेह है, तब इस सवाल का भी स्पष्ट जवाब होना ही चाहिये कि - वर्ष 1927 से अब तक वन विकास निगम के माध्यम से कुल कितने पेड़ और जंगल काटे गये और उससे कितना राजस्व अर्जित किया गया?
क्या अर्जित राजस्व का उपयोग स्थानीय संबंधित आदिवासी और वनाश्रित समाज के लिये किया गया? क्या वन विकास निगम की अनुमति और संज्ञान से होने वाले निर्वनीकरण की सूचना स्थानीय ग्रामवासियों को कभी दी गई ? क्या संसाधनविहीन हुये आदिवासी समाज को पुनर्स्थापित अथवा पुनर्वासित किया गया ?
जाहिर है इन जटिल सवालों के सरल उत्तर कहीं किसी के भी पास नहीं हैं। इसलिये नहीं कि वन विभाग उत्तर देने में सक्षम नहीं है - बल्कि इसलिये कि ऐसे सवालों का जवाब देना वन विभाग के संहिता में ही नहीं है।
वाकई में वन विभाग की संरचना और सोच, अब तक औपनिवेशिक ब्रितानिया हुकूमत के अधीन मालूम पड़ती है - जिनकी नजरों में जंगलों के सर्वकालीन संरक्षक, आदिवासी समाज की हैसियत आज भी एक 'अतिक्रमणकर्ता' की है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन सेवा के अधिकारिओं को पढ़ाते हैं कि वनों का संरक्षक तो 'वन विभाग' ही है - और इसीलिये वन विभाग की जागीर पर रहने वाला आदिवासी और वनाश्रित समाज 'अवैध अतिक्रमणकर्ता' है।
वन अधिकारी और कर्मचारी यह भी पढ़ते हैं कि वन विकास निगम द्वारा नियोजित और कार्यान्वित किये जाना वाला - राजस्व योग्य काष्ठीय पौधों का वनीकरण अथवा निर्वनीकरण ‘पूर्णतः वैध’ और इसका विरोध करने वाले ‘अवैध अतिक्रमणकर्ता’ हैं।
जाहिर है, औपनिवेशिक वन अधिनियम (1927) पर आधारित पूर्वाग्रहपूर्ण शिक्षा प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के क्रियाकलाप और मानसिकता 'आदिवासी हितों' के लिये होना संदिग्ध ही है।
वर्ष 2008 में वनाधिकार कानून (2006) के अधिसूचना के साथ ही भारतीय वन सेवा के (सेवानिवृत्त) अधिकारियों ने जब न्यायालय में वनाधिकार कानून की वैधता को चुनौती दी, तब उसके साथ ही यह सुनिश्चित हो गया कि वन विभाग अपने औपनिवेशिक चरित्र के चलते वनाधिकार कानून के मार्ग में स्थायी अवरोधक बना रहेगा।
पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग का संदिग्ध नजरिया और उसका जाहिरा परिणाम 'वनाधिकार कानून' के वैधानिक और व्यवहारिक ढांचे को लगातार चुनौती दे रहा है।
वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय में वनभूमि से तथाकथित अवैध अतिक्रमणकर्ताओं की बेदखली हेतु (छदम पर्यावरणवादियों द्वारा) दाखिल याचिका इसकी ही बानगी है।
इसके साथ-साथ वनाधिकार कानून (2006) के वैधानिक ढांचे को ही कुंद करने का नया प्रयास प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि विगत 2-3 बरस में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की दर और गति विगत 15 वर्षों में सबसे कमजोर और धीमी रही है।
और अब, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को जारी नया फरमान, आदिवासियों और वनाश्रितों के विरुद्ध ऐतिहासिक अन्याय करने वाले तंत्र के चरित्र को एक बार फिर बेनकाब कर रहा है।
इस फरमान के मुताबिक किसी भी (तथाकथित) विकास योजना के लिये स्थानीय आदिवासी और वनाश्रित समाज से मंजूरी लेने (या ना लेने) की जवाबदेही (अथवा औपचारिकता) अब राज्य सरकारों की है।
वास्तव में यह फरमान, ‘वेदांता बनाम डोंगरिया कंध आदिवासी पंचायत’ प्रकरण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले का जाहिर उल्लंघन है जिसके मुताबिक (विकास योजनाओं के लिये किसी भी) निर्वनीकरण से पूर्व स्थानीय संबंधित आदिवासी समाज से वैधानिक अनुमति अनिवार्य है।
26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करते हुये विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों नें भारत सरकार से अपील की है कि 28 जून 2022 को जारी आदेश वापस लिया जाना चाहिये ताकि आदिवासियों और वनाश्रित समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। उम्मीद है भारत सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की जायेगी।
ग़ौरतलब है कि दिसंबर 2015 में स्वयं, भारत सरकार के आदिवासी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि (विकास योजनाओं हेतु) निर्वनीकरण की प्रक्रिया से पूर्व स्थानीय आदिवासियों और वनाश्रित समाज से सहमति लेना आवश्यक है ताकि निर्णयों को ज्यादा वैधानिक, पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जा सके।
भारत में अनेक प्रकरण हैं जहां राजनैतिक सहूलियतों के चलते ऐसे निर्णयों को ‘स्थापित अथवा स्थगित’ करने का खेल सरकारों के मध्य खेला गया। इसीलिये विभागीय समीकरणों से सुलझाये - उलझाये जाने वाले निर्णयों को आदिवासी समाज अब भी संदेह की दृष्टि से देखता है।
क्या वर्तमान के पंचायत कानूनों को सर्वोपरि मानकर उनकी सहमति - असहमति को अंतिम नहीं माना जाना चाहिये ?
बहरहाल, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (भारत सरकार) के नये फरमान के चलते लगभग उन सभी क्षेत्रों में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में बाधा आयेगी जहाँ किसी भी परियोजना से पूर्व स्थानीय आदिवासी समाज, ऐतिहासिक न्याय के आलोक में अपना वनाधिकार चाहता है।
भारत में 1927 का भारतीय वन अधिनियम लागू हुये, अर्थात औपनिवेशिक अन्याय के लगभग 95 बरस पूरे हो चुके हैं - जिसका सार्वजानिक परिणाम है।
आदिवासियों की मातृभूमि पर वन विभाग के अतिक्रमण के चलते आदिवासियों की बेदखली….
भारत के वन आच्छादन में शर्मनाक गिरावट….
वन विभाग द्वारा संरक्षित जंगलों की वैध-अवैध कटाई और उससे अर्जित राजस्व….
तथा वनभूमि के अवैज्ञानिक विस्तार के चलते लाखों आदिवासियों को भूमिहीन बना देने की शर्मनाक कार्रवाई।
जाहिर है, जिस 'ऐतिहासिक अन्याय' के उपचार हेतु वनाधिकार कानून लागू किया गया वो 'भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण कानून 1980' के चलते न केवल बेमानी साबित हो रहे हैं, वरन वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में वैधानिक चुनौतियां खड़े कर रहे हैं।
आज आवश्यकता इस बात की है कि वनाधिकार कानून (2006) के वैधानिक प्रावधान और भावना के अनुरूप, स्वयं सरकारों द्वारा इसे प्रभावी तरीके से लागू करने का अभियान प्रारंभ करना चाहिये। अन्यथा वनाधिकार कानून, ऐतिहासिक न्याय का मार्ग कभी नहीं बन पायेगा।
आने वाले कुछ बरस वन विभाग को परे रखकर - आदिवासी कल्याण विभाग को और अधिक सशक्त करने का होना ही चाहिये। ऐसा नहीं होने का अर्थ लाखों-करोड़ों आदिवासियों के उन सभी जीवित सपनों का अंत होगा जो ब्रितानिया हुकूमत के विरुद्ध प्रथम आदिवासी विद्रोह से वह अब तक देखता - समझता और सुनता आया है।
जाहिर है, उनकी जिंदा उम्मीदों को पूरा करने वाला एक सजीव और संवेदनशील तंत्र चाहिये आज और अभी।
(लेखक रमेश शर्मा - एकता परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं)